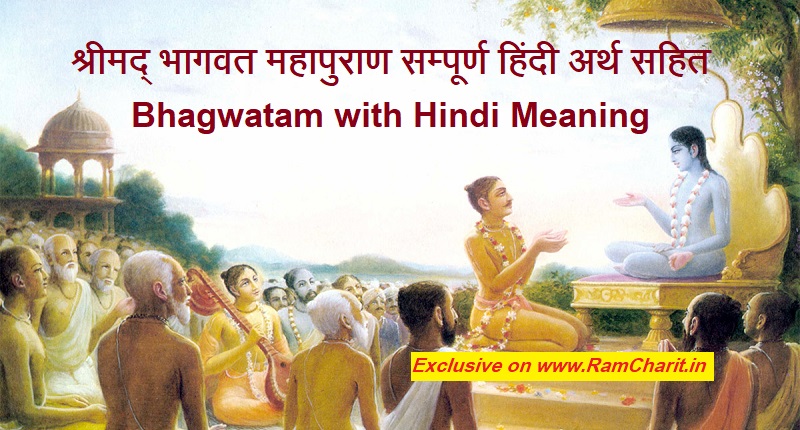श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 10 अध्याय 87
87 CHAPTER
श्रीमद्भागवतपुराणम्
स्कन्धः १०/उत्तरार्धः/अध्यायः ८७
वेदस्तुति –
श्रीपरीक्षिदुवाच –
( अनुष्टुप् )
ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः ।
कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे ॥ १ ॥
राजा परीक्षित्ने पूछा-भगवन्! ब्रह्म कार्य और कारणसे सर्वथा परे है। सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गण उसमें हैं ही नहीं। मन और वाणीसे संकेतरूपमें भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियोंका विषय गुण ही है। (वे जिस विषयका वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, क्रिया अथवा रूढिका ही निर्देश करती हैं) ऐसी स्थितिमें श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्मका प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं? क्योंकि निर्गण वस्तुका स्वरूप तो उनकी पहुँचके परे है ।।१।।
श्रीशुक उवाच –
बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान् जनानां असृजत् प्रभुः ।
मात्रार्थं च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च ॥ २ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! (भगवान् सर्वशक्तिमान् और गुणोंके निधान हैं। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर उनका तात्पर्य निर्गुण ही निकलता है। विचार करनेके लिये ही) भगवान्ने जीवोंके लिये बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छासे अर्थ, धर्म, काम अथवा मोक्षका अर्जन कर सकते हैं (प्राणोंके द्वारा जीवन-धारण, श्रवणादि इन्द्रियोंके द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके द्वारा मनन और बुद्धिके द्वारा निश्चय करनेपर श्रुतियोंके तात्पर्य निर्गुण स्वरूपका साक्षात्कार हो सकता है। इसलिये श्रुतियाँ सगुणका प्रतिपादन करनेपर भी वस्तुतः निर्गुणपरक हैं) ||२||
सैषा ह्युपनिषद् ब्राह्मी पूर्वेशां पूर्वजैर्धृता ।
श्र्रद्धया धारयेद् यस्तां क्षेमं गच्छेदकिञ्चनः ॥ ३ ॥
ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजोंके भी पूर्वज सनकादि ऋषियोंने आत्मनिश्चयके द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धापूर्वक धारण करता है, वह बन्धनके कारण समस्त उपाधियों-अनात्मभावोंसे मुक्त होकर अपने परम कल्याणस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ।।३।।
अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम् ।
नारदस्य च संवादं ऋषेर्नारायणस्य च ॥ ४ ॥
इस विषयमें मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथाके साथ स्वयं भगवान् नारायणका सम्बन्ध है। वह गाथा देवर्षि नारद और ऋषिश्रेष्ठ नारायणका संवाद है ।।४।।
एकदा नारदो लोकान् पर्यटन् भगवत्प्रियः ।
सनातनमृषिं द्रष्टुं ययौ नारायणाश्रमम् ॥ ५ ॥
एक समयकी बात है, भगवान्के प्यारे भक्त देवर्षि नारदजी विभिन्न लोकोंमें विचरण करते हुए सनातनऋषि भगवान् नारायणका दर्शन करनेके लिये बदरिकाश्रम गये ||५||
यो वै भारतवर्षेऽस्मिन् क्शेमाय स्वस्तये नृणाम् ।
धर्मज्ञानशमोपेतं आकल्पादास्थितस्तपः ॥ ६ ॥
भगवान् नारायण मनुष्योंके अभ्युदय (लौकिक कल्याण) और परम निःश्रेयस (भगवत्स्वरूप अथवा मोक्षकी प्राप्ति के लिये इस भारतवर्षमें कल्पके प्रारम्भसे ही धर्म, ज्ञान और संयमके साथ महान् तपस्या कर रहे हैं ।।६।।
तत्रोपविष्टं ऋषिभिः कलापग्रामवासिभिः ।
परीतं प्रणतोऽपृच्छद् इदमेव कुरूद्वह ॥ ७ ॥
परीक्षित्! एक दिन वे कलापग्रामवासी सिद्ध ऋषियोंके बीचमें बैठे हुए थे। उस समय नारदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे यही प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ||७||
तस्मै ह्यवोचद्भगवान् ऋषीणां श्रृणतामिदम् ।
यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम् ॥ ८ ॥
भगवान् नारायणने ऋषियोंकी उस भरी सभामें नारदजीको उनके प्रश्नका उत्तर दिया और वह कथा सुनायी, जो पूर्वकालीन जनलोकनिवासियोंमें परस्पर वेदोंके तात्पर्य और ब्रह्मके स्वरूपके सम्बन्धमें विचार करते समय कही गयी थी ।।८।।
श्रीभगवानुवाच –
स्वायम्भुव ब्रह्मसत्रं जनलोकेऽभवत् पुरा ।
तत्रस्थानां मानसानां मुनीनां ऊर्ध्वरेतसाम् ॥ ९ ॥
भगवान् नारायणने कहा-नारदजी! प्राचीन कालकी बात है। एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले ब्रह्माके मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक, सनन्दन, सनातन आदि परमर्षियोंका ब्रह्मसत्र (ब्रह्मविषयक विचार या प्रवचन) हुआ था ।।९।।
श्वेतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टुं तदीश्वरम् ।
ब्रह्मवादः सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते ।
तत्र हायमभूत्प्रश्नस्त्वं मां यमनुपृच्छसि ॥ १० ॥
उस समय तुम मेरी श्वेतद्वीपाधिपति अनिरुद्ध-मूर्तिका दर्शन करनेके लिये श्वेतद्वीप चले गये थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्मके सम्बन्धमें बड़ी ही सुन्दर चर्चा हुई थी, जिसके विषयमें श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तात्पर्यरूपसे लक्षित कराती हई उसीमें सो जाती हैं। उस ब्रह्मसत्रमें यही प्रश्न उपस्थित किया गया था, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ।।१०।।
तुल्यश्रुततपःशीलाः तुल्यस्वीयारिमध्यमाः ।
अपि चक्रुः प्रवचनं एकं शुश्रूषवोऽपरे ॥ ११ ॥
सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार—ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील-स्वभावमें समान हैं। उन लोगोंकी दष्टिमें शत्रु, मित्र और उदासीन एक-से हैं। फिर भी उन्होंने अपनेमेंसे सनन्दनको तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुननेके इच्छुक बनकर बैठ गये ।।११।।
श्रीसनन्दन उवाच –
स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः ।
तदन्ते बोधयां चक्रुः तल्लिङ्गैः श्रुतयः परम् ॥ १२ ॥
यथा शयानं सम्राजं वन्दिनस्तत्पराक्रमैः ।
प्रत्यूषेऽभेत्य सुश्लोकैः बोधयन्त्यनुजीविनः ॥ १३ ॥
सनन्दनजीने कहा-जिस प्रकार प्रातःकाल होनेपर सोते हुए सम्राटको जगानेके लिये अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट्के पराक्रम तथा सुयशका गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाये हुए सम्पूर्ण जगत्को अपने में लीन करके अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते हैं; तब प्रलयके अन्तमें श्रतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले वचनोंसे उन्हें इस प्रकार जगाती हैं ।।१२-१३।।
श्रीश्रुतय ऊचुः –
( अवितथ गाथा –
पुढील, म्हणजे १४ ते ४१ या श्लोकांना वेदस्तुति म्हणतात )
जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां
त्वमसि यदात्मना समवरुद्धसमस्तभगः ।
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक ते
क्वचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽनुचरेन्निगमः ॥ १४ ॥
श्रुतियाँ कहती हैं-अजित! आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो, जय हो। प्रभो! आप स्वभावसे ही समस्त ऐश्वर्योंसे पूर्ण हैं, इसलिये चराचर प्राणियोंको फँसानेवाली मायाका नाश कर दीजिये। प्रभो! इस गुणमयी मायाने दोषके लिये-जीवोंके आनन्दादिमय सहज स्वरूपका आच्छादन करके उन्हें बन्धनमें डालनेके लिये ही सत्त्वादि गुणोंको ग्रहण किया है। जगत्में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन सबको जगानेवाले आप ही हैं। इसलिये आपके मिटाये बिना यह माया मिट नहीं सकती। (इस विषयमें यदि प्रमाण पूछा जाय, तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही हम ही प्रमाण हैं।) यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप मायाके द्वारा जगत्की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूपस्थितिकी लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीविग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यत्किंचित् आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं ।।१४।।
बृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया
यत उदयास्तमयौ विकृतेर्मृदि वाविकृतात् ।
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं
कथमयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम् ॥ १५ ॥
इसमें सन्देह नहीं कि हमारे द्वारा इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका भी वर्णन किया जाता है, परन्तु हमारे (श्रुतियोंके) सारे मन्त्र अथवा सभी मन्त्रद्रष्टा ऋषि प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगत्को ब्रह्मस्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय यह सारा जगत् नहीं रहता, उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराव (मिट्टीका प्याला-कसोरा) आदि सभी विकार मिट्टीसे ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्ति और प्रलय आपमें ही होती है। तब क्या आप पृथ्वीके समान विकारी हैं? नहीं-नहीं, आप तो एकरस-निर्विकार हैं। इसीसे तो यह जगत् आपमें उत्पन्न नहीं, प्रतीत है। इसलिये जैसे घट, शराव आदिका वर्णन भी मिटीका ही वर्णन है, वैसे ही इन्द्र, वरुण आदि देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि, मनसे जो कुछ सोचा जाता है और वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, उसे आपमें ही स्थित, आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे-ईंट, पत्थर या काठपर-होगा वह पृथ्वीपर ही; क्योंकि वे सब पृथ्वीस्वरूप ही हैं। इसलिये हम चाहे जिस नाम या जिस रूपका वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका ही रूप है ।।१५।।
इति तव सूरयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमल
क्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः ।
किमुत पुनः स्वधामविधुताशयकालगुणाः
परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम् ॥ १६ ॥
भगवन्! लोग सत्त्व, रज, तम—इन तीन गुणोंकी मायासे बने हुए अच्छे-बुरे भावों या अच्छी-बुरी क्रियाओंमें उलझ जाया करते हैं, परन्तु आप तो उस मायानटीके स्वामी, उसको नचानेवाले हैं। इसीलिये विचारशील पुरुष आपकी लीलाकथाके अमृतसागरमें गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप-तापको धो-बहा देते हैं। क्यों न हो, आपकी लीला-कथा सभी जीवोंके मायामलको नष्ट करनेवाली जो है। पुरुषोत्तम! जिन महापुरुषोंने आत्मज्ञानके द्वारा अन्तःकरणके राग-द्वेष आदि और शरीरके कालकृत जरा-मरण आदि दोष मिटा दिये हैं और निरन्तर आपके उस स्वरूपकी अनुभूतिमें मग्न रहते हैं, जो अखण्ड आनन्दस्वरूप है, उन्होंने अपने पाप-तापोंको सदाके लिये शान्त, भस्म कर दिया है—इसके विषयमें तो कहना ही क्या है ।।१६।।
दृतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा
महदहमादयोऽण्डमसृजन् यदनुग्रहतः
पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः
सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम् ॥ १७ ॥
भगवन्! प्राणधारियोंके जीवनकी सफलता इसीमें है कि वे आपका भजन-सेवन करें, आपकी आज्ञाका पालन करें; यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीरमें श्वासका चलना ठीक वैसा ही है, जैसा लुहारकी धौंकनीमें हवाका आना-जाना। महत्तत्त्व, अहंकार आदिने आपके अनग्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर ही इस ब्रह्माण्डकी सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय-इन पाँचों कोशोंमें पुरुष-रूपसे रहनेवाले, उनमें ‘मैं-मैं’ की स्फर्ति करनेवाले भी आप ही हैं! आपके ही अस्तित्वसे उन कोशोंके अस्तित्वका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सबमें अन्वित और सबकी अवधि होनेपर भी आप असंग ही हैं। क्योंकि वास्तवमें जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्ति अथवा नास्तिके रूपमें अनुभव होता है, उन समस्त कार्यकारणोंसे आप परे हैं। ‘नेति-नेति’ के द्वारा इन सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेधके भी साक्षी हैं और वास्तवमें आप ही एकमात्र सत्य हैं (इसलिये आपके भजनके बिना जीवका जीवन व्यर्थ ही है, क्योंकि वह इस महान् सत्यसे वंचित है)* ।।१७।।
उदरमुपासते य ऋषिवर्त्मसु कूर्पदृशः
परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम् ।
तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं
पुनरिह यत्समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे ॥ १८ ॥
ऋषियोंने आपकी प्राप्तिके लिये अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो स्थूल दृष्टिवाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमें अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं। अरुणवंशके ऋषि समस्त नाड़ियोंके निकलनेके स्थान हृदयमें आपके परम सूक्ष्मस्वरूप दहर ब्रह्मकी उपासना करते हैं। प्रभो! हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरन्ध्रतकगयी हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्गको प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपरकी ओर बढता है, वह फिर जन्म-मत्यके चक्करमें नहीं पडता* ।।१८।।
स्वकृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया
तरतमतश्चकास्स्यनलवत् स्वकृतानुकृतिः ।
अथ वितथास्वमूष्ववितथां तव धाम समं
विरजधियोऽनुयन्त्यभिविपण्यव एकरसम् ॥ १९ ॥
भगवन! आपने ही देवता, मनुष्य और पशु-पक्षी आदि योनियाँ बनायी हैं। सदा-सर्वत्र सब रूपोंमें आप हैं ही, इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न करनेपर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो उसमें प्रविष्ट हए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियोंका अनुकरण करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे प्रतीत होते हैं, जैसे आग छोटी-बड़ी लकड़ियों और कर्मोंके अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाणमें या उत्तम-अधमरूपमें प्रतीत होती है। इसलिये संत पुरुष लौकिक-पारलौकिक कर्मोंकी दूकानदारीसे, उनके फलोंसे विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धिसे सत्य-असत्य, आत्मा-अनात्माको पहचानकर जगत्के झूठे रूपोंमें नहीं फँसते; आपके सर्वत्र एकरस, समभावसे स्थित सत्यस्वरूपका साक्षात्कार करते हैं ||१९||
स्वकृतपुरेष्वमीष्वबहिरन्तरसंवरणं
तव पुरुषं वदन्त्यखिलशक्तिधृतोंऽशकृतम् ।
इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं
भवत उपासतेऽङ्घ्रिमभवम्भुवि विश्वसिताः ॥ २० ॥
प्रभो! जीव जिन शरीरों में रहता है, वे उसके कर्मके द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तवमें उन शरीरोंके कार्य-कारणरूप आवरणोंसे वह रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणोंकी सत्ता ही नहीं है। तत्त्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियोंको धारण करनेवाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होनेके कारण अंश न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होनेपर भी निर्मित कहते हैं। इसीसे बुद्धिमान् पुरुष जीवके वास्तविक स्वरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ आपके चरणकमलोंकी उपासना करते हैं। क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मोंके समर्पणस्थान और मोक्षस्वरूप हैं ||२०||
दुरवगमात्मतत्त्वनिगमाय तवात्ततनोः
चरितमहामृताब्धिपरिवर्तपरिश्रमणाः ।
न परिलषन्ति केचिदपवर्गमपीश्वर ते
चरणसरोजहंसकुलसङ्गविसृष्टगृहाः ॥ २१ ॥
भगवन्! परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है। उसीका ज्ञान करानेके लिये आप विविध प्रकारके अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं, जो अमतके महासागरसे भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानन्दमें मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, जो आपकी लीला-कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी अभिलाषा नहीं करते-स्वर्ग आदिकी तो बात ही क्या है। वे आपके चरणकमलोंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा होती है, इतना सुखमानते हैं कि उसके लिये इस जीवनमें प्राप्त अपनी घर-गृहस्थीका भी परित्याग कर देते हैं ||२१||
त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहृत्प्रियवत्
चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च ।
न बत रमन्त्यहो असदुपासनयात्महनो
यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीरभृतः ॥ २२ ॥
प्रभो! यह शरीर आपकी सेवाका साधन होकर जब आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा, हितैषी, सुहृद् और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता है। आप जीवके सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा-सर्वदा जीवको अपनानेके लिये तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होनेपर तथा अनुकूल मानव-शरीरको पाकर भी लोग सख्यभाव आदिके द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आपमें नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत् शरीर तथा उसके सम्बन्धियोंमें ही रम जाते हैं, उन्हींकी उपासना करने लगते हैं और इस प्रकार अपने आत्माका हनन करते हैं, उसे अधोगतिमें पहँचाते हैं। भला, यह कितने कष्टकी बात है! इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, सारी वासनाएँ शरीर आदिमें ही लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु-पक्षी आदिके न जाने कितने बुरे-बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यन्त भयावह जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है ।।२२।।
निभृतमरुन्मनोऽक्षदृढयोगयुजो हृदि यत्
मुनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात् ।
स्त्रिय उरगेन्द्रभोगभुजदण्डविषक्तधियो
वयमपि ते समाः समदृशोऽङ्घ्रिसरोजसुधाः ॥ २३ ॥
प्रभो! बडे-बडे विचारशील योगी-यति अपने प्राण, मन और इन्द्रियोंको वशमें करके दढ़ योगाभ्यासके द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते हैं। परन्तु आश्चर्यकी बात तो यह है कि उन्हें जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसीकी प्राप्ति उन शत्रओंको भी हो जाती है, जो आपसे वैर-भाव रखते हैं। क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँतककहें, भगवन्! वे स्त्रियाँ, जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनागके समान मोटी, लम्बी तथा सकमार भुजाओंके प्रति कामभावसे आसक्त रहती हैं, जिस परम पदको प्राप्त करती हैं, वही पद हम श्रुतियोंको भी प्राप्त होता है यद्यपि हम आपको सदा-सर्वदा एकरस अनुभव करती हैं और आपके चरणारविन्दका मकरन्दरस पान करती रहती हैं। क्यों न हो, आप समदर्शी जो हैं। आपकी दृष्टिमें उपासकके परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न भावमें कोई अन्तर नहीं है ।।२३।।
क इह नु वेद बतावरजन्मलयोऽग्रसरं
यत उदगादृषिर्यमनु देवगणा उभये ।
तर्हि न सन्न चासदुभयं न च कालजवः
किमपि न तत्र शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा ॥ २४ ॥
भगवन्! आप अनादि और अनन्त हैं। जिसका जन्म और मृत्यु कालसे सीमित है, वह भला, आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्माजी, निवृत्तिपरायण सनकादि तथा प्रवृत्तिपरायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके। क्योंकि उस समय न तो आकाशादि स्थूल जगत् रहता है और न तो महत्तत्त्वादि सूक्ष्म जगत्। इन दोनोंसे बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण-मुहूर्त आदि कालके अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता। यहाँतक कि शास्त्र भी आपमें ही समा जाते हैं (ऐसी अवस्थामें आपको जाननेकी चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है।)* ।।२४।।
जनिमसतः सतो मृतिमुतात्मनि ये च भिदां
विपणमृतं स्मरन्त्युपदिशन्ति त आरुपितैः ।
त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता
त्वयि न ततः परत्र स भवेदवबोधरसे ॥ २५ ॥
प्रभो! कुछ लोग मानते हैं कि असत् जगत्की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत्-रूप दुःखोंका नाश होनेपर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्माको अनेक मानते हैं, तो कई लोग कर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक और परलोकरूप व्यवहारको सत्य मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये सभी बातें भ्रममूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है—इस प्रकारका भेदभाव केवल अज्ञानसे ही होता है और आप अज्ञानसे सर्वथा परे हैं। इसलिये ज्ञानस्वरूप आपमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं है। ||२५||
सदिव मनस्त्रिवृत्त्वयि विभात्यसदामनुजात्
सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयाऽत्मविदः ।
न हि विकृतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया
स्वकृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितम् ॥ २६ ॥
यह त्रिगुणात्मक जगत् मनकी कल्पनामात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत्से पृथक प्रतीत होनेवाला पुरुष भी कल्पनामात्र ही है। इस प्रकार वास्तवमें असत् होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ताके कारण यह सत्य-सा प्रतीत हो रहा है। इसलिये भोक्ता, भोग्य और दोनोंके सम्बन्धको सिद्ध करनेवाली इन्द्रियाँ आदि जितना भी जगत् है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्मरूपसे सत्य ही मानते हैं। सोनेसे बने हुए कड़े, कुण्डल आदि स्वर्णरूप ही तो हैं; इसलिये उनको इस रूपमें जाननेवाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता है कि यह भी सोना है। इसी प्रकार यह जगत् आत्मामें ही कल्पित, आत्मासे ही व्याप्त है; इसलिये आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं ||२६||
तव परि ये चरन्त्यखिलसत्त्वनिकेततया
त उत पदाक्रमन्त्यविगणय्य शिरो निर्ऋतेः ।
परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तान्
त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विमुखाः ॥ २७ ॥
भगवन्! जो लोग यह समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्मभावसे आपका भजन-सेवन करते हैं, वे मृत्युको तुच्छ समझकर उसके सिरपर लात मारते हैं अर्थात् उसपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान् हों, उन्हें आप कर्मोंका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसे पशुओंके समान बाँध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रखा है, वे न केवल अपनेको बल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते हैं-जगत्के बन्धनसे छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला, आपसे विमुख लोगोंको कैसे प्राप्त हो सकता है ||२७||
त्वमकरणः स्वराडखिलकारकशक्तिधरः
तव बलिमुद्वहन्ति समदन्त्यजयानिमिषाः ।
वर्षभुजोऽखिलक्षितिपतेरिव विश्वसृजो
विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः ॥ २८ ॥
प्रभो! आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि करणोंसे–चिन्तन, कर्म आदिकेसाधनोंसे सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणोंकी शक्तियोंसे सदा-सर्वदा सम्पन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान्, स्वयंप्रकाश हैं; अतः कोई काम करनेके लिये आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे-छोटे राजा अपनी-अपनी प्रजासे कर लेकर स्वयं अपने सम्राट्को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्योंके पूज्य देवता और देवताओंके पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियोंसे पूजा स्वीकार करते हैं और मायाके अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करनेके लिये उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वह काम करते रहते हैं ।।२८।।
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो
विहर उदीक्षया यदि परस्य विमुक्त ततः ।
न हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेद्
वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥ २९ ॥
नित्यमुक्त! आप मायातीत हैं, फिर भी जब अपने ईक्षणमात्रसे—संकल्पमात्रसे मायाके साथ क्रीडा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवोंके सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म-संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है। प्रभो! आप परम दयालु हैं। आकाशके समान सबमें सम होनेके कारण न तो कोई आपका अपना है और न तो पराया। वास्तवमें तो आपके स्वरूपमें मन और वाणीकी गति ही नहीं है। आपमें कार्य-कारणरूप प्रपंचका अभाव होनेसे बाह्य दृष्टिसे आप शून्यके समान ही जान पड़ते हैं; परन्तु उस दृष्टिके भी अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य हैं ।।२९।।
अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगताः
तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रव नेतरथा ।
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तृ भवेत्
सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥ ३० ॥
भगवन्! आप नित्य एकरस हैं। यदि जीव असंख्य हों और सब-के-सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों, तब तो वे आपके समान ही हो जायँगे; उस हालतमें वे शासित हैं और आप शासक-यह बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियन्त्रण आप तभी कर सकते हैं, जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्यून हों। इसमें सन्देह नहीं कि ये सब-के-सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिये आप उनमें कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तवमें आप उनमें समरूपसे स्थित हैं। परन्तु यह जाना नहीं जा सकता कि आपका वह स्वरूप कैसा है। क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तवमें आपको नहीं जाना; उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धिके विषयको जाना है, जिससे आप परे हैं। और साथ ही मतिके द्वारा जितनी वस्तुएँ जानीजाती हैं, वे मतियोंकी भिन्नताके कारण भिन्न-भिन्न होती हैं; इसलिये उनकी दुष्टता, एक मतके साथ दूसरे मतका विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतोंके परे है ||३०||
न घटत उद्भवः प्रकृतिपूरुषयोरजयोः
उभययुजा भवन्त्यसुभृतो जलबुद्बुदवत् ।
त्वयि त इमे ततो विविधनामगुणैः परमे
सरित इवार्णवे मधुनि लिल्युरशेषरसाः ॥ ३१ ॥
स्वामिन्! जीव आपसे उत्पन्न होता है, यह कहनेका ऐसा अर्थ नहीं है कि आप परिणामके द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धान्त तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं। अर्थात् उनका वास्तविक स्वरूप-जो आप हैं-कभी वृत्तियोंके अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तब प्राणियोंका जन्म कैसे होता है? अज्ञानके कारण प्रकृतिको पुरुष और पुरुषको प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दूसरेके साथ संयोग हो जानेसे जैसे ‘बुलबुला’ नामकी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है, परन्तु उपादान-कारण जल और निमित्त-कारण वायुके संयोगसे उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृतिका अध्यास (एकमें दूसरेकी कल्पना) हो जानेके कारण ही जीवोंके विविध नाम और गुण रख लिये जाते हैं। अन्तमें जैसे समुद्रमें नदियाँ और मधुमें समस्त पुष्पोंके रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब-के-सब उपाधिरहित आपमें समा जाते हैं। (इसलिये जीवोंकी भिन्नता और उनका पृथक् अस्तित्व आपके द्वारा नियन्त्रित है। उनकी पृथक् स्वतन्त्रता और सर्व-व्यापकता आदि वास्तविक सत्यको न जाननेके कारण ही मानी जाती है)* ||३१।।
नृषु तव मयया भ्रमममीष्ववगत्य भृशं
त्वयि सुधियोऽभवे दधति भावमनुप्रभवम् ।
कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रुकुटिः
सृजति मुहुस्त्रिणमिरभवच्छरणेषु भयम् ॥ ३२ ॥
भगवन्! सभी जीव आपकी मायासे भ्रममें भटक रहे हैं, अपनेको आपसे पृथक् मानकर जन्म-मृत्युका चक्कर काट रहे हैं। परन्तु बुद्धिमान् पुरुष इस भ्रमको समझ लेते हैं और सम्पूर्ण भक्तिभावसे आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्ममृत्युके चक्करसे छुड़ानेवाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा—इन तीन भागोंवाला कालचक्र आपका भ्रूविलासमात्र है, वह सभीको भयभीत करता है, परन्तु वह उन्हींको बार-बार भयभीत करता है, जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला, जन्म-मृत्युरूप संसारका भय कैसे हो सकता है?’ ||३२||
विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं
य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपायखिदः ।
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं
वणिज इवाज सन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ ॥ ३३ ॥
अजन्मा प्रभो! जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और प्राणोंको वशमें कर लिया है, वे भी, जब गुरुदेवके चरणोंकी शरण न लेकर उच्छृखल एवं अत्यन्त चंचल मन-तुरंगको अपने वशमें करनेका प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनोंमें सफल नहीं होते। उन्हें बारबार खेद और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पडता है, केवल श्रम और दःख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है, जैसी समुद्रमें बिना कर्णधारकी नावपर यात्रा करनेवाले व्यापारियोंकी होती है (तात्पर्य यह कि जो मनको वशमें करना चाहते हैं, उनके लिये कर्णधार-गुरुकी अनिवार्य आवश्यकता है)* ||३३||
स्वजनसुतात्मदारधनधामधरासुरथैः
त्वयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे ।
इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां
सुखयति को न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभगे ॥ ३४ ॥
भगवन्! आप अखण्ड आनन्दस्वरूप और शरणागतोंके आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे क्या प्रयोजन है? जो लोग इस सत्य सिद्धान्तको न जानकर स्त्री-पुरुषके सम्बन्धसे होनेवाले सुखोंमें ही रम रहे हैं, उन्हें संसारमें भला, ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो सुखी कर सके। क्योंकि संसारकी सभी वस्तएँ स्वभावसे ही विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मटियामेट हो जानेवाली हैं। और तो क्या, वे स्वरूपसे ही सारहीन और सत्ताहीन हैं; वे भला, क्या सुख दे सकती हैं। ||३४||
भुवि पुरुपुण्यतीर्थसदनान्यृषयो विमदाः
त उत भवत्पदाम्बुजहृदोऽघभिदङ्घ्रिजलाः ।
दधति सकृन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे
न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान् ॥ ३५ ॥
भगवन! जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदिके घमंडसे रहित हैं, वे संतपुरुष इस पृथ्वीतलपर परम पवित्र और सबको पवित्र करनेवाले पुण्यमय सच्चे तीर्थस्थान हैं। क्योंकि उनके हृदयमें आपके चरणारविन्द सर्वदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उन संत पुरुषोंका चरणामृत समस्त पापों और तापोंको सदाके लिये नष्ट कर देनेवाला है। भगवन्! आप नित्य-आनन्दस्वरूप आत्मा ही हैं। जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं आपमें मन लगा देते हैं वे उन देह-गेहोंमें कभी नहीं फँसते जो जीवके विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शान्ति आदि गुणोंका नाश करनेवाले हैं। वे तो बस, आपमें ही रम जाते हैं ।।३५।।
सत इदं उत्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं
व्यभिचरति क्व च क्व च मृषा न तथोभययुक् ।
व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया
भ्रमयति भारती त उरुवृत्तिभिरुक्थजडान् ॥ ३६ ॥
भगवन! जैसे मिट्टीसे बना हआ घडा मिटीरूप ही होता है, वैसे ही सतसे बना हआ जगत् भी सत् ही है—यह बात युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि कारण और कार्यका निर्देश ही उनके भेदका द्योतक है। यदि केवल भेदका निषेध करनेके लिये ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्रमें, दण्ड और घटनाशमें कार्य-कारण-भाव होनेपर भी वे एक दूसरेसे भिन्न हैं। इस प्रकार कार्य-कारणकी एकता सर्वत्र एक-सी नहीं देखी जाती। यदि कारण-शब्दसे निमित्त-कारण न लेकर केवल उपादान-कारण लिया जाय-जैसे कुण्डलका सोना-तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित होती है; जैसे रस्सीमें साँप। यहाँ उपादान-कारणके सत्य होनेपर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाय कि प्रतीत होनेवाले सर्पका उपादान-कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्याका-भ्रमका मेल भी है, तो यह समझना चाहिये कि अविद्या और सत् वस्तुके संयोगसे ही इस जगत्की उत्पत्ति हुई है। इसलिये जैसे रस्सीमें प्रतीत होनेवाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत् वस्तुमें अविद्याके संयोगसे प्रतीत होनेवाला नाम-रूपात्मक जगत् भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहारकी सिद्धिके लिये ही जगत्की सत्ता अभीष्ट हो, सत्य है। यह भ्रम व्यावहारिक जगत्में माने हुए कालकी दृष्टिसे अनादि है; और अज्ञानीजन बिना विचार किये पूर्व-पूर्वके भ्रमसे प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थितिमें कर्मफलको सत्य बतलानेवाली श्रृतियाँ केवल उन्हीं लोगोंको भ्रममें डालती हैं, जो कर्ममें जड हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्मफलकी नित्यता बतलानेमें नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगानेमें है ।।३६।।
न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनाद्
अनु मितमन्तरा त्वयि विभाति मृषैकरसे ।
अत उपमीयते द्रविणजातिविकल्पपथैः
वितथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यबुधाः ॥ ३७ ॥
भगवन्! वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत् उत्पत्तिके पहले नहीं था और प्रलयके बाद नहीं रहेगा; इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीचमें भी एकरस परमात्मामें मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसीसे हम श्रुतियाँ इस जगत्का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टीमें घड़ा, लोहेमें शस्त्र और सोने में कुण्डल आदि नाममात्र हैं, वास्तवमें मिट्टी, लोहा और सोना ही हैं। वैसे ही परमात्मामें वर्णित जगत् नाममात्र है, सर्वथा मिथ्या और मनकी कल्पना है। इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं ||३७।।
स यदजया त्वजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्
भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः ।
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभगो
महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः ॥ ३८ ॥
भगवन्! जब जीव मायासे मोहित होकर अविद्याको अपना लेता है, उस समय – उसके स्वरूपभूत आनन्दादि गुण ढक जाते हैं; वह गुणजन्य वृत्तियों, इन्द्रियों और देहोंमें फँस जाता है तथा उन्हींको अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म-मृत्युमें अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके चक्करमें पड़ जाता है। परन्तु प्रभो! जैसे साँप अपने केंचुलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता हैवैसे ही आप माया-अविद्यासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, उसे सदा-सर्वदा छोडे रहते हैं। इसीसे आपके सम्पूर्ण ऐश्वर्य, सदा-सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अणिमा आदि अष्टसिद्धियोंसे युक्त परमैश्वर्यमें आपकी स्थिति है। इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनन्त है; वह देश, काल और वस्तुओंकी सीमासे आबद्ध नहीं है ||३८।।
यदि न समुद्धरन्ति यतयो हृदि कामजटा
दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्मृतकण्ठमणिः ।
असुतृपयोगिनामुभयतोऽप्यसुखं भगवन्न्
अनपगतान्तकादनधिरूढपदाद्भवतः ॥ ३९ ॥
भगवन! यदि मनष्य योगी-यति होकर भी अपने हृदयकी विषय-वासनाओंको उखाड़ नहीं फेंकते तो उन असाधकोंके लिये आप हृदयमें रहनेपर भी वैसे ही दुर्लभ हैं, जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परन्तु उसकी याद न रहनेपर उसे ढूँढ़ता फिरे इधर-उधर। जो साधक अपनी इन्द्रियोंको तप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयोंसे विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवनभर और जीवनके बाद भी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है। क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्युसे छुटकारा नहीं मिला है, लोगोंको रिझाने, धन कमाने आदिके क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप न जाननेके कारण अपने धर्म-कर्मका उल्लंघन करनेसे परलोकमें नरक आदि प्राप्तहोनेका भय भी बना ही रहता है ।।३९।।
त्वदवगमी न वेत्ति भवदुत्थशुभाशुभयोः
गुणविगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः ।
अनुयुगमन्वहं सगुण गीतपरम्परया
श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः ॥ ४० ॥
भगवन्! आपके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाला पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और पाप-कर्मोंके फल सुख एवं दुःखोंको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य और भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि-निषेधके प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निवृत्त हो जाते हैं; क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिये हैं। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युगमें की हुई लीलाओं, गुणोंका गान सुन-सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदयमें बैठा लेता है तो अनन्त, अचिन्त्य, दिव्यगुणगणोंके निवासस्थान प्रभो! आपका वह प्रेमी भक्त भी पाप-पुण्योंके फल सुख-दुःखों और विधि-निषेधोंसे अतीत हो जाता है। क्योंकि आप ही उनकी मोक्षस्वरूप गति हैं। (परन्तु इन ज्ञानी और प्रेमियोंको छोड़कर और सभी शास्त्र बन्धनमें हैं तथा वे उसका उल्लंघन करनेपर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं)* ।।४०।।
द्युपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया
त्वमपि यदन्तराण्डनिचया ननु सावरणाः ।
ख इव रजांसि वान्ति वयसा सह यत् श्रुतयः
त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवन्निधनाः ॥ ४१ ॥
भगवन्! स्वर्गादि लोकोंके अधिपति इन्द्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी थाह-आपका पार न पा सके; और आश्चर्यकी बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते। क्योंकि जब अन्त है ही नहीं, तब कोई जानेगा कैसे? प्रभो! जैसे आकाशमें हवासे धूलके नन्हेंनन्हें कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आपमें कालके वेगसे अपनेसे उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरणोंके सहित असंख्य ब्रह्माण्ड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला, आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियाँ भी आपके स्वरूपका साक्षात् वर्णन नहीं कर सकतीं, आपके अतिरिक्त वस्तुओंका निषेध करते-करते अन्तमें अपना भी निषेध कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं ।।४१।।
श्रीभगवानुवाच –
( अनुष्टुप् )
इत्येतद्ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मानुशासनम् ।
सनन्दनमथानर्चुः सिद्धा ज्ञात्वाऽऽत्मनो गतिम् ॥ ४२ ॥
भगवान् नारायणने कहा-देवर्षे! इस प्रकार सनकादि ऋषियोंने आत्मा और ब्रह्मकी एकता बतलानेवाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूपको जाना और नित्य सिद्ध होनेपर भी इस उपदेशसे कृतकृत्य-से होकर उन लोगोंने सनन्दनकी पूजा की ।।४२।।
इत्यशेषसमाम्नाय पुराणोपनिषद्रसः ।
समुद्धृतः पूर्वजातैः व्योमयानैर्महात्मभिः ॥ ४३ ॥
नारद! सनकादि ऋषि सृष्टिके आरम्भमें उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओंने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़ लिया है, यह सबका सार-सर्वस्व है ।।४३।।
त्वं चैतद्ब्रह्मदायाद श्रद्धयाऽऽत्मानुशासनम् ।
धारयंश्चर गां कामं कामानां भर्जनं नृणाम् ॥ ४४ ॥
देवर्षे! तुम भी उन्हींके समान ब्रह्माके मानस-पुत्र हो–उनकी ज्ञान-सम्पत्तिके उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धाके साथ इस ब्रह्मात्मविद्याको धारण करो और स्वच्छन्दभावसे पृथ्वीमें विचरण करो। यह विद्या मनुष्योंकी समस्त वासनाओंको भस्म कर देनेवाली है ।।४४।।
श्रीशुक उवाच –
एवं स ऋषिणाऽऽदिष्टं गृहीत्वा श्रद्धयात्मवान् ।
पूर्णः श्रुतधरो राजन् आह वीरव्रतो मुनिः ॥ ४५ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्णकाम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान् नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया, तब उन्होंने बड़ी श्रद्धासे उसे ग्रहण किया और उनसे यह कहा ।।४५।।
श्रीनारद उवाच –
नमस्तस्मै भगवते कृष्णायामलकीर्तये ।
यो धत्ते सर्वभूतानां अभवायोशतीः कलाः ॥ ४६ ॥
देवर्षि नारदने कहा-भगवन! आप सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियोंके परम कल्याण-मोक्षके लिये कमनीय कलावतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।।४६।।
इत्याद्यमृषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः ।
ततोऽगाद् आश्रमं साक्षात् पितुर्द्वैपायनस्य मे ॥ ४७ ॥
परीक्षित! इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद आदि ऋषि भगवान नारायणको और उनके शिष्योंको नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्रीकृष्णद्वैपायनके आश्रमपर गये ।।४७।।
सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः ।
तस्मै तद् वर्णयामास नारायणमुखाच्छ्रुतम् ॥ ४८ ॥
भगवान् वेदव्यासने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गये, इसके बाद देवर्षि नारदने जो कुछ भगवान् नारायणके मुँहसे सुना था, वह सब कुछ मेरे पिताजीको सुना दिया ।।४८।।
इत्येतद् वर्णितं राजन् यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया ।
यथा ब्रह्मण्यनिर्देश्ये नीऋगुणेऽपि मनश्चरेत् ॥ ४९ ॥
राजन्! इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन-वाणीसे अगोचर और समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित परब्रह्म परमात्माका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं और उसमें मनका कैसे प्रवेश होता है? यही तो तुम्हारा
प्रश्न था ।।४९।।
( शार्दूलविक्रीडित )
योऽस्योत्प्रेक्षक आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो
यः सृष्ट्वेदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्रे पुरः शास्ति ताः ।
यं सम्पद्य जहात्यजामनुशयी सुप्तः कुलायं यथा
तं कैवल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्रं हरिम् ॥ ५० ॥
परीक्षित्! भगवान् ही इस विश्वका संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अन्तमें स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनोंके स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सष्टि करके जीवके साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरोंका निर्माण करके वे ही उनका नियन्त्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा-सुषुप्तिमें मग्न पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान्को पाकर यह जीव मायासे मुक्त हो जाता है। भगवान् ऐसे विशुद्ध, केवल चिन्मात्र तत्त्व हैं कि उनमें जगत्के कारण माया अथवा । प्रकृतिका रत्तीभर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तवमें अभय-स्थान हैं। उनका चिन्तन निरन्तर करते रहना चाहिये ।।५०।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां
संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे
वेदस्तुति नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥