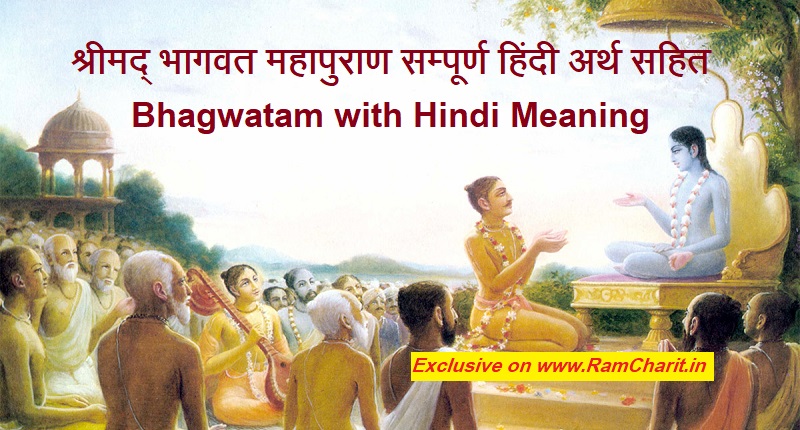श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 11 अध्याय 18
18 CHAPTER
श्रीमद्भागवतपुराणम्/स्कन्धः ११/अध्यायः १८
वानप्रस्थ संन्यासाश्रमधर्म निरूपणम् –
श्रीभगवानुवाच –
( अनुष्टुप् )
वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्यां न्यस्य सहैव वा ।
वन एव वसेत् शान्तः तृतीयं भागमायुषः ॥ १ ॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय उद्धव! यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोंके हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे ।।१।।
कन्दमूलफलैः वन्यैः मेध्यैः वृत्तिं प्रकल्पयेत् ।
वसीत वल्कलं वासः तृणपर्णाजिनानि च ॥ २ ॥
उसे वनके पवित्र कन्द-मूल और फलोंसे ही शरीर-निर्वाह करना चाहिये; वस्त्रकी जगह वृक्षोंकी छाल पहिने अथवा घास-पात और मृगछालासे ही काम निकाल ले ||२||
केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिभृयाद् दतः ।
न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः ॥ ३ ॥
केश, रोएँ, नख और मूंछदाढ़ीरूप शरीरके मलको हटावे नहीं। दातुन न करे। जलमें घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरतीपर ही पड़ रहे ।।३।।
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन् वर्षास्वासारषाड् जले ।
आकण्ठमग्नः शिशिरे एवंवृत्तस्तपश्चरेत् ॥ ४ ॥
ग्रीष्म ऋतुमें पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें रहकर वर्षाकी बौछार सहे। जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जलमें डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ||४||
अग्निपक्वं समश्नीयात् कालपक्वमथापि वा ।
उलूखलाश्मकुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा ॥ ५ ॥
कन्द-मूलोंको केवल आगमें भूनकर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटनेकी आवश्यकता हो तो ओखलीमें या सिलपर कूट ले, अन्यथा दाँतोंसे ही चबा-चबाकर खा ले ||५||
स्वयं सञ्चिनुयात् सर्वम् आत्मनो वृत्तिकारणम् ।
देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाऽऽहृतम् ॥ ६ ॥
वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैंइन बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये स्वयं ही सब प्रकारके कन्द-मूल-फल आदि ले आवे। देश-काल आदिसे अनभिज्ञ लोगोंसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके संचित पदार्थोंको अपने काममें न ले* ।।६।।
वन्यैश्चरु-पुरोडाशैः निर्वपेत् कालचोदितान् ।
न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७ ॥
नीवार आदि जंगली अन्नसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जानेपरवेदविहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न करे ||७||
अग्निहोत्रं च दर्शश्च पौर्णमासश्च पूर्ववत् ।
चातुर्मास्यानि च मुनेः आम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ ॥
वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोंके लिये है ||८||
एवं चीर्णेन तपसा मुनिः र्धमनिसंततः ।
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम् ॥ ९ ॥
इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जानेके कारण वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने लगती है। वह इस तपस्याके द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके लोकमें जाता है और वहाँसे फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है ।।९।।
यस्त्वेतत्कृच्छ्रतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत् ।
कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद् बालिशः कोऽपरस्ततः ॥ १० ॥
प्रिय उद्धव! जो पुरुष बड़े कष्टसे किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान तपस्याको स्वर्ग, ब्रह्मलोक आदि छोटे-मोटे फलोंकी प्राप्तिके लिये करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा? इसलिये तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये ।।१०।।
यदासौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः ।
आत्मन्यग्नीन् समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत् ॥ ११ ॥
प्यारे उद्धव! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमोंका पालन करने में असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके कारण उसका शरीर काँपने लगे, तब यज्ञाग्नियोंको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें लगाकर अग्निमें प्रवेश कर जाय। (यह विधान केवल उनके लिये है, जो विरक्त नहीं हैं) ।।११।।
यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु ।
विरागो जायते सम्यङ् न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत्ततः ॥ १२ ॥
यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि काम्य कर्मोंसे उनके फलस्वरूप जो लोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोंके समान ही दुःखपूर्ण हैं और मनमें लोक-परलोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक यज्ञाग्नियोंका परित्याग करके संन्यास ले ले ।।१२।।
इष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे ।
अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत् ॥ १३ ॥
जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार आठों प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विजको दे दे। यज्ञाग्नियोंको अपने प्राणोंमें लीन कर ले और फिर किसी भीस्थान, वस्तु और व्यक्तियोंकी अपेक्षा न रखकर स्वच्छन्द विचरण करे ।।१३।।
विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः ।
विघ्नान् कुर्वन्त्ययं ह्यस्मान् आक्रम्य समियात् परम् ॥ १४ ॥
उद्धवजी! जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तब देवतालोग स्त्री-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंका रूप धारण करके उसके संन्यास-ग्रहणमें विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि ‘अरे! यह तो हमलोगोंकी अवहेलना कर, हमलोगोंको लाँघकर परमात्माको प्राप्त होने जा रहा है’ ।।१४।।
बिभृयाच्चेन् मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् ।
त्यक्तं न दण्डपात्राभ्याम् अन्यत् किञ्चिद् अनापदि ॥ १५ ॥
यदि संन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लँगोटी लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लँगोटी ढक जाय। तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्तिकालको छोड़कर सदाके लिये है ||१५||
दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं पिबेत् जलम् ।
सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥ १६ ॥
नेत्रोंसे धरती देखकर पैर रखे, कपड़ेसे छानकर जल पिये, मुँहसे प्रत्येक बात सत्यपूत–सत्यसे पवित्र हुई ही निकाले और शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धि-पूर्वक सोच-विचार कर ही करे ||१६||
मौनानीहानिलायामाः दण्डा वाक्-देह-चेतसाम् ।
न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिर्न भवेद् यतिः ॥ १७ ॥
वाणीके लिये मौन, शरीरके लिये निश्चेष्ट स्थिति और मनके लिये प्राणायाम दण्ड हैं। जिसके पास ये तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केवल शरीरपर बाँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी स्वामी नहीं हो जाता ।।१७।।
भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयन् चरेत् ।
सप्तागारान् असङ्क्लृप्तान् तुष्येत् लब्धेन तावता ॥ १८ ॥
संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि पतितोंको छोड़कर चारों वर्गों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित सात घरोंसे जितना मिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले ।।१८।।
बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः ।
विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीताशेषमाहृतम् ॥ १९ ॥
इसप्रकार भिक्षा लेकर बस्तीके बाहर जलाशयपर जाय, वहाँ हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले; फिर शास्त्रोक्त पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समयके लिये बचाकर न रखे और न अधिक माँगकर ही लाये ||१९||
एकश्चरेत् महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः ।
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान् समदर्शनः ॥ २० ॥
संन्यासीको पृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये। उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इन्द्रियाँ अपने वशमें हों। वह अपने-आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी धैर्य रखे और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे ।।२०।।
विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमलाशयः ।
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः ॥ २१ ॥
संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये। उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध बना रहे। वह अपने-आपको मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन करे ।।२१।।
अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ।
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥ २२ ॥
वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विक्षिप्त होना-चंचल होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ।।२२।।
तस्मान्नियम्य षड्वर्गं मद्भावेन चरेन् मुनिः ।
विरक्तः क्षुद्रकामेभ्यो लब्ध्वा आत्मनि सुखं महत् ॥ २३ ॥
इसलिये संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंको जीत ले, भोगोंकी क्षुद्रता समझकर उनकी ओरसे सर्वथा मुँह मोड़ ले और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें विचरता रहे ||२३||
पुरग्रामव्रजान् सार्थान् भिक्षार्थं प्रविशंश्चरेत् ।
पुण्यदेश सरिच्छैशैल वनाश्रमवतीं महीम् ॥ २४ ॥
केवल भिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्ती या यात्रियोंकी टोलीमें जाय। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमोंसे पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे ।।२४।।
वानप्रस्थाश्रमपदेषु अभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत् ।
संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्धसत्त्वः शिलान्धसा ॥ २५ ॥
भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही ग्रहण करे; क्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बनी हई भिक्षा शीघ्र ही चित्तको शुद्ध कर देती है और उससे बचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है ।।२५।।
नैतद् वस्तुतया पश्येद् दृश्यमानं विनश्यति ।
असक्तचित्तो विरमेद् इहामुत्र चिकीर्षितात् ॥ २६ ॥
विचारवान् संन्यासी दृश्यमान जगत्को सत्य वस्तु कभी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान् है। इस जगत्में कहीं भी अपने चित्तको लगाये नहीं। इस लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय ।।२६।।
यदेतदात्मनि जगन् मनो-वाक्-प्राण-संहतम् ।
सर्वं मायेति तर्केण स्वस्थः त्यक्त्वा न तत्स्मरेत् ॥ २७ ॥
संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका संघातरूप यह जगत् है, वह सारा-का-सारा माया ही है। इस विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे ||२७||
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वाऽनपेक्षकः ।
सलिङ्गान् आश्रमान् त्यक्त्वा चरेद् अविधिगोचरः ॥ २८ ॥
ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिह्नोंको छोड़-छाड़कर, वेद-शास्त्रके विधि-निषेधोंसे परे होकर स्वच्छन्दविचरे ।।२८।।
बुधो बालकवत् क्रीडेत् कुशलो जडवच्चरेत् ।
वदेद् उन्मत्तवद् विद्वान् गोचर्यां नैगमश्चरेत् ॥ २९ ॥
वह बुद्धिमान् होकर भी बालकोंके समान खेले। निपुण होकर भी जडवत् रहे, विद्वान् होकर भी पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे (अनियत आचारवान्) रहे ।।२९।।
वेदवादरतो न स्यात् न पाखण्डी न हैतुकः ।
शुष्कवादविवादे न कञ्चित् पक्षं समाश्रयेत् ॥ ३० ॥
उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाण्ड-भागकी व्याख्या में न लगे, पाखण्ड न करे, तर्क-वितर्कसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हो रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले ||३०||
नोद्विजेत जनाद् धीरो जनं चोद्वेजयेत् न तु ।
अतिवादान् तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ।
देहमुद्दिश्य पशुवत् वैरं कुर्यान् न केनचित् ॥ ३१ ॥
वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणीसे उद्वेग न हो और वह स्वयं भी किसी प्राणीको उद्विग्न न करे। उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह ले; किसीका अपमान न करे। प्रिय उद्धव! संन्यासी इस शरीरके लिये किसीसे भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं ।।३१।।
एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः ।
यथेदमुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥ ३२ ॥
जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए विभिन्न पात्रोंमें अलग-अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियोंमें और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक है ही, पंचभूतोंसे बने हए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पांचभौतिक ही तो हैं। (ऐसी अवस्था में किसीसे भी वैर-विरोध करना अपना ही वैरविरोध है) ||३२||
अलब्ध्वा न विषीदेत कालेकालेऽशनं क्वचित् ।
लब्ध्वा न हृष्येद्-धृतिमानुभयं दैवतं त्रितम् ॥ ३३ ॥
प्रिय उद्धव! संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर भोजन न मिले, तो उसे दुःखी नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिलता रहे, तो हर्षित न होना चाहिये। उसे चाहिये कि वह धैर्य रखे। मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्धके अधीन हैं ।।३३।।
आहारार्थं समीहेत युक्तं तत् प्राणधारणम् ।
तत्त्वं विमृश्यते तेन तद् विज्ञाय विमुच्यते ॥ ३४ ॥
भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; क्योंकि भिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती है। प्राण रहनेसे ही तत्त्वका विचार होता है और तत्त्वविचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति मिलती है ||३४||
यदृच्छयोपपन्नान्नमद्यात् श्रेष्ठमुतापरम् ।
तथा वासः तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेन् मुनिः ॥ ३५ ॥
संन्यासीको प्रारब्धके अनुसार अच्छी या बुरी-जैसी भी भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जायँ, उन्हींसे काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी कल्पना न करे ||३५||
शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत् ।
अन्यांश्च नियमान् ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः ॥ ३६ ॥
जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीलासे ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमोंका पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका लीलासे ही आचरण करे। वह शास्त्रविधिके अधीन होकर-विधि-किंकर होकर न करे ।।३६।।
न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद् वीक्षया हता ।
आ देहान्तात् क्वचित् ख्यातिः ततः संपद्यते मया ॥ ३७ ॥
क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती। जो पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गयी। यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है, तब भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है ।।३७।।
दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान् ।
अजिज्ञासित मद्धर्मो गुरुं मुनिमुपाव्रजेत् ॥ ३८ ॥
उद्धवजी! (यह तो हुई ज्ञानवान्की बात, अब केवल वैराग्यवान्की बात सुनो।) जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निश्चय हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फल दुःख-ही-दुःख है, तब वह विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राप्तिके साधनोंको न जानता हो तो भगवच्चिन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुकी शरण ग्रहण करे ||३८||
तावत् परिचरेद् भक्तः श्रद्धावान् अनसूयकः ।
यावद् ब्रह्म विजानीयान् मामेव गुरुमादृतः ॥ ३९ ॥
वह गुरुकी दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बड़े आदरसे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे ।।३९।।
यस्त्वसंयत षड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रिय सारथिः ।
ज्ञानवैराग्यरहितः त्रिदण्डमुपजीवति ॥ ४० ॥
सुरान् आत्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धर्महा ।
अविपक्वकषायोऽस्माद् अमुष्माच्च विहीयते ॥ ४१ ॥
किन्तु जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन, इन छहोंपर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथि बिगड़े हए हैं और जिसके हृदयमें न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पालता है तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओंको, अपने-आपको और अपने हृदयमें स्थित मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है। अभी उस वेषमात्रके संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं; इसलिये वह इस लोक और परलोक दोनोंसे हाथ धो बैठता है ||४०-४१।।
भिक्षोः धर्मः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वनौकसः ।
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनम् ॥ ४२ ॥
संन्यासीका मुख्य धर्म है शान्ति और अहिंसा। वानप्रस्थीका मुख्य धर्म है-तपस्या और भगवद्भाव। गृहस्थका मुख्य धर्म है-प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है-आचार्यकी सेवा ||४२||
ब्रह्मचर्यं तपः शौचं संतोषो भूतसौहृदम् ।
गृहस्थस्यापि ऋतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम् ॥ ४३ ॥
गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें ही अपनी स्त्रीका सहवास करे। उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, सन्तोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेमभाव-ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो सभीको करनी चाहिये ।।४३।।
इति मां यः स्वधर्मेण भजन् नित्यमनन्यभाक् ।
सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं विन्दते दृढाम् ॥ ४४ ॥
जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे अपने वर्णाश्रमधर्मके द्वारा मेरी सेवामें लगा रहता है और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है ||४४।।
भक्त्योद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम् ।
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः ॥ ४५ ॥
उद्धवजी! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र स्वामी, सबकी उत्पत्ति और प्रलयका परम कारण ब्रह्म हूँ। नित्य-निरन्तर बढ़नेवाली अखण्ड भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है ||४५||
इति स्वधर्मनिर्णिक्तसत्त्वो निर्ज्ञातमद्गतिः ।
ज्ञानविज्ञान सम्पन्नो न चिरात् समुपैति माम् ॥ ४६ ॥
इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणको शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्यको-मेरे स्वरूपको जान लेता है और ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है ।।४६||
वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचार लक्षणः ।
स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः ॥ ४७ ॥
मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतलाया है। यदि इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट लग जाय, तब तोइससे अनायास ही परम कल्याणस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ।।४७।।
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान् पृच्छति यच्च माम् ।
यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात् परम् ॥ ४८ ॥
साधुस्वभाव उद्धव! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्मका पालन करनेवाला भक्त मुझ परब्रह्म-स्वरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है ।।४८।।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां
संहितायां एकादशस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥