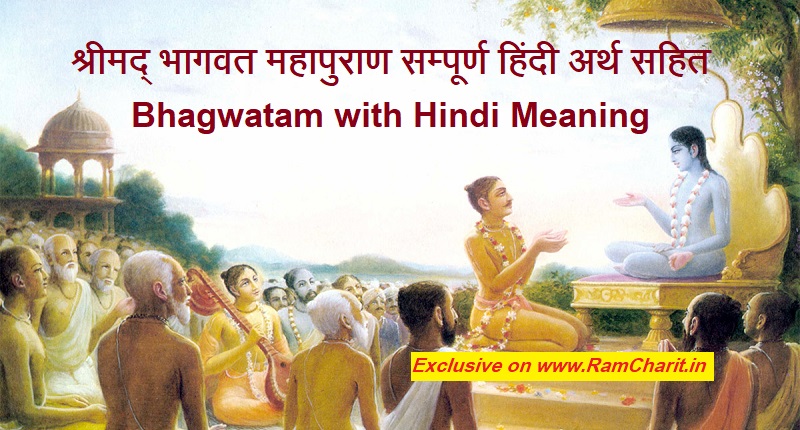श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 11 अध्याय 22
22 CHAPTER
श्रीमद्भागवतपुराणम्/स्कन्धः ११/अध्यायः २२
श्रीउद्धव उवाच।
कति तत्त्वानि विश्वेश सङ्ख्यातान्यृषिभिः प्रभो।
नवैकादश पञ्च त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम १।
उद्धवजीने कहा-प्रभो! विश्वेश्वर! ऋषियोंने तत्त्वोंकी संख्या कितनी बतलायी है? आपने तो अभी (उन्नीसवें अध्यायमें) नौ, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात् कुल अट्ठाईस तत्त्व गिनाये हैं। यह तो हम सुन चुके हैं ||१||
केचित्षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिं ।
सप्तैके नव षट्केचिच्चत्वार्येकादशापरे ।
केचित्सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश २।
किन्तु कुछ लोग छब्बीस तत्त्व बतलाते हैं तो कुछ पचीस; कोई सात, नौ अथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते हैं तो कोई ग्यारह ।।२।।
एतावत्त्वं हि सङ्ख्यानामृषयो यद्विवक्षया।
गायन्ति पृथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि ३।
इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि-मुनियोंके मतमें उनकी संख्या सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं। सनातन श्रीकृष्ण! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्रायसे बतलाते हैं? आप कृपा करके हमें बतलाइये ||३||
श्रीभगवानुवाच।
युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा।
मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम् ४।
भगवान् श्रीकृष्णने कहा-उद्धवजी! वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वहसभी ठीक है; क्योंकि सभी तत्त्व सबमें अन्तर्भूत हैं। मेरी मायाको स्वीकार करके क्या कहना असम्भव है? ||४||
नैतदेवं यथात्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा।
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ५।
‘जैसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ, वही यथार्थ है’-इस प्रकार जगत्के कारणके सम्बन्धमें विवाद इसलिये होता है कि मेरी शक्तियों सत्त्व, रज आदि गुणों और उनकी वृत्तियोंका रहस्य लोग समझ नहीं पाते; इसलिये वे अपनी अपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बैठते हैं ||५||
यासां व्यतिकरादासीद्विकल्पो वदतां पदम्।
प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति ६।
सत्त्व आदि गुणोंके क्षोभसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपंच-जो वस्तु नहीं केवल नाम है—उठ खड़ा हआ है। यही वाद-विवाद करनेवालोंके विवादका विषय है। जब इन्द्रियाँ अपने वशमें हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट जाते हैं ||६||
परस्परानुप्रवेशात्तत्त्वानां पुरुषर्षभ।
पौर्वापर्यप्रसङ्ख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् ७।
पुरुष-शिरोमणे! तत्त्वोंका एक-दूसरेमें अनुप्रवेश है, इसलिये वक्ता तत्त्वोंकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेता है ||७||
एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च।
पूर्वस्मिन्वा परस्मिन्वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ८।
ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्त्वमें बहुत-से दूसरे तत्त्वोंका अन्तर्भाव हो गया है। इसका कोई बन्धन नहीं है कि किसका किसमें अन्तर्भाव हो। कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके कारण मिट्टी-सूत
आदिमें, तो कभी मिट्री-सूत आदिका घट-पट आदि कार्यों में अन्तर्भाव हो जाता है ||८||
पौर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसङ्ख्यानमभीप्सताम्।
यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात् ९।
इसलिये वादी-प्रतिवादियोंमेंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको जिस कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके तत्त्वोंकी जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं; क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसंगत ही है ।।९।।
अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्।
स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् १०।
उद्धवजी! जिन लोगोंने छब्बीस संख्या स्वीकार की है, वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने-आपको नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान करानेके लिये किसी अन्य सर्वज्ञकी आवश्यकता है। (इसलिये प्रकृतिके कार्यकारणरूप चौबीस तत्त्व, पचीसवाँ पुरुष और छब्बीसवाँ ईश्वर–इस प्रकार कुल छब्बीस तत्त्व स्वीकार करने चाहिये) ।।१०।।
पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि।
तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ११।
पचीस तत्त्व माननेवाले कहते हैं कि इस शरीरमें जीव और ईश्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद नहीं है, इसलिये उनमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञानकी बात, सो तो सत्त्वात्मिका प्रकृतिका गुण है ||११||
प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः।
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः १२।
तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; इसलिये सत्त्व, रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हैं। इन्हींके द्वारा जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिये ज्ञान आत्माका गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ।।१२।।
सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते।
गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च १३।
इस प्रसंगमें सत्त्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न करनेवाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात् महत्तत्त्व ही स्वभाव है। (इसलिये पचीस और छब्बीस तत्त्वोंकी–दोनों ही संख्या युक्तिसंगत है) ||१३||
पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः।
ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव १४।
उद्धवजी! (यदि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अलग मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलयको देखते हुए मानना चाहिये, तो तत्त्वोंकी संख्या स्वयं ही अट्ठाईस हो जाती है। उन तीनोंके अतिरिक्त पचीस ये हैं—) पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-ये नौ तत्त्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ ।।१४।।
श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः।
वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ्घ्रिः कर्माण्यङ्गोभयं मनः १५।
शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः।
गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः १६।
श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना-ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वाक्, पाणि, पाद, पाय और उपस्थ-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ; तथा मन, जो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं। इस प्रकार कुल ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध–ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय। इस प्रकार तीन, नौ, ग्यारह और पाँच–सब मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व होते हैं। कर्मेन्द्रियों के द्वारा होनेवाले पाँच कर्म-चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना इनके द्वारा तत्त्वोंकी संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेन्द्रियस्वरूप ही मानना चाहिये ||१५-१६||
सर्गादौ प्रकृतिर्ह्यस्य कार्यकारणरूपिणी।
सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते १७।
सष्टिके आरम्भमें कार्य (ग्यारह इन्द्रिय और पंचभूत) और कारण (महत्तत्त्व आदि) के रूपमें प्रकृति ही रहती है। वही सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी अवस्थाएँ धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है ।।१७।।
व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया।
लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेर्बलात् १८।
महत्तत्त्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके ईक्षणसे शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बलसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं ।।१८।।
सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पञ्च खादयः।
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः १९।
उद्धवजी! जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सात स्वीकार करते हैं, उनके विचारसे आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-ये पाँच भूत, छठा जीव और सातवाँ परमात्मा–जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत् दोनोंका अधिष्ठान है—ये ही तत्त्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राणादिकी उत्पत्ति तो पंचभूतोंसे ही हुई है [इसलिये वे इन्हें अलग नहीं गिनते ||१९||
षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्।
तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः सृष्ट्वेदं समपाविशत् २०।
जो लोग केवल छः तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और छठा है परमपुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाये हुए पंचभूतोंसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है (इस मतके अनुसार जीवका परमात्मामें और शरीर आदिका पंचभूतोंमें समावेश हो जाता है) ||२०||
चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः।
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु २१।
जो लोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे तेज, जल और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगत्में जितने पदार्थ हैं, सब इन्हींसे उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्योंका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं ||२१||
सङ्ख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च।
पञ्च पञ्चैकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः २२।
जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं—पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन और एक आत्मा ।।२२।।
तद्वत्षोडशसङ्ख्याने आत्मैव मन उच्यते।
भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश २३।
जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सोलह बतलाते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अन्तर केवल इतना ही है कि वे आत्मामें मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्त्वसंख्या सोलह रह जाती है। जो लोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं कि आकाशादि पाँच भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक जीवात्मा और परमात्मा—ये तेरह तत्त्व हैं ।।२३।।
एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च।
अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ २४।
ग्यारह संख्या माननेवालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और इनके अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व स्वीकार किया है। जो लोग नौ तत्त्व मानते हैं, वे आकाशादि पाँच भूत और मन, बुद्धि, अहंकार-ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष—इन्हींको तत्त्व मानते हैं ।।२४।।
इति नानाप्रसङ्ख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम्।
सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्विदुषां किमशोभनम् २५।
उद्धवजी! इस प्रकार ऋषि-मुनियोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे तत्त्वोंकी गणना की है। सबका कहना उचित ही है, क्योंकि सबकी संख्या युक्तियुक्त है। जो लोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मतमें बुराई नहीं दीखती। उनके लिये तो सब कुछठीक ही है ।।२५।।
श्रीउद्धव उवाच।
प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ।
अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः।
प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथात्मनि २६।
उद्धवजीने कहा-श्यामसुन्दर! यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष-दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपसमें इतने घुल-मिल गये हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो? ||२६||
एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि।
छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः २७।
कमलनयन श्रीकष्ण! मेरे हृदयमें इनकी भिन्नता और अभिन्नताको लेकर बहत बड़ा सन्देह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणीसे मेरे सन्देहका निवारण कर दीजिये ।।२७।।
त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः।
त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः २८।
भगवन्! आपकी ही कृपासे जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे ही उनके ज्ञानका नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा सन्देह मिटाने में समर्थ हैं ।।२८।।
श्रीभगवानुवाच।
प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ।
एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः २९।
भगवान् श्रीकृष्णने कहा-उद्धवजी! प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा-इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है। इस प्राकृत जगत्में जन्म-मरण एवं वृद्धि-ह्रास आदि विकार लगे ही रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणोंके क्षोभसे ही बना है ||२९||
ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा विकल्पबुद्धीश्च गुणैर्विधत्ते।
वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदैवमधिभूतमन्यत् ३०।
प्रिय मित्र! मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्त्व, रज आदि गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदवृत्तियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टिको तीन भागोंमें बाँट सकते हैं। वे तीन भाग हैं-अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ||३०||
दृग्रूपमार्कं वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे।
आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः ३१।
उदाहरणार्थ-नेत्रेन्द्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है और नेत्र-गोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक-दूसरेके आश्रमसे सिद्ध होते हैं। और इसलिये अध्यात्म, अधिदैव और अधिभत—ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परन्तु आकाशमें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है, क्योंकि वह स्वतःसिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थों की मूलसिद्धि है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके भीतीन-तीन भेद हैं ||३१||
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुर्।
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम् ३२।
प्रकतिसे महत्तत्त्व बनता है और महत्तत्त्वसे अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणोंके क्षोभसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है। अहंकारके तीन भेद हैं -सात्त्विक, तामस और राजस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूलकारण है ।।३२।।
योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान्महतः प्रसूतः।
अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतुर्वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च ३३।
आत्मा ज्ञानस्वरूप है; उसका इन पदार्थोंसे न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई विवादकी ही बात है! अस्ति-नास्ति (है-नहीं), सगण-निर्गण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूलकारण भेददृष्टि ही है। इसमें सन्देह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सर्वथा व्यर्थ है तथापि जो लोग मुझसे-अपने वास्तविक स्वरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ।।३३।।
आत्मापरिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः।
व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात् ३४।
उद्धवजीने पूछा-भगवन! आपसे विमुख जीव अपने किये हए पुण्य-पापोंके फलस्वरूप ऊँची-नीची योनियों में जाते-आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकर्ताका कर्म करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे सम्भव है? ||३४||
श्रीउद्धव उवाच।
त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो।
उच्चावचान्यथा देहान्गृह्णन्ति विसृजन्ति च ३५।
गोविन्द! जो लोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयके ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते। और इस विषयके विद्वान् संसारमें प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी भूल-भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस्य समझाइये ||३५||
तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः।
न ह्येतत्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्चिताः ३६।
भगवान् श्रीकृष्णने कहा-प्रिय उद्धव! मनुष्योंका मन कर्म-संस्कारोंका पुंज है। उन संस्कारोंके अनुसार भोग प्राप्त करनेके लिये उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी लगी हुई हैं। इसीका नाम है लिंगशरीर। वही कर्मों के अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे लोकमें आता-जाता रहता है। आत्मा इस लिंगशरीरसे सर्वथा पृथक् है। उसका आना-जाना नहीं होता; परन्तु जब वह अपनेको लिंगशरीर ही समझ बैठता है, उसीमें अहंकार कर लेता है, तब उसे भी अपना जाना-आना प्रतीत होने लगता है ||३६||
श्रीभगवानुवाच।
मनः कर्ममयं नॄणामिन्द्रियैः पञ्चभिर्युतम्।
लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ३७।
मन कर्मोंके अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता है और क्षणभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्वचिन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है। धीरे-धीरे उसकी स्मृति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है ||३७।।
ध्यायन्मनोऽनु विषयान्दृष्टान्वानुश्रुतानथ।
उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति ३८।
उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है ।।३८।।
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्स्मरेत्पुनः।
जन्तोर्वै कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः ३९।
उदार उद्धव! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेद-भावसे ‘मैं’ के रूपमें स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीरमें अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ । कहा जाता है ||३९||
जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद।
विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः ४०।
यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूर्व देहका स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके स्वप्न और मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथमें पूर्व सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझता है ||४०।।
स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ।
तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति ४१।
इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मवस्तुमें यह उत्तम, मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती है। उनमें अभिमान करनेसे ही आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेदोंका हेतु मालूम पड़ने लगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आदिके लिये भेदका हेतु हो जाता है ।।४१।।
इन्द्रियायनसृष्ट्येदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि।
बहिरन्तर्भिदाहेतुर्जनोऽसज्जनकृद्यथा ४२।
प्यारे उद्धव! कालकी गति सूक्ष्म है। उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्म-मरण नहीं दीख पड़ते ।।४२।।
नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च।
कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते ४३।
जैसे कालके प्रभावसे दियेकी लौ, नदियोंके प्रवाह अथवा वृक्षके फलोंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही समस्त प्राणियोंके शारीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है ||४३||
यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः।
तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ४४।
जैसे यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका यह वही जल है—ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, वैसे ही विषय-चिन्तनमें व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है ।।४४।।
सोऽयं दीपोऽर्चिषां यद्वत्स्रोतसां तदिदं जलम्।
सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीर्धीर्मृषायुषाम् ४५।
यद्यपि वह भ्रान्त पुरुष भी अपने कर्मों के बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है; वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रान्तिसे वह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी है, जैसे कि काष्ठसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता है ।।४५।।
मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्।
म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः ४६।
उद्धवजी! गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु–ये नौ अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं ।।४६।।
निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्।
वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव ४७।
यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ उसके मनोरथके अनुसार ही हैं; परन्तु वह अज्ञानवश गुणोंके संगसे इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हो जानेपर इन्हें छोड भी देता है ||४७||
एता मनोरथमयीर्हान्यस्योच्चावचास्तनूः।
गुणसङ्गादुपादत्ते क्वचित्कश्चिज्जहाति च ४८।
पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने-अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये। जन्म-मृत्युसे युक्त देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे युक्त शरीर नहीं है ।।४८।।
आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ।
न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो द्वयलक्षणः ४९।
जैसे जौ-गेहूँ आदिकी फसल बोनेपर उग आती है और पक जानेपर काट दी जाती है, किन्तु जो पुरुष उनके उगने और काटनेका जाननेवाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक है; वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वथा पृथक है ।।४९।।
तरोर्बीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ।
तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक् ५०।
अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीरसे आत्माका विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्त्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं। इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युरूप संसारमें भटकना पड़ता है ।।५०।।
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्।
तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ५१।
जब अविवेकी जीव अपने कर्मोंके अनुसार जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकने लगता है, तब सात्त्विक कर्मोकी आसक्तिसे वह ऋषिलोक और देवलोकमें राजसिक कर्मोकी आसक्तिसे मनुष्य और असुरयोनियोंमें तथा तामसी कर्मोंकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योनियों में जाता है ||५१।।
सत्त्वसङ्गादृषीन्देवान्रजसासुरमानुषान्।
तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः ५२।
जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने–तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धिके गुणोंको देखता है, तब स्वयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है ||५२।।
नृत्यतो गायतः पश्यन्यथैवानुकरोति तान्।
एवं बुद्धिगुणान्पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते ५३।
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव।
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ५४।
जैसे नदी-तालाब आदिके जलके हिलने या चंचल होनेपर उसमें प्रतिबिम्बित तटके वक्ष भी उसके साथ हिलतेडोलते-से जान पड़ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाले नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती हुई-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये तथा स्वप्नमें देखे गये भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दाशार्ह! आत्माका विषयानुभवरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वभाव ही है ।।५३-५४।।
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा।
स्वप्नदृष्टाश्च दाशार्ह तथा संसार आत्मनः ५५।
विषयोंके सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका ही चिन्तन करता रहता है, उसका यह जन्म-मृत्युरूप संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता, जैसे स्वप्नमें प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं होती ।।५५।।
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते।
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ५६।
प्रिय उद्धव! इसलिये इन दुष्ट (कभी तृप्त न होनेवाली) इन्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो। आत्म-विषयक अज्ञानसे प्रतीत होनेवाला सांसारिक भेद-भाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो ||५६||
तस्मादुद्धव मा भुङ्क्ष्व विषयानसदिन्द्रियैः।
आत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम् ५७।
क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्भिः प्रलब्धोऽसूयितोऽथ वा।
ताडितः सन्निरुद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः ५८।
असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणीद्वारा अपमान करें, उपहास करें, निन्दा करें, मारें-पीटें, बाँधे, आजीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, मूत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें, निष्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें; उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुब्ध न होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका तो पता नहीं है। अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयोंसे अपनी विवेक-बद्धिद्वारा ही किसी बाहा साधनसे नहीं-अपनेको बचा लेना चाहिये। वस्तुतः आत्म-दष्टि ही समस्त विपत्तियोंसे बचनेका एकमात्र साधन है ।।५७-५८।।
निष्ठ्युतो मूत्रितो वाज्ञैर्बहुधैवं प्रकम्पितः।
श्रेयस्कामः कृच्छ्रगत आत्मनात्मानमुद्धरेत् ५९।
उद्धवजीने कहा-भगवन्! आप समस्त वक्ताओंके शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त असहा समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकँ, आपका उपदेश जीवनमें धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइये ।।५९।।
श्रीउद्धव उवाच।
यथैवमनुबुध्येयं वद नो वदतां वर ६०।
विश्वात्मन्! जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेम-पूर्वक संलग्न हैं, जिन्होंने आपके चरणकमलोंका ही आश्रय ले लिया है, उन शान्त पुरुषों के अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टोंके द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि प्रकृति अत्यन्त बलवती है ।।६०||
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः।