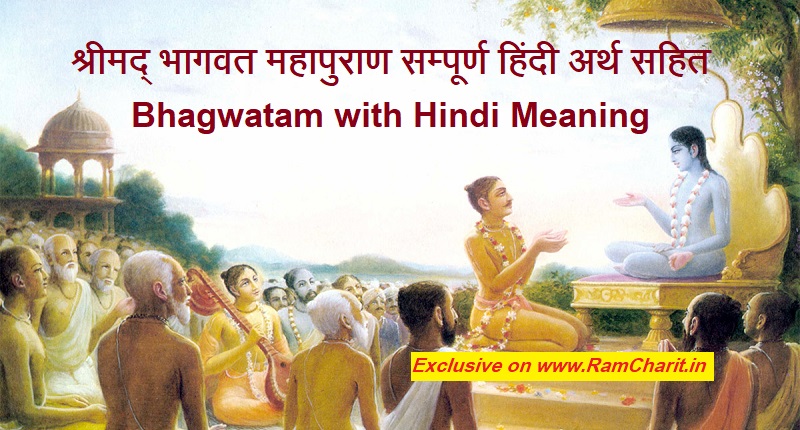श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 11 अध्याय 28
28 CHAPTER
श्रीमद्भागवतपुराणम्/स्कन्धः ११/अध्यायः २८
परमार्थनिरूपणम् –
श्रीभगवानुवाच –
( अनुष्टुप् )
परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गहयेत् ।
विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च ॥ १ ॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-उद्धवजी! यद्यपि व्यवहार में पुरुष और प्रकृति-द्रष्टा और दृश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत् जान पड़ता है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठान-स्वरूप ही है; इसलिये किसीके शान्त, घोर और मढ स्वभाव तथा उनके अनुसार कर्मोंकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा। सर्वदा अद्वैत-दष्टि रखनी चाहिये ।।१।।
परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति ।
स आशु भ्रश्यते स्वार्थाद् असत्यभिनिवेशतः ॥ २ ॥
जो पुरुष दूसरोंके स्वभाव और उनके कर्मोंकी प्रशंसा अथवा निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवेशका उसके प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दृढ़ करती हैं ।।२।।
तैजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः ।
मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वत् नानार्थदृक् पुमान् ॥ ३ ॥
उद्धवजी! सभी इन्द्रियाँ राजस अहंकारके कार्य हैं। जब वे निद्रित हो जाती हैं तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो जाता है; अर्थात् उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती। उस समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपनेके झूठे दृश्योंमें भटकने लगता है और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्युके समान गाढ़ निद्रा-सुषुप्तिमें लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने अद्वितीय आत्मस्वरूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने लगता है तब वह स्वप्नके समान झूठे दृश्योंमें फँस जाता है; अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता है ।।३।।
किं भद्रं किं अभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत् ।
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च ॥ ४ ॥
उद्धवजी! जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और इतनी बुरी है—यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये दृश्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिथ्यात्व तो स्पष्ट ही है ।।४।।
छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः ।
एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम् ॥ ५ ॥
परछाईं, प्रतिध्वनि और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परन्तु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय-कम्प आदिका संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएँ हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परन्तु जबतक ज्ञानके द्वारा इनकी असत्यताका बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं ||५||
आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः ।
त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः ॥ ६ ॥
उद्धवजी! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है। वही सर्वशक्तिमान् भी है। जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी है। अर्थात् वही विश्व बनता है और वही बनाताभी है, वही रक्षक है और रक्षित भी वही है। सर्वात्मा भगवान् ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं ||६||
तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मात् अन्यो भावो निरूपितः ।
निरूपितेऽयं त्रिविधा निर्मूल भातिरात्मनि ।
इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् ॥ ७ ॥
अवश्य ही व्यवहारदष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न है; परन्तु आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है। उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मस्वरूप ही है; इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत-ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा निर्मूल ही हैं। न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्त्व, रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्रष्टादर्शन-दृश्य आदिकी त्रिविधता मायाका खेल है ||७||
एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम् ।
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत् ॥ ८ ॥
उद्धवजी! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है वह न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा। वह जगत्में सूर्यके समान समभावसे विचरता रहता है ।।८।।
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा ।
आद्यन्तवत् असज्ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह ॥ ९ ॥
प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभूति आदि सभी प्रमाणोंसे यह सिद्ध है कि यह जगत् उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत्में असंगभावसे विचरना चाहिये ।।९।।-
श्रीउद्धव उवाच –
नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टृदृश्ययोः ।
अनात्मस्वदृशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥ १० ॥
उद्धवजीने पूछा-भगवन्! आत्मा है द्रष्टा और देह है दृश्य। आत्मा स्वयंप्रकाश है और देह है जड। ऐसी स्थितिमें जन्म-मृत्युरूप संसार न शरीरको हो सकता है और न आत्माको। परन्तु इसका होना भी उपलब्ध होता है। तब यह होता किसे है? ||१०||
आत्माव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः ।
अग्निवद्दारुवद् अचिद् देहः कस्येह संसृतिः ॥ ११ ॥
आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित, शुद्ध, स्वयंप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणोंसे रहित है; तथा शरीर विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत है। आत्मा अग्निके समान प्रकाशमान है तो शरीर काठकी तरह अचेतन। फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार है किसे? ||११।।
श्रीभगवानुवाच –
यावद् देहेन्द्रियप्राणैः आत्मनः सन्निकर्षणम् ।
संसारः फलवांस्तावद् अपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥ १२ ॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा-वस्तुतः प्रिय उद्धव! संसारका अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है ||१२||
अर्थे हि अविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ।
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥ १३ ॥
जैसे स्वप्नमें अनेकों विपत्तियाँ आती हैं पर वास्तवमें वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती ।।१३।।
यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बह्वनर्थभृत् ।
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते ॥ १४ ॥
जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पहले उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परन्तु जब उसकी नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो स्वप्नकी विपत्तियाँ रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह आदि विकार ||१४||
शोकहर्षभयक्रोध लोभमोहस्पृहादयः ।
अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्ममृत्युश्च नात्मनः ॥ १५ ॥
उद्धवजी! अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहा और जन्ममृत्युका शिकार बनता है। आत्मासे तो इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है ।।१५।।
( मिश्र – ११ अक्षरी )
देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो
जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः ।
सूत्रं महानित्युरुधेव गीतः
संसार आधावति कालतन्त्रः ॥ १६ ॥
उद्धवजी! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है तब उसका नाम ‘जीव’ हो जाता है। उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्माकी मूर्ति है—गुण और कर्मोंका बना हुआ लिंगशरीर। उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्त्व। उसके और भी बहुत-से नाम हैं। वही कालरूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्ममृत्युरूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है ।।१६।।
अमूलमेतद् बहुरूपरूपितं
मनोवचःप्राणशरीरकर्म ।
ज्ञानासिनोपासनया शितेन
च्छित्त्वा मुनिर्गां विचरत्यतृष्णः ॥ १७ ॥
वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही कार्य हैं। यह है तो निर्मल, परन्तु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें इसीकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासनाकी शानपर चढ़ाकर ज्ञानकी तलवारको अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमानका अहंकारका मूलोच्छेद करके पृथ्वीमें निर्द्वन्द्व होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकारकी आशा-तृष्णा नहीं रहती ||१७||
ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च
प्रत्यक्षमैतिह्यमथानुमानम् ।
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥ १८ ॥
आत्मा और अनात्माके स्वरूपको पृथक्-पृथक् भलीभाँति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको शुद्ध करके वेदादि शास्त्रोंका श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महापुरुषोंके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध स्वानुभूति भी प्रमाण हैं। सबका सार यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्वितीय, उपाधिशून्य परमात्मा बीचमें भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है ।।१८।।
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्
पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य ।
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं
नानापदेशैरहमस्य तद्वत् ॥ १९ ॥
उद्धवजी! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण बनते हैं; परन्तु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा। इसलिये जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है। ठीक ऐसे ही जगत्का आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ। वास्तवमें मैं ही सत्य तत्त्व हूँ ।।१९।।
विज्ञानमेतत् त्रियवस्थमङ्ग
गुणत्रयं कारणकार्यकर्तृ ।
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च
येनैव तुर्येण तदेव सत्यम् ॥ २० ॥
भाई उद्धव! मनकी तीन अवस्थाएँ होती हैं-जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति; इन अवस्थाओंके कारण तीन ही गुण हैं सत्त्व, रज और तम, और जगतके तीन भेद हैं-अध्यात्म (इन्द्रियाँ), अधिभूत (पृथिव्यादि) और अधिदैव (कर्ता)। ये सभी त्रिविधताएँ जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीयतत्त्व-इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्मतत्त्व ही सत्य है ।।२०।।
न यत्पुरस्ताद् उत यन्न पश्चान्
मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम् ।
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद् यत्
तदेव तत् स्यादिति मे मनीषा ॥ २१ ॥
जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात् भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं-केवल कल्पनामात्र, नाममात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है—यह मेरा दृढ़ निश्चय है ।।२१।।
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो
वैकारिको राजससर्ग एषः ।
ब्रह्म स्वयं ज्योतिरतो विभाति
ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् ॥ २२ ॥
यह जो विकारमयीराजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है। यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन और पञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है ।।२२।।
एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः ।
परापवादेन विशारदेन ।
छित्त्वाऽऽत्मसन्देहमुपारमेत ।
स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः ॥ २३ ॥
ब्रह्मविचारके साधन हैं-श्रवण, मनन, निदिध्यासन और स्वानुभूति। उनमें सहायक हैं—आत्मज्ञानी गुरुदेव! इनके द्वारा विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थों का निषेध कर देना चाहिये। इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविषयक सन्देहोंको छिन्नभिन्न करके अपने आनन्दस्वरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ||२३||
नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि
देवा ह्यसुर्वायुर्जलम् हुताशः ।
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्त्वम्
अहङ्कृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम् ॥ २४ ॥
निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके कारण शरीर आत्मा नहीं है। इन्द्रिय, उनके अधिष्ठात-देवता, प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका धारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता है। बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणोंकी साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि ये सब-के-सब दृश्य एवं जड हैं ।।२४।।
समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभि
र्गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः ।
विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दूषणं ।
घनैरुपेतैर्विगतै रवेः किम् ॥ २५ ॥
उद्धवजी! जिसे मेरे स्वरूपका भलीभाँति ज्ञान हो गया है, उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे लाभ क्या है? और यदि वे विक्षिप्त रहती हैं तो उनसे हानि भी क्या है? क्योंकि अन्तःकरण और बाह्यकरण—सभी गुणमय हैं और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। भला, आकाशमें बादलोंके छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या बनता-बिगड़ता है? ||२५||
यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणै
र्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते ।
तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलै
रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम् ॥ २६ ॥
जैसे वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धुल-धएँ मटमैला नहीं कर सकते और ऋतुओंके गुण गरमी-सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते क्योंकि ये सब आनेजानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश इन सबका एकरस अधिष्ठान है-वैसे ही सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी वृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे है। इनके द्वारा तो केवल वही संसारमें भटकता है जो इनमें अहंकार कर बैठता है ||२६||
तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो
गुणेषु मायारचितेषु तावत् ।
मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्
रजो निरस्येत मनःकषायः ॥ २७ ॥
उद्धवजी! ऐसा हेनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गणों और उनके कार्योंका संग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे सुदृढ़ भक्तियोगके द्वारा मनका रजोगुणरूप मल एकदम निकल न जाय ।।२७।।
यथाऽऽमयोऽसाधु चिकित्सितो नृणां
पुनः पुनः सन्तुदति प्ररोहन् ।
एवं मनोऽपक्वकषायकर्म
कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम् ॥ २८ ॥
उद्धवजी! जैसे भलीभाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समूल नाश नहीं होता, वह बारबार उभरकर मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कर्मोंके संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो स्त्री-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको बेधता रहता है और उसे कई बार योगभ्रष्ट भी कर देता है ।।२८।।
कुयोगिनो ये विहितान्तरायै
र्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ।
ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् ॥ २९ ॥
देवताओंके द्वारा प्रेरित शिष्य-पत्र आदिके द्वारा किये हुए विघ्नोंसे यदि कदाचित् अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी वह अपने पुर्वाभ्यासके कारण पुनः योगाभ्यासमें ही लग जाता है। कर्म आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती ।।२९।।
करोति कर्म क्रियते च जन्तुः
केनाप्यसौ चोदित आनिपतात् ।
न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि
निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या ॥ ३० ॥
उद्धवजी! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्ममें ही लगा रहता है और उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो तत्त्वका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित रहनेपर भी संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें इष्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं होता; क्योंकि आनन्दस्वरूप आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसारसम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं ।।३०।।
तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं
शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम् ।
स्वभावमन्यत् किमपीहमानं
आत्मानमात्मस्थमतिर्न वेद ॥ ३१ ॥
जो अपने स्वरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मस्वरूपमें स्थित ब्रह्माकार रहती है ।।३१।।
यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थं
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् ।
न मन्यते वस्तुतया मनीषी
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम् ॥ ३२ ॥
यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो कि असत् हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूतिसे सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जानेपर स्वप्नमें देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोंको कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोंको सत्य नहीं मानते ||३२||
पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्रम्
अज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग ।
निवर्तते तत्पुनरीक्षयैव
न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥ ३३ ॥
उद्धवजी! (इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि) अनेकों प्रकारके गुण और कर्मोंसे युक्त देह, इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योंकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका ग्रहण हो सकता है और न त्याग ।।३३।।
यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां
तमो निहन्यान्न तु सद् विधत्ते ।
एवं समीक्षा निपुणा सती मे
हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः ॥ ३४ ॥
जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योंके नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका परदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूपका दृढ़ अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर देता है। वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभव नहीं कराता ||३४||
एष स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो
महानुभूतिः सकलानुभूतिः ।
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे
येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥ ३५ ॥
उद्धवजी! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती। वह स्वयंप्रकाश है। उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकारके विकार नहीं हैं। वह जन्मरहित है अर्थात् कभी किसी प्रकार भी वृत्तिमें सकता। आत्मामें देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। सबकी और सब प्रकारकीअनुभुतियाँ आत्मस्वरूप ही हैं। जब मन और वाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहारदृष्टिसे उसके स्वरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें निरूपण किया जाता है ||३५||
( अनुष्टुप् )
एतावान् आत्मसम्मोहो यद् विकल्पस्तु केवले ।
आत्मन्नृते स्वमात्मानं अवलम्बो न यस्य हि ॥ ३६ ॥
उद्धवजी! अद्वितीय आत्मतत्त्वमें अर्थहीन नामोंके द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच यह बहत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस भ्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं। इसलिये सब कुछ आत्मा ही है ||३६||
यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पञ्चवर्णमबाधितम् ।
व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पण्डितमानिनाम् ॥ ३७ ॥
बहुत-से पण्डिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्चभौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिये सत्य है। परन्तु यह तो अर्थहीन वाणीका आडम्बरमात्र है; क्योंकि तत्त्वतः तो इन्द्रियोंकी पृथक् सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसीको प्रमाणित कैसे करेंगी? ||३७।।
योगिनोऽपक्वयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः ।
उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥ ३८ ॥
उद्धवजी! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीडित हो, तो उसे इन उपायोंका आश्रय लेना चाहिये ।।३८।।
योगधारणया कांश्चिद् आसनैर्धारणान्वितैः ।
तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिद् उपसर्गान् विनिर्दहेत् ॥ ३९ ॥
गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमासूर्य आदिकी धारणाके द्वारा, वात आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रहसादिकत विघ्नोंको तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नष्ट कर डालना चाहिये ||३९||
कांश्चित् ममानुध्यानेन नामसङ्कीर्तनादिभिः ।
योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्याद् अशुभदान्छनैः ॥ ४० ॥
काम-क्रोध आदि विघ्नोंको मेरे चिन्तन और नाम-संकीर्तन आदिके द्वारा नष्ट करना चाहिये।तथा पतनकी ओर ले जानेवाले दम्भ-मद आदि विघ्नोंको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर कर देना चाहिये ।।४०||
केचिद् देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम् ।
विधाय विविधोपायैः अथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥ ४१ ॥
न हि तत् कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः ।
अन्तवत्त्वात् शरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ ४२ ॥
कोई-कोई मनस्वी योगी विविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको सुदृढ़ और युवावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके लिये योगसाधन करते हैं, परन्तु बुद्धिमान् पुरुष ऐसे विचारका समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्षमें लगे हुए फलके समान इस शरीरका नाश तो अवश्यम्भावी है ||४१-४२||
योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् ।
तत् श्रद्दध्यान्न मतिमान् योगमुत्सृज्य मत्परः ॥ ४३ ॥
यदि कदाचित् बहुत दिनोंतक निरन्तर और आदरपूर्वक योगसाधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ़ भी हो जाय, तब भी बुद्धिमान् पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्तिके लिये ही संलग्न रहना चाहिये ।।४३।।
योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः ।
नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः ॥ ४४ ॥
जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हई योगसाधनामें संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न-बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभूतिमें मग्न हो जाता है ।।४४।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां
संहितायां एकादशस्कन्धे अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥