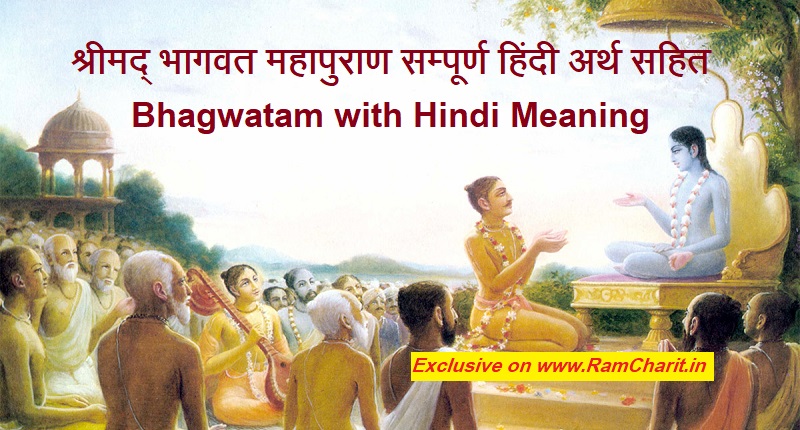श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 3 अध्याय 7
7rd chapter
श्रीमद्भागवतपुराणम्
अध्यायः ७
श्रीशुक उवाच –
(अनुष्टुप्)
एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायनसुतो बुधः ।
प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥ १ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-मैत्रेयजीका यह भाषण सुनकर बुद्धिमान् व्यासनन्दन विदुरजीने उन्हें अपनी वाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा ।।१।।
विदुर उवाच ।
ब्रह्मन् कथं भगवतः चिन्मात्रस्याविकारिणः ।
लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः ॥ २ ॥
विदुरजीने पूछा-ब्रह्मन्! भगवान् तो शुद्ध बोधस्वरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं; उनके साथ लीलासे भी गुण और क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ।।२।।
क्रीडायां उद्यमोऽर्भस्य कामश्चिक्रीडिषान्यतः ।
स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः ॥ ३ ॥
बालकमें तो कामना और दूसरों के साथ खेलनेकी इच्छा रहती है, इसीसे वह खेलनेके लिये प्रयत्न करता है; किन्तु भगवान् तो स्वतः नित्यतृप्त-पूर्णकाम और सर्वदा असंग हैं, वे क्रीडाके लिये भी क्यों संकल्प करेंगे ।।३।।
अस्राक्षीत् भगवान् विश्वं गुणमय्याऽऽत्ममायया ।
तया संस्थापयत्येतद् भूयः प्रत्यपिधास्यति ॥ ४ ॥
भगवान्ने अपनी गुणमयी मायासे जगत्की रचना की है, उसीसे वे इसका पालन करते हैं और फिर उसीसे संहार भी करेंगे ।।४।।
देशतः कालतो योऽसौ अवस्थातः स्वतोऽन्यतः ।
अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येताजया कथम् ॥ ५ ॥
जिनके ज्ञानका देश, काल अथवा अवस्थासे, अपने-आप या किसी दूसरे निमित्तसे भी कभी लोप नहीं होता, उनका मायाके साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है ।।५।।
भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्ववस्थितः ।
अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः ॥ ६ ॥
एकमात्र ये भगवान् ही समस्त क्षेत्रोंमें उनके साक्षीरूपसे स्थित हैं, फिर इन्हें दर्भाग्य या किसी प्रकारके कर्मजनित क्लेशकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ।।६।।
एतस्मिन्मे मनो विद्वन् खिद्यतेऽज्ञानसङ्कटे ।
तन्नः पराणुद विभो कश्मलं मानसं महत् ॥ ७ ॥
भगवन्! इस अज्ञानसंकटमें पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है, आप मेरे मनके इस महान् मोहको कृपा करके दूर कीजिये ||७||
श्रीशुक उवाच –
स इत्थं चोदितः क्षत्त्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः ।
प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः ॥ ८ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-तत्त्वजिज्ञासु विदुरजीकी यह प्रेरणा प्राप्तकर अहंकारहीन श्रीमैत्रेयजीने भगवान्का स्मरण करते हुए मुसकराते हुए कहा ।।८।।
मैत्रेय उवाच –
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ।
ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम् ॥ ९ ॥
श्रीमैत्रेयजीने कहा-जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्तस्वरूप है, वही दीनता और बन्धनको प्राप्त हो—यह बात युक्तिविरुद्ध अवश्य है; किन्तु वस्तुतः यही तो भगवान्की माया है ||९||
यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः ।
प्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरश्छेदनादिकः ॥ १० ॥
जिस प्रकार स्वप्न देखनेवाले पुरुषको अपना सिर कटना आदि व्यापार न होनेपर भी अज्ञानके कारण सत्यवत् भासते हैं, उसी प्रकार इस जीवको बन्धनादि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं ।।१०।।।
यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः ।
दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुः आत्मनोऽनात्मनो गुणः ॥ ११ ॥
यदि यह कहा जाय कि फिर ईश्वरमें इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जलमें होनेवाली कम्प आदि क्रिया जलमें दीखनेवाले चन्द्रमाके प्रतिबिम्बमें न होनेपर भी भासती है, आकाशस्थ चन्द्रमामें नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्या धर्मोकी प्रतीति होती है, परमात्मामें नहीं ||११||
स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया ।
भगवद्भक्तियोगेन तिरोधत्ते शनैरिह ॥ १२ ॥
निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह प्रतीति धीरे-धीरे निवृत्त हो जाती है ||१२||
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ ।
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्नशः ॥ १३ ॥
जिस समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-द्वेषादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ।।१३।।
अशेषसङ्क्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः ।
किं वा पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवारतिरात्मलब्धा ॥ १४ ॥
श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन एवं श्रवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके चरणकमलकी रजके सेवनका प्रेम जग पड़े, तब तो कहना ही क्या है? ||१४।।।
विदुर उवाच –
(अनुष्टुप्)
सञ्छिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासिना विभो ।
उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति ॥ १५ ॥
विदुरजीने कहा-भगवन्! आपके युक्तियुक्त वचनोंकी तलवारसे मेरे सन्देह छिन्न-भिन्न हो गये हैं। अब मेरा चित्त भगवानकी स्वतन्त्रता और जीवकी परतन्त्रता दोनों ही विषयोंमें खूब प्रवेश कर रहा है ।।१५।।
साध्वेतद् व्याहृतं विद्वन् आत्ममायायनं हरेः ।
आभात्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः ॥ १६ ॥
विद्वन्! आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीवको जो क्लेशादिकी प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान्की माया ही है। वह क्लेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है; क्योंकि इस विश्वका मूल कारण ही मायाके अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।।१६।।
यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः ।
तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥ १७ ॥
इस संसारमें दो ही प्रकारके लोग सुखी हैं—या तो जो अत्यन्त मूढ़ (अज्ञानग्रस्त) हैं या जो बुद्धि आदिसे अतीत श्रीभगवानको प्राप्त कर चुके हैं। बीचकी श्रेणीके संशयापन्न लोग तो दुःख ही भोगते रहते हैं ।।१७।।
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः ।
तां चापि युष्मच्चरण सेवयाहं पराणुदे ॥ १८ ॥
भगवन्! आपकी कृपासे मुझे यह निश्चय हो गया किये अनात्म पदार्थ वस्तुतः हैं नहीं, केवल प्रतीत ही होते हैं। अब मैं आपके चरणोंकी सेवाके प्रभावसे उस प्रतीतिको भी हटा दूँगा ।।१८।।
यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः ।
रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनार्दनः ॥ १९ ॥
इन श्रीचरणोंकी सेवासे नित्यसिद्ध भगवान् श्रीमधुसूदनके चरणकमलोंमें उत्कट प्रेम और आनन्दकी वृद्धि होती है, जो आवागमनकी यन्त्रणाका नाश कर देती है ।।१९।।
दुरापा ह्यल्पतपसः सेवा वैकुण्ठवर्त्मसु ।
यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः ॥ २० ॥
महात्मालोग भगवत्प्राप्तिके साक्षात् मार्ग ही होते हैं, उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्रीहरिके गुणोंका गान होता रहता है; अल्पपुण्य पुरुषको उनकी सेवाका अवसर मिलना अत्यन्त कठिन है ।।२०।।
सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराणि अनुक्रमात् ।
तेभ्यो विराजं उद्धृत्य तमनु प्राविशद्विभुः ॥ २१ ॥
भगवन्! आपने कहा कि सृष्टिके प्रारम्भमें भगवान्ने क्रमशः महदादि तत्त्व और उनके विकारोंको रचकर फिर उनके अंशोंसे विराट्को उत्पन्न किया और इसके पश्चात् वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गये ।।२१।।
यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्र्यूरुबाहुकम् ।
यत्र विश्व इमे लोकाः सविकाशं समासते ॥ २२ ॥
उन विराट्के हजारों पैर, जाँचे और बाँहें हैं; उन्हींको वेद आदिपुरुष कहते हैं; उन्हींमें ये सब लोक विस्तृतरूपसे स्थित हैं ||२२||
यस्मिन् दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थेन्द्रियः त्रिवृत् ।
त्वयेरितो यतो वर्णाः तद्विभूतीर्वदस्व नः ॥ २३ ॥
यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः ।
प्रजा विचित्राकृतय आसन्याभिरिदं ततम् ॥ २४ ॥
उन्हींमें इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियाभिमानी देवताओंके सहित दस प्रकारके प्राणोंका-जो इन्द्रियबल, मनोबल और शारीरिक बलरूपसे तीन प्रकारके हैं-आपने वर्णन किया है और उन्हींसे ब्राह्मणादि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे उनकी ब्रह्मादि विभूतियोंका वर्णन सुनाइये-जिनसे पुत्र, पौत्र, नाती और कुटुम्बियोंके सहित तरह-तरहकी प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्माण्ड भर गया ||२३-२४||
प्रजापतीनां स पतिः चकॢपे कान् प्रजापतीन् ।
सर्गांश्चैवानुसर्गांश्च मनून् मन्वन्तराधिपान् ॥ २५ ॥
वह विराट् ब्रह्मादि प्रजापतियोंका भी प्रभु है। उसने किन-किन प्रजापतियोंको उत्पन्न किया तथा सर्ग, अनुसर्ग और मन्वन्तरोंके अधिपति मनुओंकी भी किस क्रमसे रचना की? ||२५||
एतेषामपि वंशांश्च वंशानुचरितानि च ।
उपर्यधश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते ॥ २६ ॥
तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय ।
तिर्यङ्मानुषदेवानां सरीसृप पतत्त्रिणाम् ।
वद नः सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्विजोद्भिदाम् ॥ २७॥
मैत्रेयजी! उन मनुओंके वंश और वंशधर राजाओंके चरित्रोंका, पृथ्वीके ऊपर और नीचेके लोकों तथा भूर्लोकके विस्तार और स्थितिका भी वर्णन कीजिये तथा यह भी बताइये कि तिर्यक्, मनुष्य, देवता, सरीसृप (सर्पादि रेंगनेवाले जन्तु) और पक्षी तथा जरायुज, स्वेदज, अण्डज और उद्भिज्ज–ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए ||२६-२७।।
गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयम् ।
सृजतः श्रीनिवासस्य व्याचक्ष्वोदारविक्रमम् ॥ २८ ॥
श्रीहरिने सृष्टि करते समय जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके लिये अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु और महादेवरूपसे जो कल्याणकारी लीलाएँ कीं, उनका भी वर्णन कीजिये ||२८||
वर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः ।
ऋषीणां जन्मकर्माणि वेदस्य च विकर्षणम् ॥ २९ ॥
यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो ।
नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तंत्रं वा भगवत्स्मृतम् ॥ ३० ॥
पाषण्डपथवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनम् ।
जीवस्य गतयो याश्च यावतीर्गुणकर्मजाः ॥ ३१ ॥
वेष, आचरण और स्वभावके अनुसार वर्णाश्रमका विभाग, ऋषियोंके जन्म-कर्मादि, वेदोंका विभाग, यज्ञोंका विस्तार, योगका मार्ग, ज्ञानमार्ग और उसका साधन सांख्यमार्ग तथा भगवान्के कहे हुए नारदपांचरात्र आदि तन्त्रशास्त्र, विभिन्न पाखण्डमार्गोंके प्रचारसे होनेवाली विषमता, नीचवर्णके पुरुषसे उच्चवर्णकी स्त्रीमें होनेवाली सन्तानोंके प्रकार तथा भिन्न-भिन्न गुण और कर्मोंके कारण जीवकी जैसी और जितनी गतियाँ होती हैं, वे सब हमें सुनाइये ।।२९-३१।।
धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः ।
वार्ताया दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् ॥ ३२ ॥
श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ।
ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् ॥ ३३ ॥
ब्रह्मन्! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिके परस्पर अविरोधी साधनोंका, वाणिज्य, दण्डनीति और शास्त्रश्रवणकी विधियोंका, श्राद्धकी विधिका, पितृगणोंकी सृष्टिका तथा कालचक्रमें ग्रह, नक्षत्र और तारागणकी स्थितिका भी अलग-अलग वर्णन कीजिये ||३२-३३।।
दानस्य तपसो वापि यच्चेष्टापूर्तयोः फलम् ।
प्रवासस्थस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदि ॥ ३४ ॥
दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मोंका क्या फल है? प्रवास और आपत्तिके समय मनुष्यका क्या धर्म होता है? ||३४||
येन वा भगवान् तुस्तुष्येद् धर्मयोनिर्जनार्दनः ।
सम्प्रसीदति वा येषां एतत् आख्याहि मेऽनघ ॥ ३५ ॥
निष्पाप मैत्रेयजी! धर्मके मूल कारण श्रीजनार्दनभगवान् किस आचरणसे सन्तुष्ट होते हैं और किनपर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिये ।।३५।।
अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम ।
अनापृष्टमपि ब्रूयुः गुरवो दीनवत्सलाः ॥ ३६ ॥
द्विजवर! दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रोंको बिना पूछे भी उनके हितकी बात बतला दिया करते हैं ।।३६।।
तत्त्वानां भगवन् तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः ।
तत्रेमं क उपासीरन् क उ स्विदनुशेरते ॥ ३७ ॥
भगवन्! उन महदादि तत्त्वोंका प्रलय कितने प्रकारका है? तथा जब भगवान योगनिद्रामें शयन करते हैं, तब उनमेंसे कौन-कौन तत्त्व उनकी सेवा करते हैं और कौन उनमें लीन हो जाते हैं? ||३७||
पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ।
ज्ञानं च नैगमं यत्तद् गुरुशिष्यप्रयोजनम् ॥ ३८ ॥
जीवका तत्त्व, परमेश्वरका स्वरूप, उपनिषत-प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्यका पारस्परिक प्रयोजन क्या है? ||३८||
निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघसूरिभिः ।
स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा ॥ ३९ ॥
पवित्रात्मन् विद्वानोंने उस ज्ञानकी प्राप्तिके क्या-क्या उपाय बतलाये हैं? क्योंकि मनुष्योंको ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्यकी प्राप्ति अपने-आप तो हो नहीं सकती ||३९||
एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्मविवित्सया ।
ब्रूहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वात् अजया नष्टचक्षुषः ॥ ४० ॥
ब्रह्मन! माया-मोहके कारण मेरी विचारदष्टि नष्ट हो गयी है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुहृद् हैं; अतः श्रीहरिलीलाका ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे मैंने जो प्रश्न किये हैं, उनका उत्तर मुझे दीजिये ।।४०।।
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ ।
जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि ॥ ४१ ॥
पुण्यमय मैत्रेयजी! भगवत्तत्त्वके उपदेशद्वारा जीवको जन्म-मृत्युसे छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदोंके अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दानादिसे होनेवाला पुण्य उस पुण्यके सोलहवें अंशके बराबर भी नहीं हो सकता ।।४१।।
श्रीशुक उवाच –
स इत्थं आपृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः ।
प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥ ४२ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन्! जब कुरु-श्रेष्ठ विदुरजीने मुनिवर मैत्रेयजीसे इस प्रकार पुराणविषयक प्रश्न किये, तब भगवच्च के लिये प्रेरित किये जानेके कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुसकराकर उनसे कहने लगे ।।४२।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥