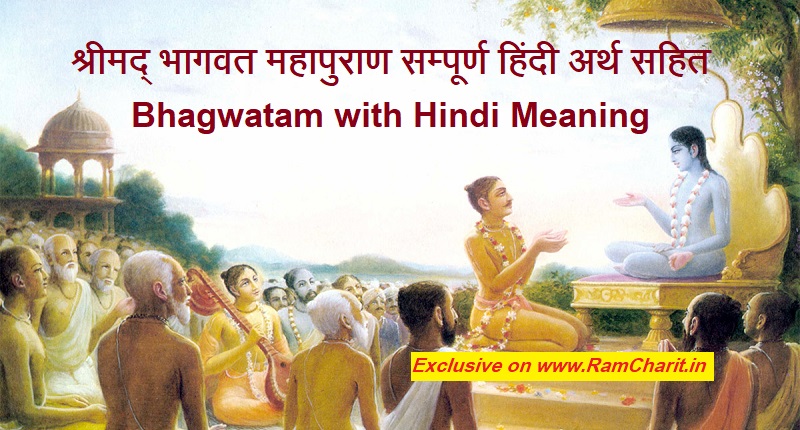श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 4 अध्याय 19
श्रीमद्भागवतपुराणम्
चतुर्थ स्कन्ध अध्यायः १९
मैत्रेय उवाच –
(अनुष्टुप्)
अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः ।
ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती ॥ १ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! महाराज मनुके ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें, जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथुने सौ अश्वमेध-यज्ञोंकी दीक्षा ली ।।१।।
तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः ।
शतक्रतुर्न ममृषे पृथोर्यज्ञमहोत्सवम् ॥ २ ॥
यह देखकर भगवान इन्द्रको विचार हआ कि इस प्रकार तो पथके कर्म मेरे कर्मोंकी अपेक्षा भी बढ़ जायँगे। इसलिये वे उनके यज्ञमहोत्सवको सहन न कर सके ।।२।।
यत्र यज्ञपतिः साक्षाद् भगवान् हरिरीश्वरः ।
अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरुः प्रभुः ॥ ३ ॥
महाराज पृथुके यज्ञमें सबके अन्तरात्मा सर्वलोकपूज्य जगदीश्वर भगवान् हरिने यज्ञेश्वररूपसे साक्षात् दर्शन दिया था ।।३।।
अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः ।
उपगीयमानो गन्धर्वैः मुनिभिश्चाप्सरोगणैः ॥ ४ ॥
उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने-अपने अनुचरोंके सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गन्धर्व, मुनि और अप्सराएँ प्रभुकी कीर्ति गा रहे थे ||४||
सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः ।
सुनन्दनन्दप्रमुखाः पार्षदप्रवरा हरेः ॥ ५ ॥
कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः ।
तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः ॥ ६ ॥
सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनन्द-नन्दादि भगवान्के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान्की सेवाके लिये उत्सुक रहते हैं वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आये थे ||५-६||
यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुघा सती ।
दोग्धि स्माभीप्सितान् अर्थान् यजमानस्य भारत ॥ ७ ॥
भारत! उस यज्ञमें यज्ञसामग्रियोंको देनेवाली भूमिने कामधेनुरूप होकर यजमानकी सारी कामनाओंको पूर्ण किया था ।।७।।
ऊहुः सर्वरसान्नद्यः क्षीरदध्यन्नगोरसान् ।
तरवो भूरिवर्ष्माणः प्रासूयन्त मधुच्युतः ॥ ८ ॥
नदियाँ दाख और ईख आदि सब प्रकारके रसोंको बहा लाती थीं तथा जिनसे मधु चूता रहता था—ऐसे बड़े-बड़े वक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह-तरहकी सामग्रियाँ समर्पण करते थे ||८||
सिन्धवो रत्ननिकरान् गिरयोऽन्नं चतुर्विधम् ।
उपायनं उपाजह्रुः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥ ९ ॥
समुद्र बहुत-सी रत्नराशियाँ, पर्वत भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य–चार प्रकारके अन्न तथा लोकपालोंके सहित सम्पूर्ण लोक तरह-तरहके उपहार उन्हें समर्पण करते थे ।।९।।
इति चाधोक्षजेशस्य पृथोस्तु परमोदयम् ।
असूयन् भगवान् इन्द्रः प्रतिघातमचीकरत् ॥ १० ॥
महाराज पृथु तो एकमात्र श्रीहरिको ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपासे उस यज्ञानुष्ठानमें उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ। किन्तु यह बात देवराज इन्द्रको सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालनेकी भी चेष्टा की ||१०||
चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम् ।
वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् अपोवाह तिरोहितः ॥ ११ ॥
जिस समय महाराज पृथु अन्तिम यज्ञद्वारा भगवान् यज्ञपतिकी आराधना कर रहे थे, इन्द्रने ईर्ष्यावश गुप्तरूपसे उनके यज्ञका घोड़ा हर लिया ।।११।।
तं अत्रिर्भगवानैक्षत् त्वरमाणं विहायसा ।
आमुक्तमिव पाखण्डं योऽधर्मे धर्मविभ्रमः ॥ १२ ॥
अत्रिणा चोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः ।
अन्वधावत सङ्क्रुद्धः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत् ॥ १३ ॥
इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये कवचरूपसे पाखण्डवेष धारण कर लिया था, जो अधर्ममें धर्मका भ्रम उत्पन्न करनेवाला है जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा-सा जान पड़ता है। इस वेषमें वे घोड़ेको लिये बड़ी शीघ्रतासे आकाशमार्गसे जा रहे थे कि उनपर भगवान् अत्रिकी दृष्टि पड़ गयी। उनके कहनेसे महाराज पृथुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोधसे बोला, ‘अरे खड़ा रह! खड़ा रह’ ।।१२-१३।।
तं तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मं शरीरिणम् ।
जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति ॥ १४ ॥
इन्द्र सिरपर जटाजूट और शरीरमें भस्म धारण किये हुए थे। उनका ऐसा वेष देखकर पृथुकुमारने उन्हें मूर्तिमान् धर्म समझा, इसलिये उनपर बाण नहीं छोड़ा ।।१४।।
वधान्निवृत्तं तं भूयो हन्तवेऽत्रिरचोदयत् ।
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधमम् ॥ १५ ॥
जब वह इन्द्रपर वार किये बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रिने पुनः उसे इन्द्रको मारनेके लिये आज्ञा दी—’वत्स! इस देवताधम इन्द्रने तुम्हारे यज्ञमें विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो’ ||१५||
एवं वैन्यसुतः प्रोक्तः त्वरमाणं विहायसा ।
अन्वद्रवद् अभिक्रुद्धो रावणं गृध्रराडिव ॥ १६ ॥
अत्रि मुनिके इस प्रकार उत्साहित करनेपर पृथुकुमार क्रोधमें भर गया। इन्द्र बड़ी तेजीसे आकाशमें जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा, जैसे रावणके पीछे जटायु ||१६||
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तर्हितः स्वराट् ।
वीरः स्वपशुमादाय पितुर्यज्ञं उपेयिवान् ॥ १७ ॥
स्वर्गपति इन्द्र उसे पीछे आते देख, उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये और वह वीर अपना यज्ञपशु लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट आया ||१७||
तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः ।
नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो ॥ १८ ॥
शक्तिशाली विदुरजी! उसके इस अद्भुत पराक्रमको देखकर महर्षियोंने उसका नाम विजिताश्व रखा ।।१८।।
उपसृज्य तमस्तीव्रं जहाराश्वं पुनर्हरिः ।
चषालयूपतश्छन्नो हिरण्यरशनं विभुः ॥ १९ ॥
यज्ञपशुको चषाल और यूपमें बाँध दिया गया था। शक्तिशाली इन्द्रने घोर अन्धकार फैला दिया और उसीमें छिपकर वे फिर उस घोडेको उसकी सोनेकी जंजीर समेत ले गये ||१९||
अत्रिः सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहायसा ।
कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नैनमबाधत ॥ २० ॥
अत्रि मनिने फिर उन्हें आकाशमें तेजीसे जाते दिखा दिया, किन्तु उनके पास कपाल और खट्वांग देखकर पृथुपुत्रने उनके मार्गमें कोई बाधा न डाली ||२०||
अत्रिणा चोदितस्तस्मै सन्दधे विशिखं रुषा ।
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितः स्वराट् ॥ २१ ॥
तब अत्रिने राजकुमारको फिर उकसाया और उसने गुस्सेमें भरकर इन्द्रको लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेष और घोड़ेको छोड़कर वहीं अन्तर्धान हो गये ||२१||
वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत् ।
तदवद्यं हरे रूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलाः ॥ २२ ॥
वीर विजिताश्व अपना घोडा लेकर पिताकी यज्ञशालामें लौट आया। तबसे इन्द्रके उस निन्दित वेषको मन्दबुद्धि पुरुषोंने ग्रहण कर लिया ।।२२।।
यानि रूपाणि जगृहे इन्द्रो हयजिहीर्षया ।
तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते ॥ २३ ॥
इन्द्रने अश्वहरणकी इच्छासे जो-जो रूप धारण किये थे, वे पापके खण्ड होनेके कारण पाखण्ड कहलाये। यहाँ ‘खण्ड’ शब्द चिह्नका वाचक है ।।२३।।
एवमिन्द्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिघांसया ।
तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणाम् ॥ २४ ॥
धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु ।
प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥ २५ ॥
इस प्रकार पृथुके यज्ञका विध्वंस करनेके लिये यज्ञपशुको चुराते समय इन्द्रने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन ‘नग्न’, ‘रक्ताम्बर’ तथा ‘कापालिक’ आदि पाखण्डपूर्ण आचारोंमें मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः मोहित हो जाती है; क्योंकि ये नास्तिकमत देखनेमें सुन्दर हैं और बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे अपने पक्षका समर्थन करते हैं। वास्तवमें ये उपधर्ममात्र हैं। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं ।।२४-२५||
तदभिज्ञाय भगवान् पृथुः पृथुपराक्रमः ।
इन्द्राय कुपितो बाणं आदत्तोद्यतकार्मुकः ॥ २६ ॥
इन्द्रकी इस कुचालका पता लगनेपर परम पराक्रमी महाराज पृथुको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया ||२६||
तमृत्विजः शक्रवधाभिसन्धितं
विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यमसह्यरंहसम् ।
निवारयामासुरहो महामते
न युज्यतेऽत्रान्यवधः प्रचोदितात् ॥ २७ ॥
उस समय क्रोधावेशके कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजोंने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इन्द्रका वध करनेको तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, ‘राजन्! आप तो बड़े बुद्धिमान् हैं, यज्ञदीक्षा ले लेनेपर शास्त्रविहित यज्ञपशुको छोड़कर और किसीका वध करना उचित नहीं है ।।२७।।
वयं मरुत्वन्तमिहार्थनाशनं
ह्वयामहे त्वच्छ्रवसा हतत्विषम् ।
अयातयामोपहवैरनन्तरं
प्रसह्य राजन् जुहवाम तेऽहितम् ॥ २८ ॥
इस यज्ञकार्यमें विघ्न डालनेवाला आपका शत्रु इन्द्र तो आपके सुयशसे ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन-मन्त्रोंद्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्निमें हवन किये देते हैं’ ।।२८।।
(अनुष्टुप्)
इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यर्त्विजो रुषा ।
स्रुग्घस्तान् जुह्वतोऽभ्येत्य स्वयम्भूः प्रत्यषेधत ॥ २९ ॥
विदुरजी! यजमानसे इस प्रकार सलाह करके उसके याजकोंने क्रोधपूर्वक इन्द्रका आवाहन किया। वे स्रुवाद्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्माजीने वहाँ आकर उन्हें रोक दिया ।।२९।।
न वध्यो भवतां इन्द्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः ।
यं जिघांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुराः ॥ ३० ॥
वे बोले, ‘याजको! तुम्हें इन्द्रका वध नहीं करना चाहिये, यह यज्ञसंज्ञक इन्द्र तो भगवानकी ही मूर्ति है। तुम यज्ञद्वारा जिन देवताओंकी आराधना कर रहे हो, वे इन्द्रके ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञद्वारा मारना चाहते हो ||३०||
तदिदं पश्यत महद् धर्मव्यतिकरं द्विजाः ।
इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद्विजिघांसता ॥ ३१ ॥
पृथुके इस यज्ञानुष्ठानमें विघ्न डालनेके लिये इन्द्रने जो पाखण्ड फैलाया है, वह धर्मका उच्छेदन करनेवाला है। इस बातपर तुम ध्यान दो, अब उससे अधिक विरोध मत करो; नहीं तो वह और भी पाखण्ड मार्गोंका प्रचार करेगा ।।३१।।
पृथुकीर्तेः पृथोर्भूयात् तर्ह्येकोनशतक्रतुः ।
अलं ते क्रतुभिः स्विष्टैः यद्भवान् मोक्षधर्मवित् ॥ ३२ ॥
अच्छा, परमयशस्वी महाराज पृथुके निन्यानबे ही यज्ञ रहने दो।’ फिर राजर्षि पृथुसे कहा, ‘राजन्! आप तो मोक्षधर्मके जाननेवाले हैं; अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानोंकी आवश्यकता नहीं है ||३२||
नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि ।
उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहौ ॥ ३३ ॥
आपका मंगल हो! आप और इन्द्र–दोनोंकीपवित्रकीर्ति भगवान् श्रीहरिके शरीर हैं; इसलिये अपने ही स्वरूपभूत इन्द्रके प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिये ।।३३।।
मास्मिन्महाराज कृथाः स्म चिन्तां
निशामयास्मद्वच आदृतात्मा ।
यद्ध्यायतो दैवहतं नु कर्तुं
मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धम् ॥ ३४ ॥
आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हआ—इसके लिये आप चिन्ता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिये। देखिये, जो मनुष्य विधाताके बिगाड़े हुए कामको बनानेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त क्रोधमें भरकर भयंकर मोहमें फँस जाता है ||३४||
(अनुष्टुप्)
क्रतुर्विरमतामेष देवेषु दुरवग्रहः ।
धर्मव्यतिकरो यत्र पाखण्डैः इन्द्रनिर्मितैः ॥ ३५ ॥
बस, इस यज्ञको बंद कीजिये। इसीके कारण इन्द्रके चलाये हुए पाखण्डोंसे धर्मका नाश हो रहा है; क्योंकि देवताओंमें बड़ा दुराग्रह होता है ||३५||
एभिरिन्द्रोपसंसृष्टैः पाखण्डैर्हारिभिर्जनम् ।
ह्रियमाणं विचक्ष्वैनं यस्ते यज्ञध्रुगश्वमुट् ॥ ३६ ॥
जरा देखिये तो, जो इन्द्र घोडेको चुराकर आपके यज्ञमें विघ्न डाल रहा था, उसीके रचे हुए इन मनोहर पाखण्डोंकी ओर सारी जनता खिंचती चली जा रही है ।।३६।।
भवान्परित्रातुमिहावतीर्णो
धर्मं जनानां समयानुरूपम् ।
वेनापचारादवलुप्तमद्य
तद्देहतो विष्णुकलासि वैन्य ॥ ३७ ॥
आप साक्षात् विष्णुके अंश हैं। वेनके दुराचारसे धर्म लुप्त हो रहा था, उस समयोचित धर्मकी रक्षाके लिये ही आपने उसके शरीरसे अवतार लिया है ।।३७।।
स त्वं विमृश्यास्य भवं प्रजापते
सङ्कल्पनं विश्वसृजां पिपीपृहि ।
ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं
प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि ॥ ३८ ॥
अतः प्रजापालक पथजी! अपने इस अवतारका उद्देश्य विचारकर आप भग आदि विश्वरचयिता मनीश्वरोंका संकल्प पूर्ण कीजिये। यह प्रचण्ड पाखण्ड-पथरूप इन्द्रकी माया अधर्मकी जननी है। आप इसे नष्ट कर डालिये’ ||३८।।
मैत्रेय उवाच –
इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः ।
तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघोनापि च सन्दधे ॥ ३९ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-लोकगुरु भगवान् ब्रह्माजीके इस प्रकार समझानेपर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथुने यज्ञका आग्रह छोड़ दिया और इन्द्रके साथ प्रीतिपूर्वक सन्धि भी कर ली ।।३९।।
कृतावभृथस्नानाय पृथवे भूरिकर्मणे ।
वरान्ददुस्ते वरदा ये तद्बर्हिषि तर्पिताः ॥ ४० ॥
इसके पश्चात् जब वे यज्ञान्त स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञोंसे तृप्त हुए देवताओंने उन्हें अभीष्ट वर दिये ।।४०||
विप्राः सत्याशिषस्तुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणाः ।
आशिषो युयुजुः क्षत्तः आदिराजाय सत्कृताः ॥ ४१ ॥
आदिराज पृथुने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणोंको दक्षिणाएँ दी तथा ब्राह्मणोंने उनके सत्कारसे सन्तुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिये ||४१।।
त्वयाऽऽहूता महाबाहो सर्व एव समागताः ।
पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षिमानवाः ॥ ४२ ॥
वे कहने लगे, ‘महाबाहो! आपके बुलानेसे जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्यादि आये थे, उन सभीका आपने दान-मानसे खूब सत्कार किया’ ।।४२।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
चतुर्थस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥