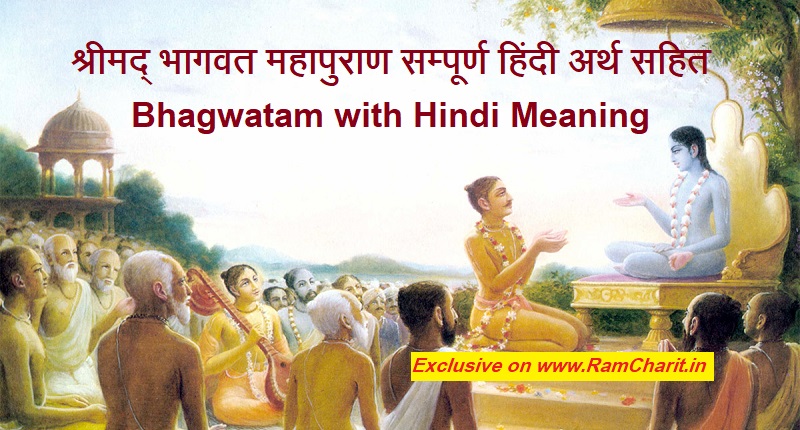श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 4 अध्याय 22
श्रीमद्भागवतपुराणम्
चतुर्थ स्कन्ध अध्यायः २२
मैत्रेय उवाच –
(अनुष्टुप्)
जनेषु प्रगृणत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमम् ।
तत्रोपजग्मुर्मुनयः चत्वारः सूर्यवर्चसः ॥ १ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं जिस समय प्रजाजन परमपराक्रमी पृथ्वीपाल पृथुकी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्यके समान तेजस्वी चार मुनीश्वर आये ||१||
तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोऽवतरतोऽर्चिषा ।
लोकानपापान् कुर्वत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान् ॥ २ ॥
राजा और उनके अनुचरोंने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कान्तिसे सम्पूर्ण लोकोंको पापनिर्मुक्त करते हुए आकाशसे उतरकर आ रहे हैं ||२||
तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः ।
ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेशो गुणानिव ॥ ३ ॥
राजाके प्राण सनकादिकोंका दर्शन करते ही, जैसे विषयी जीव विषयोंकी ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पडे—मानो उन्हें रोकनेके लिये ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियोंके साथ एकाएक उठकर खड़े हो गये ||३||
गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः ।
विधिवत्पूजयां चक्रे गृहीताध्यर्हणासनान् ॥ ४ ॥
जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकारकर आसनपर विराज गये, तब शिष्टाग्रणी पथने उनके गौरवसे प्रभावित हो विनयवश गरदन झकाये हए उनकी विधिवत पूजा की ।।४।।
तत्पादशौचसलिलैः आर्जितालकबन्धनः ।
तत्र शीलवतां वृत्तं आचरन् मानयन्निव ॥ ५ ॥
फिर उनके चरणोदकको अपने सिरके बालोंपर छिड़का। इस प्रकार शिष्टजनोचित आचारका आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषोंको ऐसा व्यवहार करना चाहिये ||५||
हाटकासन आसीनान् स्वधिष्ण्येष्विव पावकान् ।
श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान् ॥ ॥ ६ ॥
सनकादि मुनीश्वर भगवान् शंकरके भी अग्रज हैं। सोनेके सिंहासनपर वे ऐसे सुशोभित हुए, जैसे अपने-अपने स्थानोंपर अग्नि देवता। महाराज पृथुने बड़ी श्रद्धा और संयमके साथ प्रेमपूर्वक उनसे कहा ।।६।।
पृथुरुवाच –
अहो आचरितं किं मे मङ्गलं मङ्गलायनाः ।
यस्य वो दर्शनं ह्यासीद् दुर्दर्शानां च योगिभिः ॥ ७ ॥
पृथुजीने कहा-मंगलमूर्ति मुनीश्वरो! आपके दर्शन तो योगियोंको भी दुर्लभ हैं; मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ ||७||
किं तस्य दुर्लभतरं इह लोके परत्र च ।
यस्य विप्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः ॥ ८ ॥
जिसपर ब्राह्मण अथवा अनुचरोंके सहित श्रीशंकर या विष्णुभगवान प्रसन्न हों, उसके लिये इहलोक और परलोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ है ।।८।।
नैव लक्षयते लोको लोकान् पर्यटतोऽपि यान् ।
यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥ ९ ॥
इस दृश्य-प्रपंचके कारण महत्तत्त्वादि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्माको नहीं देख सकते; इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकोंमें विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारीलोग आपको देख नहीं पाते ।।९।।
अधना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः ।
यद्गृहा ह्यर्हवर्याम्बु तृणभूमीश्वरावराः ॥ १० ॥
जिनके घरोंमें आप-जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवकादि किसी अन्य पदार्थको स्वीकार कर लेते हैं, वे गहस्थ धनहीन होनेपर भी धन्य हैं ||१०||
व्यालालयद्रुमा वै तेऽपि अरिक्ताखिलसम्पदः ।
यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थविवर्जिताः ॥ ११ ॥
जिन घरोंमें कभी भगवद्भक्तोंके परमपवित्र चरणोदकके छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकारकी ऋद्धिसिद्धियोंसे भरे होनेपर भी ऐसे वृक्षोंके समान हैं कि जिनपर साँप रहते हैं ।।११।।
स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः ।
चरन्ति श्रद्धया धीरा बाला एव बृहन्ति च ॥ १२ ॥
मुनीश्वरो! आपका स्वागत है। आपलोग तो बाल्यावस्थासे ही मुमुक्षुओंके मार्गका अनुसरण करते हुए एकाग्रचित्तसे ब्रह्मचर्यादि महान् व्रतोंका बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे है ।।१२।।
कच्चिन्नः कुशलं नाथा इन्द्रियार्थार्थवेदिनाम् ।
व्यसनावाप एतस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः ॥ १३ ॥
स्वामियो! हमलोग अपने कर्मोंके वशीभूत होकर विपत्तियोंके क्षेत्ररूप इस संसारमें पड़े हुए केवल इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंको ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं; सो क्या हमारे निस्तारका भी कोई उपाय है ।।१३।।
भवत्सु कुशलप्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते ।
कुशलाकुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तयः ॥ १४ ॥
आपलोगोंसे कुशलप्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरन्तर आत्मामें ही रमण करते हैं। आपमें यह कुशल है और यह अकुशल है—इस प्रकारकी वृत्तियाँ कभी होती ही नहीं ||१४||
तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनाम् ।
सम्पृच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनाञ्जसा भवेत् ॥ १५ ॥
आप संसारानलसे सन्तप्त जीवोंके परम सुहृद् हैं, इसलिये आपमें विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसारमें मनुष्यका किस प्रकार सुगमतासे कल्याण हो सकता है? ||१५||
व्यक्तमात्मवतामात्मा भगवान् आत्मभावनः ।
स्वानां अनुग्रहायेमां सिद्धरूपी चरत्यजः ॥ १६ ॥
यह निश्चय है कि जो आत्मवान् (धीर) पुरुषोंमें ‘आत्मा’ रूपसे प्रकाशित होते हैं और उपासकोंके हृदयमें अपने स्वरूपको प्रकट करनेवाले हैं, वे अजन्मा भगवान् नारायण ही अपने भक्तोंपर कृपा करनेके लिये आप-जैसे सिद्ध पुरुषोंके रूपमें इस पृथ्वीपर विचरा करते हैं ।।१६।।
मैत्रेय उवाच –
पृथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठु मितं मधु ।
स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥ १७ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं राजा पृथुके ये युक्तियुक्त, गम्भीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्रीसनत्कुमारजी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुसकराते हुए कहने लगे ।।१७।।
सनत्कुमार उवाच –
साधु पृष्टं महाराज सर्वभूतहितात्मना ।
भवता विदुषा चापि साधूनां मतिरीदृशी ॥ १८ ॥
श्रीसनत्कुमारजीने कहा-महाराज! आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियोंकेकल्याणकी दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधुपुरुषोंकी बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है ।।१८।।
सङ्गमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः ।
यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः सर्वेषां वितनोति शम् ॥ १९ ॥
सत्पुरुषोंका समागम श्रोता और वक्ता दोनोंको ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभीका कल्याण करते हैं ।।१९।।
अस्त्येव राजन् भवतो मधुद्विषः
पादारविन्दस्य गुणानुवादने ।
रतिर्दुरापा विधुनोति नैष्ठिकी
कामं कषायं मलमन्तरात्मनः ॥ २० ॥
राजन्! श्रीमधुसूदन भगवान्के चरणकमलोंके गुणानुवादमें अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसीको इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जानेपर यह हृदयके भीतर रहनेवाले उस वासनारूप मलको सर्वथानष्ट कर देती है, जो और किसी उपायसे जल्दी नहीं छूटता ।।२०।।
शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां
क्षेमस्य सध्र्यग्विमृशेषु हेतुः ।
असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि
दृढा रतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे च या ॥ २१ ॥
शास्त्र जीवोंके कल्याणके लिये भलीभाँति विचार करनेवाले हैं; उनमें आत्मासे भिन्न देहादिके प्रति वैराग्य तथा अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्ममें सुदृढ़ अनुराग होना—यही कल्याणका साधन निश्चित किया गया है ||२१||
सा श्रद्धया भगवद्धर्मचर्यया
जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया ।
योगेश्वरोपासनया च नित्यं
पुण्यश्रवःकथया पुण्यया च ॥ २२ ॥
अर्थेन्द्रियारामसगोष्ठ्यतृष्णया
तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च ।
विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्
विना हरेर्गुणपीयूषपानात् ॥ २३ ॥
अहिंसया पारमहंस्यचर्यया
स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्र्यसीधुना ।
यमैरकामैर्नियमैश्चाप्यनिन्दया
निरीहया द्वन्द्वतितिक्षया च ॥ २४ ॥
हरेर्मुहुस्तत्परकर्णपूर
गुणाभिधानेन विजृम्भमाणया ।
भक्त्या ह्यसङ्गः सदसत्यनात्मनि
स्यान्निर्गुणे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥ २५ ॥
शास्त्रोंका यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्रके वचनोंमें विश्वास रखनेसे, भागवतधर्मोंका आचरण करनेसे, तत्त्वजिज्ञासासे, ज्ञानयोगकी निष्ठासे, योगेश्वर श्रीहरिकी उपासनासे, नित्यप्रति पुण्यकीर्ति श्रीभगवान्की पावन कथाओंको सुननेसे, जो लोग धन और इन्द्रियोंके भोगोंमें ही रत हैं उनकी गोष्ठीमें प्रेम न रखनेसे, उन्हें प्रिय लगनेवाले पदार्थोंका आसक्तिपूर्वक संग्रह न करनेसे, भगवद्गुणामृतका पान करनेके सिवा अन्य समय आत्मामें ही सन्तुष्ट रहते हुए एकान्तसेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी भी जीवको कष्ट न देतेसे, निवृत्तिनिष्ठासे, आत्महितका अनुसन्धान करते रहनेसे, श्रीहरिके पवित्र चरित्ररूप श्रेष्ठ अमृतका आस्वादन करनेसे, निष्कामभावसे यम-नियमोंका पालन करनेसे, कभी किसीकी निन्दा न करनेसे, योगक्षेमके लिये प्रयत्न न करनेसे, शीतोष्णादि द्वन्द्वोंको सहन करनेसे, भक्तजनोंके कानोंको सुख देनेवाले श्रीहरिके गुणोंका बार-बार वर्णन करनेसे और बढ़ते हुए भक्तिभावसे मनुष्यका कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जड प्रपंचसे वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परब्रह्ममें अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है ।।२२-२५||
यदा रतिर्ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान्
आचार्यवान् ज्ञानविरागरंहसा ।
दहत्यवीर्यं हृदयं जीवकोशं
पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽग्निः ॥ २६ ॥
परब्रह्ममें सुदृढ़ प्रीति हो जानेपर पुरुष सद्गुरुकी शरण लेता है; फिर ज्ञान और वैराग्यके प्रबल वेगके कारण वासनाशून्य हुए अपने अविद्यादि पाँच प्रकारके क्लेशोंसे युक्त अहंकारात्मक अपने लिंगशरीरको वह उसी प्रकार भस्म कर देता है, जैसे अग्नि लकडीसे प्रकट होकर फिर उसीको जला डालती है ।।२६।।
दग्धाशयो मुक्तसमस्ततद्गुणो
नैवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे ।
परात्मनोर्यद् व्यवधानं पुरस्तात्
स्वप्ने यथा पुरुषस्तद्विनाशे ॥ २७ ॥
इस प्रकार लिंग देहका नाश हो जानेपर वह उसके कर्तृत्वादि सभी गुणोंसे मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्नावस्थामें तरह-तरहके पदार्थ देखनेपर भी उससे जग पड़नेपर उनमेंसे कोई चीज दिखायी नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीरके बाहर दिखायी देनेवाले घट-पटादि और भीतर अनुभव होनेवाले सुखदुःखादिको भी नहीं देखता। इस स्थितिके प्राप्त होनेसे पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्माके बीचमें रहकर उनका भेद कर रहे थे ।।२७।।
(अनुष्टुप्)
आत्मानमिन्द्रियार्थं च परं यदुभयोरपि ।
सत्याशय उपाधौ वै पुमान् पश्यति नान्यदा ॥ २८ ॥
जबतक अन्तःकरणरूप उपाधि रहती है, तभीतक पुरुषको जीवात्मा, इन्द्रियोंके विषय और इन दोनोंका सम्बन्ध करानेवाले अहंकारका अनुभव होता है; इसके बाद नहीं ।।२८।।
निमित्ते सति सर्वत्र जलादौ अपि पूरुषः ।
आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥ २९ ॥
बाह्य जगत्में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तोंके रहनेपर ही अपने बिम्ब और प्रतिबिम्बका भेद दिखायी देता है, अन्य समय नहीं ||२९||
इन्द्रियैर्विषयाकृष्टैः आक्षिप्तं ध्यायतां मनः ।
चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव ह्रदात् ॥ ३० ॥
जो लोग विषयचिन्तनमें लगे रहते हैं, उनकी इन्द्रियाँ विषयोंमें फँस जाती हैं तथा मनको भी उन्हींकी ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशयके तीरपर उगे हुए कुशादि अपनी जड़ोंसे उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इन्द्रियासक्त मन बुद्धिकी विचारशक्तिको क्रमशः हर लेता है ||३०||
भ्रश्यत्यनु स्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये ।
तद्रोधं कवयः प्राहुः आत्मापह्नवमात्मनः ॥ ३१ ॥
विचारशक्तिके नष्ट हो जानेपर पूर्वापरकी स्मृति जाती रहती है और स्मृतिका नाश हो जानेपर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञानके नाशको ही पण्डितजन ‘अपने-आप अपना नाश करना’ कहते हैं ||३१||
नातः परतरो लोके पुंसः स्वार्थव्यतिक्रमः ।
यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वं आत्मनः स्वव्यतिक्रमात् ॥ ३२ ॥
जिसके उद्देश्यसे अन्य सब पदार्थोमें प्रियताका बोध होता है-उस आत्माका अपनेद्वारा ही नाश होनेसे जो स्वार्थहानि होती है, उससे बढ़कर लोकमें जीवकी और कोई हानि नहीं है ||३२||
अर्थेन्द्रियार्थाभिध्यानं सर्वार्थापह्नवो नृणाम् ।
भ्रंशितो ज्ञानविज्ञानाद् येनाविशति मुख्यताम् ॥ ३३ ॥
धन और इन्द्रियों के विषयोंका चिन्तन करना मनुष्यके सभी पुरुषार्थोंका नाश करनेवाला है; क्योंकि इनकी चिन्तासे वह ज्ञान और विज्ञानसे भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियोंमें जन्म पाता है ।।३३।।
न कुर्यात्कर्हिचित्सङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः ।
धर्मार्थकाममोक्षाणां यदत्यन्तविघातकम् ॥ ३४ ॥
इसलिये जिसे अज्ञानान्धकारसे पार होनेकी इच्छा हो, उस पुरुषको विषयोंमें आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी प्राप्तिमें बड़ी बाधक है ||३४।।
तत्रापि मोक्ष एवार्थ आत्यन्तिकतयेष्यते ।
त्रैवर्ग्योऽर्थो यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥ ३५ ॥
इन चार पुरुषार्थोंमें भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है; क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थों में सर्वदा कालका भय लगा रहता है ||३५||
परेऽवरे च ये भावा गुणव्यतिकरादनु ।
न तेषां विद्यते क्षेमं ईशविध्वंसिताशिषाम् ॥ ३६ ॥
प्रकृतिमें गुणक्षोभ होनेके बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव-पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशलसे रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। कालभगवान् उन सभीके कुशलोंको कुचलते रहते हैं ।।३६।।
तत्त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थूषां च
देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिरावृतानाम् ।
यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विश्वगाविः
प्रत्यक् चकास्ति भगवान् तमवेहि सोऽस्मि ॥ ३७ ॥
अतः राजन्! जो भगवान् देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकारसे आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियोंके हृदयोंमें जीवके नियामक अन्तर्यामी आत्मारूपसे सर्वत्र साक्षात् प्रकाशित हो रहे हैं उन्हें तुम ‘वह मैं ही हूँ’ ऐसा जानो ||३७।।
यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति
माया विवेकविधुति स्रजि वाहिबुद्धिः ।
तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविशुद्धतत्त्वं
प्रत्यूढकर्मकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये ॥ ३८ ॥
जिस प्रकार मालाका ज्ञान हो जानेपर उसमें सर्पबुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होनेपर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा यह मायामय प्रपंच जिसमें कार्य-कारणरूपसे प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृतिसे परे है, उस नित्यमुक्त, निर्मल और ज्ञानस्वरूप परमात्माको मैं प्राप्त हो रहा हूँ ।।३८||
यत्पादपङ्कजपलाशविलासभक्त्या
कर्माशयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः ।
तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्ध
स्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम् ॥ ३९ ॥
संत-महात्मा जिनके चरणकमलोंके अंगुलिदलकी छिटकती हुई छटाका स्मरण करके अहंकाररूप हृदयग्रन्थिको, जो कर्मोंसे गठित है, इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके अपने अन्तःकरणको निर्विषय करनेवाले संन्यासी भीवैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान् वासुदेवका भजन करो ।।३९।।
कृच्छ्रो महानिह भवार्णवमप्लवेशां
षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीर्षन्ति ।
तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं
कृत्वोडुपं व्यसनमुत्तर दुस्तरार्णम् ॥ ४० ॥
जो लोग मन और इन्द्रियरूप मगरोंसे भरे हुए इस संसारसागरको योगादि दुष्कर साधनोंसे पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुँचना कठिन ही है; क्योंकि उन्हें कर्णधाररूप श्रीहरिका आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान्के आराधनीय चरणकमलोंको नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्रको पार कर लो ।।४०।।
मैत्रेय उवाच –
(अनुष्ट्प्)
स एवं ब्रह्मपुत्रेण कुमारेणात्ममेधसा ।
दर्शितात्मगतिः सम्यक् प्रशस्योवाच तं नृपः ॥ ४१ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-विदुरजी! ब्रह्माजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारजीसे इस प्रकार आत्मतत्त्वका उपदेश पाकर महाराज पृथुने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा ।।४१।।
राजोवाच –
कृतो मेऽनुग्रहः पूर्वं हरिणाऽऽर्तानुकम्पिना ।
तमापादयितुं ब्रह्मन् भगवन् यूयमागताः ॥ ४२ ॥
राजा पृथुने कहा-भगवन्! दीनदयाल श्रीहरिने मुझपर पहले कृपा की थी, उसीको पूर्ण करनेके लिये आपलोग पधारे हैं ।।४२।।
निष्पादितश्च कार्त्स्न्येन भगवद्भिः घृणालुभिः ।
साधूच्छिष्टं हि मे सर्वं आत्मना सह किं ददे ॥ ४३ ॥
आपलोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्यके लिये आपलोग पधारे थे, उसे आपलोगोंने अच्छी तरह सम्पन्न कर दिया। अब, इसके बदले में मैं आपलोगोंको क्या दूँ? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है, वह सब महापुरुषोंका ही प्रसाद है ।।४३।।
प्राणा दाराः सुता ब्रह्मन् गुहाश्च सपरिच्छदाः ।
राज्यं बलं मही कोश इति सर्वं निवेदितम् ॥ ४४ ॥
ब्रह्मन्! प्राण, स्त्री, पुत्र सब प्रकारकी सामग्रियोंसे भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश-यह सब कुछ आप ही लोगोंका है, अतः आपके ही श्रीचरणोंमें अर्पित है ।।४४।।
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।
सर्व लोकाधिपत्यं च वेदशास्त्रविदर्हति ॥ ४५ ॥
वास्तवमें तो सेनापतित्व, राज्य, दण्डविधान और सम्पूर्ण लोकोंके शासनका अधिकार वेद-शास्त्रोंके ज्ञाता ब्राह्मणोंको ही है ।।४५||
स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च ।
तस्यैवानुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः ॥ ४६ ॥
ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसीकी कपासे अन्न खानेको पाते हैं ||४६।।
यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवादे
एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः ।
तुष्यन्त्वदभ्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं
को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम् ॥ ४७ ॥
आपलोग वेदके पारगामी हैं, आपने अध्यात्मतत्त्वका विचार करके हमें निश्चितरूपसे समझा दिया है कि भगवान्के प्रति इस प्रकारकी अभेद-भक्ति ही उनकी उपलब्धिका प्रधान साधन है। आपलोग परम कृपालु हैं। अतः अपने इस दीनोद्धाररूप कर्मसे ही सर्वदा सन्तुष्ट रहें। आपके इस उपकारका बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिये प्रयत्न करना भी अपनी हँसी कराना ही है ।।४७।।
मैत्रेय उवाच –
(अनुष्टुप्)
ते आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः ।
शीलं तदीयं शंसन्तः खेऽभूवन् मिषतां नृणाम् ॥ ४८ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदुरजी! फिर आदिराज पृथुने आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ सनकादिकी पूजा की और वे उनके शीलकी प्रशंसा करते हुए सब लोगोंके सामने ही आकाशमार्गसे चले गये ।।४८।।
वैन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया ।
आप्तकामं इवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥ ४९ ॥
महात्माओंमें अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्तकी एकाग्रतासे आत्मामें ही स्थित रहनेके कारण अपनेको कृतकृत्य-सा अनुभव करने लगे ।।४९।।
कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम् ।
यथोचितं यथावित्तं अकरोद्ब्रह्मसात्कृतम् ॥ ५० ॥
वे ब्रह्मार्पण-बुद्धिसे समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धनके अनुसार सभी कर्म करते थे ।।५०।।
फलं ब्रह्मणि विन्यस्य निर्विषङ्गः समाहितः ।
कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम् ॥ ५१ ॥
इस प्रकार एकाग्र चित्तसे समस्त कर्मोंका फल परमात्माको अर्पण करके आत्माको कर्मोंका साक्षी एवं प्रकृतिसे अतीत देखनेके कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे ।।५१।।
गृहेषु वर्तमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः ।
नासज्जतेन्द्रियार्थेषु निरहंमतिरर्कवत् ॥ ५२ ॥
जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करनेपर भी वस्तुओंके गुण-दोषसे निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी अहंकारशून्य होनेके कारण वे इन्द्रियोंके विषयों में आसक्त नहीं हुए ||५२।।।
एवं अध्यात्मयोगेन कर्माणि अनुसमाचरन् ।
पुत्रान् उत्पादयामास पञ्चार्चिष्यात्मसम्मतान् ॥ ५३ ॥
इस प्रकार आत्मनिष्ठामें स्थित होकर सभी कर्तव्यकर्मोंका यथोचित रीतिसे अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्चिके गर्भसे अपने अनुरूप पाँच पुत्र उत्पन्न किये ||५३।।
विजिताश्वं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं वृकम् ।
सर्वेषां लोकपालानां दधारैकः पृथुर्गुणान् ॥ ५४ ॥
गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले स्वे स्वेऽच्युतात्मकः ।
मनोवाग् वृत्तिभिः सौम्यैः गुणैः संरञ्जयन् प्रजाः ॥ ५५ ॥
राजेत्यधान् नामधेयं सोमराज इवापरः ।
सूर्यवद्विसृजन्गृह्णन् प्रतपंश्च भुवो वसु ॥ ५६ ॥
उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान्के अंश थे। वे समय-समयपर, जब-जब आवश्यक होता था, जगत्के प्राणियोंकी रक्षाके लिये अकेले ही समस्त लोकपालोंके गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणोंके द्वारा प्रजाका रंजन करते रहनेसे दूसरे चन्द्रमाके समान उनका ‘राजा’ यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गरमीमें पृथ्वीका जल खींचकर वर्षाकालमें उसे पुनः पृथ्वीपर बरसा देता है तथा अपनी किरणोंसे सबको ताप पहुँचाता है, उसी प्रकार वे कररूपसे प्रजाका धन लेकर उसे दुष्कालादिके समय मुक्तहस्तसे प्रजाकेहितमें लगा देते थे तथा सबपर अपना प्रभाव जमाये रखते थे ।।५४-५६।।
दुर्धर्षस्तेजसेवाग्निः महेन्द्र इव दुर्जयः ।
तितिक्षया धरित्रीव द्यौरिवाभीष्टदो नृणाम् ॥ ५७ ॥
वे तेजमें अग्निके समान दुर्धर्ष, इन्द्रके समान अजेय, पृथ्वीके समान क्षमाशील और स्वर्गके समान मनुष्योंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले थे ।।५७।।
वर्षति स्म यथाकामं पर्जन्य इव तर्पयन् ।
समुद्र इव दुर्बोधः सत्त्वेनाचलराडिव ॥ ५८ ॥
समय-समयपर प्रजाजनोंको तृप्त करनेके लिये वे मेघके समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथसे लुटाते रहते थे। वे समुद्रके समान गम्भीर और पर्वतराज सुमेरुके समान धैर्यवान् भी थे ।।५८।।
धर्मराडिव शिक्षायां आश्चर्ये हिमवानिव ।
कुवेर इव कोशाढ्यो गुप्तार्थो वरुणो यथा ॥ ५९ ॥
महाराज पृथु दुष्टोंके दमन करनेमें यमराजके समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओंके संग्रहमें हिमालयके समान, कोशकी समृद्धि करनेमें कुबेरके समान और धनको छिपानेमें वरुणके समान थे ।।५९।।
मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन महसौजसा ।
अविषह्यतया देवो भगवान् भूतराडिव । ॥ ६० ॥
शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी पटुता तथा पराक्रममें सर्वत्र गतिशील वायुके समान और तेजकी असह्यतामें भगवान् शंकरके समान थे ।।६०।।
कन्दर्प इव सौन्दर्ये मनस्वी मृगराडिव ।
वात्सल्ये मनुवन्नॄणां प्रभुत्वे भगवानजः । ॥ ६१ ॥
सौन्दर्यमें कामदेवके समान, उत्साहमें सिंहके समान, वात्सल्यमें मनुके समान और मनुष्योंके आधिपत्यमें सर्वसमर्थ ब्रह्माजीके समान थे ।।६१।।
बृहस्पतिर्ब्रह्मवादे आत्मवत्त्वे स्वयं हरिः ।
भक्त्या गोगुरुविप्रेषु विष्वक्सेनानुवर्तिषु ।
ह्रिया प्रश्रयशीलाभ्यां आत्मतुल्यः परोद्यमे । ॥ ६२ ॥
ब्रह्मविचारमें बृहस्पति, इन्द्रियजयमें साक्षात् श्रीहरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवद्भक्तोंकी भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणोंमें अपने ही समान (अनुपम) थे ।।६२।।
कीर्त्योर्ध्वगीतया पुम्भिः त्रैलोक्ये तत्र तत्र ह ।
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु स्त्रीणां रामः सतामिव । ॥ ६३ ॥
लोग त्रिलोकीमें सर्वत्र उच्च स्वरसे उनकी कीर्तिका गान करते थे, इससे वे स्त्रियोंतकके कानोंमें वैसे ही प्रवेश पाये हुए थे जैसे सत्पुरुषोंके हृदयमें श्रीराम ।।६३।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
चतुर्थस्कन्धे पृथुचरिते द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥