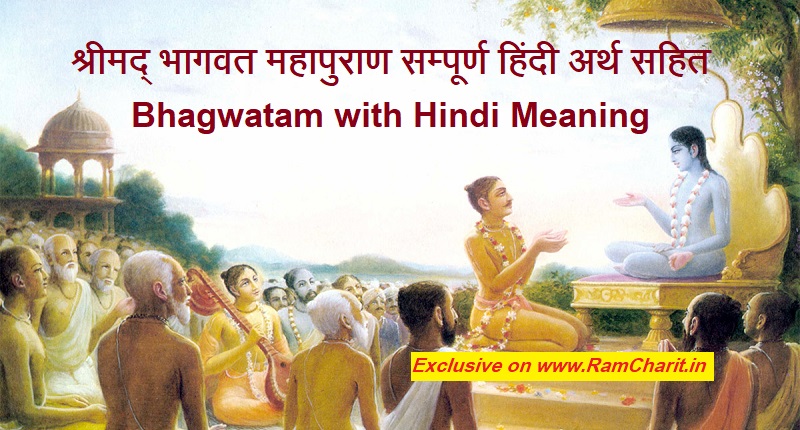श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 4 अध्याय 8
श्रीमद्भागवतपुराणम्
चतुर्थ स्कन्ध अध्यायः ८
मैत्रेय उवाच –
(अनुष्टुप्)
सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसोऽरुणिर्यतिः ।
नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसउ ऊर्ध्वरेतसः ॥ १ ॥
मृषाधर्मस्य भार्यासीद् दम्भं मायां च शत्रुहन् ।
असूत मिथुनं तत्तु निर्ऋतिर्जगृहेऽप्रजः ॥ २ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-शत्रुसूदन विदुरजी! सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणि और यति ब्रह्माजीके इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रोंने गृहस्थाश्रममें प्रवेश नहीं किया (अतः उनकेकोई सन्तान नहीं हुई)। अधर्म भी ब्रह्माजीका ही पुत्र था, उसकी पत्नीका नाम था मृषा। उसके दम्भ नामक पुत्र और माया नामकी कन्या हुई। उन दोनोंको निर्ऋति ले गया, क्योंकि उसके कोई सन्तान न थी ।।१-२।।
hHFA
तयोः समभवल्लोभो निकृतिश्च महामते ।
ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद्दुरुक्तिः स्वसा कलिः ॥ ३ ॥
दम्भ और मायासे लोभ और निकृति (शठता)-का जन्म हआ, उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलि (कलह) और उसकी बहिन दुरुक्ति (गाली) उत्पन्न हुए ||३||
दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युं च सत्तम ।
तयोश्च मिथुनं जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥ ४ ॥
साधुशिरोमणे! फिर दुरुक्तिसे कलिने भय और मृत्युको उत्पन्न किया तथा उन दोनोंके संयोगसे यातना और निरय (नरक)-का जोड़ा उत्पन्न हुआ ।।४।।
सङ्ग्रहेण मयाऽऽख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ ।
त्रिः श्रुत्वैतत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम् ॥ ५ ॥
निष्पाप विदुरजी! इस प्रकार मैंने संक्षेपसे तुम्हें प्रलयका कारणरूप यह अधर्मका वंश सुनाया। यह अधर्मका त्याग कराकर पुण्य-सम्पादनमें हेतु बनता है; अतएव इसका वर्णन तीन बार सुनकर मनुष्य अपने मनकी मलिनता दूर कर देता है ।।५।।
अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरूद्वह ।
स्वायम्भुवस्यापि मनोः हरेरंशांशजन्मनः ॥ ६ ॥
कुरुनन्दन! अब मैं श्रीहरिके अंश (ब्रह्माजी)-के अंशसे उत्पन्न हुए पवित्रकीर्ति महाराज स्वायम्भुव मनुके पुत्रोंके वंशका वर्णन करता हूँ ||६||
प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापतेः सुतौ ।
वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ ॥ ७ ॥
महारानी शतरूपा और उनके पति स्वायम्भुव मनुसे प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो पुत्र हुए। भगवान् वासुदेवकी कलासे उत्पन्न होनेके कारण ये दोनों संसारकी रक्षामें तत्पर रहते थे ।।७।।
जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः ।
सुरुचिः प्रेयसी पत्युः नेतरा यत्सुतो ध्रुवः ॥ ८ ॥
उत्तानपादके सुनीति और सुरुचि नामकी दो पत्नियाँ थीं। उनमें सरुचि राजाको अधिक प्रिय थी; सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी ।।८।।
एकदा सुरुचेः पुत्रं अङ्कमारोप्य लालयन् ।
उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत ॥ ९ ॥
एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचिके पुत्र उत्तमको गोदमें बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुवने भी गोदमें बैठना चाहा, परन्तु राजाने उसका स्वागत नहीं किया ।।९।।
तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवम् ।
सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः सेर्ष्यमाहातिगर्विता ॥ १० ॥
उस समय घमण्डसे भरी हुई सुरुचिने अपनी सौतके पुत्र ध्रुवको महाराजकी गोदमें आनेका यत्न करते देख उनके सामने ही उससे डाहभरे शब्दोंमें कहा ।।१०।।
न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवान् आरोढुमर्हति ।
न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षौ अपि नृपात्मजः ॥ ११ ॥
‘बच्चे! तू राजसिंहासनपर बैठनेका अधिकारी नहीं है। तू भी राजाका ही बेटा है, इससे क्या हुआ; तुझको मैंने तो अपनी कोखमें नहीं धारण किया ।।११।।
बालोऽसि बत नात्मानं अन्यस्त्रीगर्भसम्भृतम् ।
नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः ॥ १२ ॥
तू अभी नादान है, तुझे पता नहीं है कि तने किसी दूसरी स्त्रीके गर्भसे जन्म लिया है; तभी तो ऐसे दुर्लभ विषयकी इच्छा कर रहा है ।।१२।।
तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे ।
गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम् ॥ १३ ॥
यदि तुझे राजसिंहासनकी इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्रीनारायणकी आराधना कर और उनकी कृपासे मेरे गर्भमें आकर जन्म ले’ ||१३||
मैत्रेय उवाच –
मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्धः
श्वसन् रुषा दण्डहतो यथाहिः ।
हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं
जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम् ॥ १४ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—विदरजी! जिस प्रकार डंडेकी चोट खाकर साँप फँफकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली माँके कठोर वचनोंसे घायल होकर ध्रव क्रोधके मारे लंबी-लंबी साँस लेने लगा। उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुँहसे एक शब्द भी नहीं बोले। तब पिताको छोडकर ध्रव रोता हआ अपनी माताके पास आया ।।१४।।
तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं
सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य बालम् ।
निशम्य तत्पौरमुखान्नितान्तं
सा विव्यथे यद्गदितं सपत्न्या ॥ १५ ॥
उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक-सिसककर रो रहा था। सुनीतिने बेटेको गोदमें उठा लिया
और जब महलके दूसरे लोगोंसे अपनी सौत सुरुचिकी कही हुई बातें सुनी, तब उसे भी बड़ा दुःख हुआ ||१५||
सोत्सृज्य धैर्यं विललाप शोक
दावाग्निना दावलतेव बाला ।
वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोज
श्रिया दृशा बाष्पकलामुवाह ॥ १६ ॥
उसका धीरज टूट गया। वह दावानलसे जली हुई बेलके समान शोकसे सन्तप्त होकर मुरझा गयी तथा विलाप करने लगी। सौतकी बातें याद आनेसे उसके कमलसरीखे नेत्रोंमें आँसू भर आये ।।१६।।
दीर्घं श्वसन्ती वृजिनस्य पारं
अपश्यती बालकमाह बाला ।
मामङ्गलं तात परेषु मंस्था
भुङ्क्ते जनो यत्परदुःखदस्तत् ॥ १७ ॥
उस बेचारीको अपने दुःखपारावारका कहीं अन्त ही नहीं दिखायी देता था। उसने गहरी साँस लेकर ध्रुवसे कहा, ‘बेटा! तू दूसरोंके लिये किसी प्रकारके अमंगलकी कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरोंको दुःख देता है, उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है ।।१७।।
सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे
यद् दुर्भगाया उदरे गृहीतः ।
स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते यां
भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्माम् ॥ १८ ॥
सुरुचिने जो कुछ कहा है, ठीक ही है; क्योंकि महाराजको मुझे’पत्नी’ तो क्या, ‘दासी’ स्वीकार करनेमें भी लज्जा आती है। तूने मुझ मन्दभागिनीके गर्भसे ही जन्म लिया है और मेरे ही दूधसे तू पला है ।।१८।।
आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वं
उक्तं समात्रापि यदव्यलीकम् ।
आराधयाधोक्षजपादपद्मं
यदीच्छसेऽध्यासनमुत्तमो यथा ॥ १९ ॥
बेटा! सुरुचिने तेरी सौतेली माँ होनेपर भी बात बिलकुल ठीक कही है; अतः यदि राजकुमार उत्तमके समान राजसिंहासनपर बैठना चाहता है तो द्वेषभाव छोड़कर उसीका पालन कर। बस, श्रीअधोक्षजभगवान्के चरणकमलोंकी आराधनामें लग जा ।।१९।।
यस्याङ्घ्रिपद्मं परिचर्य विश्व
विभावनायात्तगुणाभिपत्तेः ।
अजोऽध्यतिष्ठत्खलु पारमेष्ठ्यं
पदं जितात्मश्वसनाभिवन्द्यम् ॥ २० ॥
संसारका पालन करनेके लिये सत्त्वगुणको अंगीकार करनेवाले उन श्रीहरिके चरणोंकी आराधना करनेसे ही तेरे परदादा श्रीब्रह्माजीको वह सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हआ है, जो मन और प्राणोंको जीतनेवाले मनियोंके द्वारा भी वन्दनीय है ।।२०।।
तथा मनुर्वो भगवान्पितामहो
यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः ।
इष्ट्वाभिपेदे दुरवापमन्यतो
भौमं सुखं दिव्यमथापवर्ग्यम् ॥ २१ ॥
इसी प्रकार तेरे दादा स्वायम्भव मनुने भी बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञोंके द्वारा अनन्यभावसे उन्हीं भगवान्की आराधना की थी; तभी उन्हें दूसरोंके लिये अति दुर्लभ लौकिक, अलौकिक तथा मोक्षसुखकी प्राप्ति हुई ।।२१।।
तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलं
मुमुक्षुभिर्मृग्यपदाब्जपद्धतिम् ।
अनन्यभावे निजधर्मभाविते
मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम् ॥ २२ ॥
‘बेटा! तू भी उन भक्तवत्सल श्रीभगवान्का ही आश्रय ले। जन्म-मृत्युके चक्रसे छूटनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुलोग निरन्तर उन्हींके चरणकमलोंके मार्गकी खोज किया करते हैं। तू स्वधर्मपालनसे पवित्र हुए अपने चित्तमें श्रीपुरुषोत्तमभगवान्को बैठा ले तथा अन्य सबका चिन्तन छोड़कर केवल उन्हींका भजन कर ।।२२।।
नान्यं ततः पद्मपलाशलोचनाद्
दुःखच्छिदं ते मृगयामि कञ्चन ।
यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मया
श्रियेतरैरङ्ग विमृग्यमाणया ॥ २३ ॥
बेटा! उन कमल-दल-लोचन श्रीहरिको छोड़कर मुझे तो तेरे दुःखको दूर करनेवाला और कोई दिखायी नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करनेके लिये ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूँढ़ते रहते हैं, वे श्रीलक्ष्मीजी भी दीपककी भाँति हाथमें कमल लिये निरन्तर उन्हीं श्रीहरिकी खोज किया करती हैं’ ।।२३।।
मैत्रेय उवाच –
(अनुष्टुप्)
एवं सञ्जल्पितं मातुः आकर्ण्यार्थागमं वचः ।
सन्नियम्यात्मनाऽऽत्मानं निश्चक्राम पितुः पुरात् ॥ २४ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं—माता सुनीतिने जो वचन कहे, वे अभीष्ट वस्तुकी प्राप्तिका मार्ग दिखलानेवाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुवने बुद्धिद्वारा अपने चित्तका समाधान किया। इसके बाद वे पिताके नगरसे निकल पड़े ||२४||
नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् ।
स्पृष्ट्वा मूर्धन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥ २५ ॥
यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बातको जानकर नारदजी वहाँ आये। उन्होंने ध्रुवके मस्तकपर अपना पापनाशक कर-कमल फेरते हुए मन-ही-मन विस्मित होकर कहा ।।२५।।
अहो तेजः क्षत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम् ।
बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्वचः ॥ २६ ॥
‘अहो! क्षत्रियोंका कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा-सा भी मान-भंग नहीं सह सकते। देखो, अभी तो यह नन्हा-सा बच्चा है; तो भी इसके हृदयमें सौतेली माताके कटु वचन घर कर गये हैं’ ||२६||
नारद उवाच –
नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक ।
लक्षयामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु ॥ २७ ॥
तत्पश्चात् नारदजीने ध्रवसे कहा—बेटा! अभी तो तु बच्चा है, खेल-कूदमें ही मस्त रहता है; हम नहीं समझते कि इस उम्रमें किसी बातसे तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है ।।२७।।
विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतवः ।
पुंसो मोहमृते भिन्ना यल्लोके निजकर्मभिः ॥ २८ ॥
यदि तुझे मानापमानका विचार ही हो, तो बेटा! असलमें मनुष्यके असन्तोषका कारण मोहके सिवा और कुछ नहीं है। संसारमें मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान-अपमान या सुख-दुःख आदिको प्राप्त होता है ।।२८।।
परितुष्येत् ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः ।
दैवोपसादितं यावद् वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः ॥ २९ ॥
तात! भगवान्की गति बड़ी विचित्र है! इसलिये उसपर विचार करके बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि दैववश उसे जैसी भी परिस्थितिका सामना करना पड़े, उसीमें सन्तुष्ट रहे ।।२९।।
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि ।
यत्प्रसादं स वै पुंसां दुराराध्यो मतो मम ॥ ३० ॥
अब, माताके उपदेशसे तू योगसाधनद्वारा जिन भगवान्की कृपा प्राप्त करने चला है—मेरे विचारसे साधारण पुरुषोंके लिये उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है ।।३०।।
मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्गेनोरुजन्मभिः ।
न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोगसमाधिना ॥ ३१ ॥
योगीलोग अनेकों जन्मोंतक अनासक्त रहकर समाधियोगके द्वारा बड़ी-बड़ी कठोर साधनाएँ करते रहते हैं, परन्तु भगवान्के मार्गका पता नहीं पाते ।।३१।।
अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः ।
यतिष्यति भवान् काले श्रेयसां समुपस्थिते ॥ ३२ ॥
इसलिये तू यह व्यर्थका हठ छोड़ दे और घर लौट जा; बड़ा होनेपर जब परमार्थ-साधनका समय आवे, तब उसके लिये प्रयत्न कर लेना ||३२||
यस्य यद् दैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः ।
आत्मानं तोषयन् देही तमसः पारमृच्छति ॥ ३३ ॥
विधाताके विधानके अनुसार सुख-दुःख जो कुछ भी प्राप्त हो, उसीमें चित्तको सन्तुष्ट रखना चाहिये। यों करनेवाला पुरुष मोहमय संसारसे पार हो जाता है ।।३३।।
गुणाधिकान्मुदं लिप्सेद् अनुक्रोशं गुणाधमात् ।
मैत्रीं समानादन्विच्छेत् न तापैरभिभूयते ॥ ३४ ॥
मनुष्यको चाहिये कि अपनेसे अधिक गुणवानको देखकर प्रसन्न हो; जो कम गुणवाला हो, उसपर दया करे और जो अपने समान गुणवाला हो, उससे मित्रताका भाव रखे। यों करनेसेउसे दुःख कभी नहीं दबा सकते ।।३४।।
ध्रुव उवाच –
सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम् ।
दर्शितः कृपया पुंसां दुर्दर्शोऽस्मद्विधैस्तु यः ॥ ३५ ॥
ध्रुवने कहा-भगवन्! सुख-दुःखसे जिनका चित्त चंचल हो जाता है, उन लोगोंके लिये आपने कृपा करके शान्तिका यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया। परन्तु मुझ-जैसे अज्ञानियोंकी दृष्टि यहाँतक नहीं पहुँच पाती ।।३५।।
अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्त्रं घोरमुपेयुषः ।
सुरुच्या दुर्वचोबाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि ॥ ३६ ॥
इसके सिवा, मुझे घोर क्षत्रियस्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझमें विनयका प्रायः अभाव है; सुरुचिने अपने कटुवचनरूपी बाणोंसे मेरे हृदयको विदीर्ण कर डाला है; इसलिये उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता ||३६।।
पदं त्रिभुवनोत्कृष्टं जिगीषोः साधु वर्त्म मे ।
ब्रूहि अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम् ॥ ३७ ॥
ब्रह्मन्! मैं उस पदपर अधिकार करना चाहता हूँ, जो त्रिलोकीमें सबसे श्रेष्ठ है तथा जिसपर मेरे बाप-दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहां हो सके हैं। आप मुझे उसीकी प्राप्तिका कोई अच्छा-सा मार्ग बतलाइये ||३७||
नूनं भवान् भगवतो योऽङ्गजः परमेष्ठिनः ।
वितुदन्नटते वीणां हिताय जगतोऽर्कवत् ॥ ३८ ॥
आप भगवान् ब्रह्माजीके पुत्र हैं और संसारके कल्याणके लिये ही वीणा बजाते सूर्यकी भाँति त्रिलोकीमें विचरा करते हैं ।।३८।।
मैत्रेय उवाच –
इत्युदाहृतमाकर्ण्य भगवान् नारदस्तदा ।
प्रीतः प्रत्याह तं बालं सद्वाक्यं अनुकम्पया ॥ ३९ ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-ध्रुवकी बात सुनकर भगवान् नारदजी बड़े प्रसन्न हुए और उसपर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे ।।३९।।
नारद उवाच –
जनन्याभिहितः पन्थाः स वै निःश्रेयसस्य ते ।
भगवान् वासुदेवस्तं भज तं प्रवणात्मना ॥ ४० ॥
श्रीनारदजीने कहा—बेटा! तेरी माता सुनीतिने तुझे जो कुछ बताया है, वही तेरे लिये परम कल्याणका मार्ग है। भगवान् वासुदेव ही वह उपाय हैं, इसलिये तू चित्त लगाकर उन्हीका भजन कर ||४०||
धर्मार्थकाममोक्षाख्यं य इच्छेत् श्रेय आत्मनः ।
एकं ह्येव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम् ॥ ४१ ॥
जिस पुरुषको अपने लिये धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप पुरुषार्थकी अभिलाषा हो, उसके लिये उनकी प्राप्तिका उपाय एकमात्र श्रीहरिके चरणोंका सेवन ही है ।।४१।।
तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि ।
पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः ॥ ४२ ॥
बेटा! तेरा कल्याण होगा, अब त श्रीयमनाजीके तटवर्ती परम पवित्र मधुवनको जा। वहाँ श्रीहरिका नित्य-निवास है ।।४२||
स्नात्वानुसवनं तस्मिन् कालिन्द्याः सलिले शिवे ।
कृत्वोचितानि निवसन् आत्मनः कल्पितासनः ॥ ४३ ॥
वहाँ श्रीकालिन्दीके निर्मल जलमें तीनों समय स्नान करके नित्यकर्मसे निवृत्त हो यथाविधि आसन बिछाकर स्थिरभावसे बैठना ।।४३||
प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रियमनोमलम् ।
शनैर्व्युदस्याभिध्यायेन् मनसा गुरुणा गुरुम् ॥ ४४ ॥
फिर रेचक, पूरक और कुम्भक-तीन प्रकारके प्राणायामसे धीरे-धीरे प्राण, मन और इन्द्रियके दोषोंको दूरकर धैर्ययुक्त मनसे परमगुरु श्रीभगवान्का इस प्रकार ध्यान करना ।।४४।।
प्रसादाभिमुखं शश्वत् प्रसन्नवदनेक्षणम् ।
सुनासं सुभ्रुवं चारु कपोलं सुरसुन्दरम् ॥ ४५ ॥
भगवान्के नेत्र और मुख निरन्तर प्रसन्न रहते हैं; उन्हें देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नतापूर्वक भक्तको वर देनेके लिये उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौंहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं; वे सभी देवताओंमें परम सुन्दर हैं ।।४५||
तरुणं रमणीयाङ्गं अरुणोष्ठेक्षणाधरम् ।
प्रणताश्रयणं नृम्णं शरण्यं करुणार्णवम् ॥ ४६ ॥
उनकी तरुण अवस्था है; सभी अंग बड़े सुडौल हैं; लाल-लाल होठ और रतनारे नेत्र हैं। वे प्रणतजनोंको आश्रय देनेवाले, अपार सुखदायक, शरणागतवत्सल और दयाके समुद्र हैं ।।४६।।
श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनम् ।
शङ्खचक्रगदापद्मैः अभिव्यक्तचतुर्भुजम् ॥ ४७ ॥
उनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है; उनका शरीर सजल जलधरके समान श्यामवर्ण है; वे परम पुरुष श्यामसुन्दर गलेमें वनमाला धारण किये हुए हैं और उनकी चार भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं ||४७।।
किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम् ।
कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकौशेयवाससम् ॥ ४८ ॥
उनके अंग-प्रत्यंग किरीट, कुण्डल, केयूर और कंकणादि आभूषणोंसे विभूषित हैं; गला कौस्तुभमणिकी भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीरमें रेशमी पीताम्बर है ।।४८।।
काञ्चीकलापपर्यस्तं लसत्काञ्चन नूपुरम् ।
दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम् ॥ ४९ ॥
उनके कटिप्रदेशमें कांचनकी करधनी और चरणोंमें सुवर्णमय नूपुर (पैजनी) सुशोभित हैं। भगवान्का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शान्त तथा मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाला है ।।४९||
पद्भ्यां नखमणिश्रेण्या विलसद्भ्यां समर्चताम् ।
हृत्पद्मकर्णिकाधिष्ण्यं आक्रम्यात् मन्यवस्थितम् ॥ ५० ॥
जो लोग प्रभुका मानस-पूजन करते हैं, उनके अन्तःकरणमें वे हृदयकमलकी कर्णिकापर अपने नख-मणिमण्डित मनोहर पादारविन्दोंको स्थापित करके विराजते हैं ।।५०||
स्मयमानं अभिध्यायेत् सानुरागावलोकनम् ।
नियतेनैकभूतेन मनसा वरदर्षभम् ॥ ५१ ॥
इस प्रकार धारणा करते-करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाय तब उन वरदायक प्रभुका मन-ही-मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुरागभरी दृष्टिसे निहारते हुए मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं ||५१||
एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः ।
निर्वृत्या परया तूर्णं सम्पन्नं न निवर्तते ॥ ५२ ॥
भगवानकी मंगलमयी मूर्तिका इस प्रकार निरन्तर ध्यान करनेसे मन शीघ्र ही परमानन्दमें डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहाँसे लौटता नहीं ।।५२।।
जपश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मज ।
यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान् ॥ ५३ ॥
राजकुमार! इस ध्यानके साथ जिस परम गुह्य मन्त्रका जप करना चाहिये, वह भी बतलाता हूँ सुन। इसका सात रात जप करनेसे मनुष्य आकाशमें विचरनेवाले सिद्धोंकादर्शन कर सकता है ।।५३||
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद् द्रव्यमयीं बुधः ।
सपर्यां विविधैर्द्रव्यैः देशकालविभागवित् ॥ ५४ ॥
वह मन्त्र है—’ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’। किस देश और किस कालमें कौन वस्त उपयोगी है—इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुषको इस मन्त्रके द्वारा तरह-तरहकी सामग्रियोंसे भगवान्की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिये ।।५४।।।
सलिलैः शुचिभिर्माल्यैः वन्यैर्मूलफलादिभिः ।
शस्ताङ्कुरांशुकैश्चार्चेत् तुलस्या प्रियया प्रभुम् ॥ ५५ ॥
प्रभुका पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि, पूजामें विहित दूर्वादि अंकुर, वनमें ही प्राप्त होनेवाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसीसे करना चाहिये ।।५५||
लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षित्यम्ब्वादिषु वार्चयेत् ।
आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवाङ्मितवन्यभुक् ॥ ५६ ॥
यदि शिला आदिकी मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदिमें
ही भगवान्की पूजा करे। सर्वदा संयतचित्त, मननशील, शान्त और मौन रहे तथा जंगली फल-मूलादिका परिमित आहार करे ||५६।।
स्वेच्छावतारचरितैः अचिन्त्यनिजमायया ।
करिष्यति उत्तमश्लोकः तद् ध्यायेद् हृदयङ्गमम् ॥ ५७ ॥
इसके सिवा पुण्यकीर्ति श्रीहरि अपनी अनिर्वचनाया मायाके द्वारा अपनी ही इच्छासे अवतार लेकर जो-जो मनोहर चरित्र करनेवाले हैं, उनका मन-ही-मन चिन्तन करता रहे ||५७||
परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः ।
ता मंत्रहृदयेनैव प्रयुञ्ज्यान् मंत्रमूर्तये ॥ ५८ ॥
प्रभुकी पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका विधान किया गया है, उन्हें मन्त्रमूर्ति श्रीहरिको द्वादशाक्षर मन्त्रके द्वारा ही अर्पण करे ।।५८।।
एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम् ।
परिचर्यमाणो भगवान् भक्तिमत्परिचर्यया ॥ ५९ ॥
पुंसां अमायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः ।
श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम् । ॥ ६० ॥
इस प्रकार जब हृदयस्थित हरिका मन, वाणी और शरीरसे भक्तिपूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्छलभावसे भलीभाँति भजन करनेवाले अपने भक्तोंके भावको बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छाके अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्षरूप कल्याण प्रदान करते हैं ।।५९-६०।।
विरक्तश्चेन्द्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा ।
तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विमुक्तये । ॥ ६१ ॥
यदि उपासकको इन्द्रियसम्बन्थी भोगोंसे वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्षप्राप्तिके लिये अत्यन्त भक्तिपूर्वक अविच्छिन्नभावसे भगवान्का भजन करे ।।६१।।
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपार्भकः ।
ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्चरणचर्चितम् । ॥ ६२ ॥
श्रीनारदजीसे इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुवने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनन्तर उन्होंने भगवान्के चरणचिह्नोंसे अंकित परम पवित्र मधुवनकी यात्रा की ||६२||
तपोवनं गते तस्मिन् प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः ।
अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम् । ॥ ६३ ॥
ध्रुवके तपोवनकी ओर चले जानेपर नारदजी महाराज उत्तानपादके महलमें पहुँचे। राजाने उनकी यथायोग्य उपचारोंसे पूजा की; तब उन्होंने आरामसे आसनपर बैठकर राजासे पूछा ।।६३।।
नारद उवाच –
राजन् किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यता ।
किं वा न रिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः । ॥ ६४ ॥
श्रीनारदजीने कहा–राजन्! तुम्हारा मुख सूखा हुआ है, तुम बड़ी देरसे किस सोचविचारमें पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ और काममेंसे किसीमें कोई कमी तो नहीं आ गयी? ||६४।।
राजोवाच –
सुतो मे बालको ब्रह्मन् स्त्रैणेना-करुणात्मना ।
निर्वासितः पञ्चवर्षः सह मात्रा महान्कविः । ॥ ६५ ॥
राजाने कहा-ब्रह्मन्! मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूँ। हाय, मैंने अपने पाँच वर्षके नन्हेसे बच्चेको उसकी माताके साथ घरसे निकाल दिया। मुनिवर! वह बड़ा ही बुद्धिमान् था ।।६५||
अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मा स्मादन्त्यर्भकं वृकाः ।
श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानमुखाम्बुजम् ॥ ६६ ॥
उसका कमल-सा मुख भूखसे कुम्हला गया होगा, वह थककर कहीं रास्तेमें पड़ गया होगा। ब्रह्मन्! उस असहाय बच्चेको वनमें कहीं भेड़िये न खा जाय ||६६||
अहो मे बत दौरात्म्यं स्त्रीजितस्योपधारय ।
योऽङ्कं प्रेम्णाऽऽरुरुक्षन्तं नाभ्यनन्दमसत्तमः । ॥ ६७ ॥
अहो! मैं कैसा स्त्रीका गुलाम हूँ! मेरी कुटिलता तो देखिये—वह बालक प्रेमवश मेरी गोदमें चढना चाहता था, किन्तु मुझ दुष्टने उसका तनिक भी आदर नहीं किया ।।६७।।।
नारद उवाच –
मा मा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते ।
तत्प्रभावं अविज्ञाय प्रावृङ्क्ते यद्यशो जगत् । ॥ ६८ ॥
श्रीनारदजीने कहा–राजन्! तुम अपने बालककी चिन्ता मत करो। उसके रक्षक भगवान् हैं। तुम्हें उसके प्रभावका पता नहीं है, उसका यश सारे जगत्में फैल रहा है ।।६८।।
सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभुः ।
ऐष्यत्यचिरतो राजन् यशो विपुलयंस्तव । ॥ ६९ ॥
वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस कामको बड़े-बड़े लोकपाल भी नहीं कर सके, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आयेगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा ।।६९।।
मैत्रेय उवाच –
इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः ।
राजलक्ष्मीमनादृत्य पुत्रं एवान्वचिन्तयत् ॥ ७० ॥
श्रीमैत्रेयजी कहते हैं-देवर्षि नारदजीकी बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाटकी
ओरसे उदासीन होकर निरन्तर पुत्रकी ही चिन्तामें रहने लगे ||७०।।
तत्राभिषिक्तः प्रयतः तां उपोष्य विभावरीम् ।
समाहितः पर्यचर दृष्यादेशेन पूरुषम् ॥ ७१ ॥
इधर ध्रुवजीने मधुवनमें पहुँचकर यमुनाजीमें स्नान किया और उस रात पवित्रतापूर्वक उपवास करके श्रीनारदजीकेउपदेशानुसार एकाग्रचित्तसे परमपुरुष श्रीनारायणकी उपासना आरम्भ कर दी ।।७१।।
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः ।
आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येऽर्चयन् हरिम् ॥ ७२ ॥
उन्होंने तीन-तीन रात्रिके अन्तरसे शरीरनिर्वाहके लिये केवल कैथ और बेरके फल खाकर श्रीहरिकी उपासना करते हुए एक मास व्यतीत किया ।।७२।।
द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेऽर्भको दिने ।
तृणपर्णादिभिः शीर्णैः कृतान्नोऽभ्यर्चयन् विभुम् ॥ ७३ ॥
दूसरे महीने में उन्होंने छः-छः दिनके पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान्का भजन किया ||७३।।
तृतीयं चानयन् मासं नवमे नवमेऽहनि ।
अब्भक्ष उत्तमश्लोकं उपाधावत्समाधिना ॥ ७४ ॥
तीसरा महीना नौनौ दिनपर केवल जल पीकर समाधियोगके द्वारा श्रीहरिकी आराधना करते हुए बिताया ।।७४।।
चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्वादशेऽहनि ।
वायुभक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत् ॥ ७५ ॥
चौथे महीने में उन्होंने श्वासको जीतकर बारह-बारह दिनके बाद केवल वायु पीकर ध्यानयोगद्वारा भगवान्की आराधना की ।।७५||
पञ्चमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः ।
ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥ ७६ ॥
पाँचवाँ मास लगनेपर राजकुमार ध्रुव श्वासको जीतकर परब्रह्मका चिन्तन करते हुए एक पैरसे खंभेके समान निश्चल भावसे खड़े हो गये ।।७६।।
सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ।
ध्यायन् भगवतो रूपं नाद्राक्षीत् किंचनापरम् ॥ ७७ ॥
उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इन्द्रियोंके नियामक अपने मनको सब ओरसे खींच लिया तथा हृदयस्थित हरिके स्वरूपका चिन्तन करते हुए चित्तको किसी दूसरी ओर न जाने दिया ।।७७।।
आधारं महदादीनां प्रधानपुरुषेश्वरम् ।
ब्रह्म धारयमाणस्य त्रयो लोकाश्चकम्पिरे ॥ ७८ ॥
जिस समय उन्होंने महदादि सम्पूर्ण तत्त्वोंके आधार तथा प्रकृति और पुरुषके भी अधीश्वर परब्रह्मकी धारणा की, उस समय (उनके तेजको न सह सकनेके कारण) तीनों लोक काँप उठे ।।७८।।
यदैकपादेन स पार्थिवार्भकः
तस्थौ तदङ्गुष्ठनिपीडिता मही ।
ननाम तत्रार्धमिभेन्द्रधिष्ठिता
तरीव सव्येतरतः पदे पदे ॥ ७९ ॥
जब राजकुमार ध्रुव एक पैरसे खड़े हुए, तब उनके अँगूठेसे दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गयी, जैसे किसी गजराजके चढ़ जानेपर नाव पद-पदपर दायीं-बायीं ओर डगमगाने लगती है ।।७९||
तस्मिन् अभिध्यायति विश्वमात्मनो
द्वारं निरुध्यासमनन्यया धिया ।
लोका निरुच्छ्वासनिपीडिता भृशं
सलोकपालाः शरणं ययुर्हरिम् ॥ ८० ॥
ध्रुवजी अपने इन्द्रियद्वार तथा प्राणोंको रोककर अनन्यबुद्धिसे विश्वात्मा श्रीहरिका ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राणसे अभिन्नता हो जानेके कारण सभी जीवोंका श्वास-प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालोंको बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्रीहरिकी शरणमें गये ।।८०||
देवा ऊचुः –
नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधं
चराचरस्याखिलसत्त्वधाम्नः ।
विधेहि तन्नो वृजिनाद्विमोक्षं
प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम् ॥ ८१ ॥
देवताओंने कहा-भगवन्! समस्त स्थावर-जंगम जीवोंके शरीरोंका प्राण एक साथ ही रुक गया है ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले हैं, अपनी शरणमें आये हुए हमलोगोंको इस दुःखसे छुड़ाइये ।।८१।।
श्रीभगवानुवाच –
मा भैष्ट बालं तपसो दुरत्ययान्
निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम ।
यतो हि वः प्राणनिरोध आसीत्
औत्तानपादिर्मयि सङ्गतात्मा ॥ ८२ ॥
श्रीभगवानने कहा-देवताओ! तुम डरो मत। उत्तानपादके पुत्र ध्रवने अपने चित्तको मुझ विश्वात्मामें लीन कर दिया है, इस समय मेरे साथ उसकी अभेदधारणा सिद्ध हो गयी है, इसीसे उसके प्राणनिरोधसे तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने-अपने लोकोंको जाओ, मैं उस बालकको इस दुष्कर तपसे निवृत्त कर दूंगा ।।८२।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरिते अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥