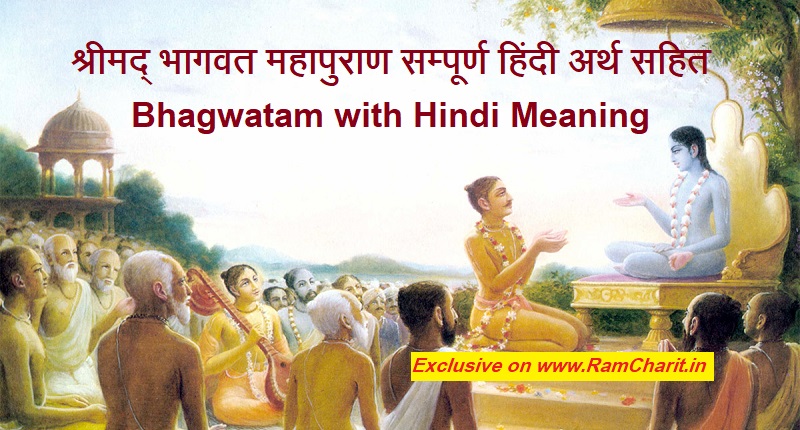श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 6 अध्याय 16
अध्यायः १६
श्रीमद्भागवत महापुराण
षष्ठः स्कन्धः – षोडशोऽध्यायः
राजपुत्रदेहवियुक्तस्य जीवात्मन उक्तिः, चित्रकेतवे नारदकर्तृकं संकर्षण
मंत्रप्रदानं तज्जपेन विद्याधरत्व प्राप्तिर्भगवतो अनन्तस्य दर्शनं च –
श्रीशुक उवाच –
अथ देवऋषी राजन् संपरेतं नृपात्मजम् ।
दर्शयित्वेति होवाच ज्ञातीनां अनुशोचताम् ॥ १ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! तदनन्तर देवर्षि नारदने मृत राजकुमारके जीवात्माको शोकाकुल स्वजनोंके सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा ।।१।।
जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते ।
सुहृदो बान्धवास्तप्ताः शुचा त्वत्कृतया भृशम् ॥ २ ॥
देवर्षि नारदने कहा-जीवात्मन्! तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता-पिता, सुहृद्सम्बन्धी तुम्हारे वियोगसे अत्यन्त शोकाकुल हो रहे हैं ।।२।।
कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः सुहृद्वृतः ।
भुङ्क्ष्व भोगान् पितृप्रत्तान् अधितिष्ठ नृपासनम् ॥ ३ ॥
इसलिये तुम अपने शरीरमें आ जाओ और शेष आयु अपने सगे-सम्बन्धियोंके साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिताके दिये हुए भोगोंको भोगो और राजसिंहासनपर बैठो ।।३।।
जीव उवाच –
कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यं पितरो मातरोऽभवन् ।
कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतिर्यङ्नृयोनिषु ॥ ४ ॥
जीवात्माने कहा-देवर्षिजी! मैं अपने कर्मोंके अनुसार देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि योनियोंमें न जाने कितने जन्मोंसे भटक रहा हूँ। उनमेंसे ये लोग किस जन्ममें मेरे माता-पिता हुए? ||४||
बन्धुज्ञात्यरिमध्यस्थ मित्रोदासीनविद्विषः ।
सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मिथः ॥ ५ ॥
विभिन्न जन्मोंमें सभी एक-दूसरेके भाई-बन्धु, नाती-गोती, शत्रु-मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं ।।५।।
यथा वस्तूनि पण्यानि हेमादीनि ततस्ततः ।
पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु ॥ ६ ॥
जैसे सुवर्ण आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ एक व्यापारीसे दूसरेके पास जाती-आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न-भिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है ।।६।।
नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु ।
यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि ॥ ७ ॥
इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि मनुष्योंकी अपेक्षा अधिक दिन ठहरनेवाले सुवर्ण आदि पदार्थोंका सम्बन्ध भी मनुष्योंके साथ स्थायी नहीं, क्षणिक ही होता है; और जबतक जिसका जिस वस्तुसे सम्बन्ध रहता है, तभीतक उसकी उस वस्तुसे ममता भी रहती है ।।७।।
एवं योनिगतो जीवः स नित्यो निरहङ्कृतः ।
यावद् यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत् ॥ ८ ॥
जीव नित्य और अहंकाररहित है। वह गर्भमें आकर जबतक जिस शरीरमें रहता है, तभीतक उस शरीरको अपना समझता है ।।८।।
एष नित्योऽव्ययः सूक्ष्म एष सर्वाश्रयः स्वदृक् ।
आत्ममायागुणैर्विश्वं आत्मानं सृजते प्रभुः ॥ ९ ॥
यह जीव नित्य अविनाशी, सूक्ष्म (जन्मादिरहित), सबका आश्रय और स्वयंप्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म-मृत्यु आदि कुछ भी नहीं हैं। फिर भी यह ईश्वररूप होनेके कारण अपनी मायाके गुणोंसे ही अपने-आपको विश्वके रूपमें प्रकट कर देता है ।।९।।
न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चित् नाप्रियः स्वः परोऽपि वा ।
एकः सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः ॥ १० ॥
इसका न तो कोई अत्यन्त प्रिय है और न अप्रिय, न अपना और न पराया। क्योंकि गुण-दोष (हित-अहित) करनेवाले मित्र-शत्रु आदिकी भिन्न-भिन्न बुद्धि-वृत्तियोंका यह अकेला ही साक्षी है; वास्तवमें यह अद्वितीय है ||१०||
नादत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् ।
उदासीनवदासीनः परावरदृगीश्वरः ॥ ११ ॥
यह आत्मा कार्य-कारणका साक्षी और स्वतन्त्र है। इसलिये यह शरीर आदिके गुण-दोष अथवा कर्मफलको ग्रहण नहीं करता, सदा उदासीनभावसे स्थित रहता है ।।११।।
श्रीशुक उवाच –
इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा ।
विस्मिता मुमुचुः शोकं छित्त्वात्म स्नेहश्रृङ्खलाम् ॥ १२ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—वह जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगेसम्बन्धी उसकी बात सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए। उनका स्नेह-बन्धन कट गया और उसके मरनेका शोक भी जाता रहा ।।१२।।
निर्हृत्य ज्ञातयो ज्ञातेः देहं कृत्वोचिताः क्रियाः ।
तत्यजुर्दुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदम् ॥ १३ ॥
इसके बाद जातिवालोंने बालककी मत देहको ले जाकर तत्कालोचित संस्कार और औदैहिक क्रियाएँ पूर्ण की और उस दुस्त्यज स्नेहको छोड़ दिया, जिसके कारण शोक, मोह, भय और दुःखकी प्राप्ति होती है ।।१३।।
बालघ्न्यो व्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः ।
बालहत्याव्रतं चेरुः ब्राह्मणैः यन्निरूपितम् ।
यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम् ॥ १४ ॥
परीक्षित्! जिन रानियोंने बच्चेको विष दिया था, वे बालहत्याके कारण श्रीहीन हो गयी थीं और लज्जाके मारे आँखतक नहीं उठा सकती थीं। उन्होंने अंगिरा ऋषिके उपदेशको याद करके (मात्सर्यहीन हो) यमुनाजीके तटपर ब्राह्मणोंके आदेशानुसार बालहत्याका प्रायश्चित्त किया ।।१४।।
स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुर्द्विजोक्तिभिः ।
गृहान्धकूपान् निष्क्रान्तः सरःपङ्कादिव द्विपः ॥ १५ ॥
परीक्षित! इस प्रकार अंगिरा और नारदजीके उपदेशसे विवेकबुद्धि जाग्रत हो जानेके कारण राजा चित्रकेतु घर-गृहस्थीके अँधेरे कुएँसे उसी प्रकार बाहर निकल पड़े, जैसे कोई हाथी तालाबके कीचड़से निकल आये ||१५||
कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः ।
मौनेन संयतप्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत ॥ १६ ॥
उन्होंने यमुनाजीमें विधिपूर्वक स्नान करके तर्पण आदि धार्मिक क्रियाएँ कीं। तदनन्तर संयतेन्द्रिय और मौन होकर उन्होंने देवर्षि नारद और महर्षि अंगिराके चरणोंकी वन्दना की ।।१६।।
अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने ।
भगवान् नारदः प्रीतो विद्यामेतामुवाच ह ॥ १७ ॥
भगवान् नारदने देखा कि चित्रकेतु जितेन्द्रिय, भगवद्भक्त और शरणागत हैं। अतः उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें इस विद्याका उपदेश किया ।।१७।।
ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ।
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कर्षणाय च ॥ १८ ॥
(देवर्षि नारदने यों उपदेश किया—) ‘ॐकारस्वरूप भगवन्! आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षणके रूपमें क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकारके अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यहरूपका बार-बार नमस्कारपूर्वक ध्यान करता हूँ ।।१८।।
नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये ।
आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टये ॥ १९ ॥
आप विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानन्दमयी है। आप अपने स्वरूपभूत आनन्दमें ही मग्न
और परम शान्त हैं। द्वैतदृष्टि आपको छूतक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।।१९।।
आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्यूर्मये नमः ।
हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥ २० ॥
अपने स्वरूपभूत आनन्दकी अनुभूतिसे ही आपने मायाजनित राग-द्वेष आदि दोषोंका तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी समस्त इन्द्रियोंके प्रेरक, परम महान् और विराट्स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।।२०।।
वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह ।
अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥ २१ ॥
मनसहित वाणी आपतक न पहँचकर बीचसे ही लौट आती है। उसके उपरत हो जानेपर जो अद्वितीय, नाम-रूपरहित, चेतनमात्र और कार्य-कारणसे परेकी वस्तु रह जाती है वह हमारी रक्षा करे ।।२१।।
यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते ।
मृण्मयेष्विव मृज्जातिः तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥ २२ ॥
यह कार्य-कारणरूप जगत् जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है तथा जो मिट्टीकी वस्तुओंमें व्याप्त मृत्तिकाके समान सबमें ओत-प्रोत हैं-उन परब्रह्मस्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ ।।२२।।
यन्न स्पृशन्ति न विदुः मनोबुद्धीन्द्रियासवः ।
अन्तर्बहिश्च विततं व्योमवत् तन्नतोऽस्म्यहम् ॥ २३ ॥
यद्यपि आप आकाशके समान बाहरभीतर एकरस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियाँ अपनी ज्ञानशक्तिसे नहीं जान सकतीं और प्राण तथा कर्मेन्द्रियाँ अपनी क्रियारूप शक्तिसे स्पर्श भी नहीं कर सकतीं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ||२३||
देहेन्द्रियप्राणमनोधियोऽमी
यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु ।
नैवान्यदा लौहमिवाप्रतप्तं
स्थानेषु तद्द्रष्ट्रपदेशमेति ॥ २४ ॥
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जाग्रत् तथा स्वप्न अवस्थाओंमें आपके चैतन्यांशसे युक्त होकर ही अपना-अपना काम करते हैं तथा सुषुप्ति और मूर्छाकी अवस्थाओंमें आपके चैतन्यांशसे युक्त न होनेके कारण अपना-अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्निसे तप्त होनेपर जला सकता है, अन्यथा नहीं। जिसे ‘द्रष्टा’ कहते हैं, वह भी आपका ही एक नाम है; जाग्रत् आदि अवस्थाओंमें आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तवमें आपसे पृथक् उनका कोई अस्तित्व नहीं है ।।२४।।
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय
महाविभूतिपतये सकलसात्वत परिवृढनिकर
करकमल कुड्मलोपलालित
चरणारविन्दयुगल परमपरमेष्ठिन् नमस्ते ॥ २५ ॥
ॐकारस्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान् महापुरुषको नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तोंका समदाय अपने करकमलोंकी कलियोंसे आपके युगल चरणकमलोंकी सेवामें संलग्न रहता है। प्रभो! आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ’ ||२५||
श्रीशुक उवाच –
भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः ।
ययावङ्गिरसा साकं धाम स्वायम्भुवं प्रभो ॥ २६ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश करके महर्षि अंगिराके साथ ब्रह्मलोकको चले गये ।।२६।।
चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषिताम् ।
धारयामास सप्ताहं अब्भक्षः सुसमाहितः ॥ २७ ॥
राजा चित्रकेतुने देवर्षि नारदके द्वारा उपदिष्ट विद्याका उनके आज्ञानुसार सात दिनतक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रताके साथ अनुष्ठान किया ।।२७।।
ततः स सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया ।
विद्याधराधिपत्यं च लेभेऽप्रतिहतं नृप ॥ २८ ॥
तदनन्तर उस विद्याके अनुष्ठानसे सात रातके पश्चात् राजा चित्रकेतुको विद्याधरोंका अखण्ड आधिपत्य प्राप्त हुआ ||२८||
ततः कतिपयाहोभिः विद्ययेद्धमनोगतिः ।
जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम् ॥ २९ ॥
इसके बाद कुछ ही दिनोंमें इस विद्याके प्रभावसे उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवाधिदेव भगवान् शेषजीके चरणोंके समीप पहुँच गये ।।२९।।
मृणालगौरं शितिवाससं स्फुरत्
किरीटकेयूरकटित्रकङ्कणम् ।
प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनं वृतं
ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलैः प्रभुम् ॥ ३० ॥
उन्होंने देखा कि भगवान् शेषजी सिद्धेश्वरोंके मण्डलमें विराजमान हैं। उनका शरीर कमलनालके समान गौरवर्ण है। उसपर नीले रंगका वस्त्र फहरा रहा है। सिरपर किरीट, बाँहोंमें बाजूबंद, कमरमें करधनी और कलाईमें कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रतनारे हैं और मुखपर प्रसन्नता छा रही है ||३०||
तद्दर्शनध्वस्तसमस्तकिल्बिषः
स्वस्थामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः ।
प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः
प्रहृष्टरोमानमदादिपुरुषम् ॥ ३१ ॥
भगवान् शेषका दर्शन करते ही राजर्षि चित्रकेतुके सारे पाप नष्ट हो गये। उनका अन्तःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदयमें भक्तिभावकी बाढ़ आ गयी। नेत्रोंमें प्रेमके आँसू छलक आये। शरीरका एक-एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थितिमें आदिपुरुष भगवान् शेषको नमस्कार किया ।।३१।।
स उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं
प्रेमाश्रुलेशैरुपमेहयन्मुहुः ।
प्रेमोपरुद्धाखिलवर्णनिर्गमो
नैवाशकत्तं प्रसमीडितुं चिरम् ॥ ३२ ॥
उनके नेत्रोंसे प्रेमके आँसू टप-टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान् शेषके चरण रखनेकी चौकी भीग गयी। प्रेमोद्रेकके कारण उनके मुँहसे एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देरतक शेषभगवान्की कुछ भी स्तुति न कर सके ||३२||
ततः समाधाय मनो मनीषया
बभाष एतत्प्रतिलब्धवागसौ ।
नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं
जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम् ॥ ३३ ॥
थोड़ी देर बाद उन्हें बोलनेकी कुछ-कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेकबुद्धिसे मनको समाहित किया और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी बाह्यवृत्तिको रोका। फिर उन जगद्गुरुकी, जिनके स्वरूपका पांचरात्र आदि भक्तिशास्त्रोंमें वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की ।।३३।।
चित्रकेतुरुवाच –
अजित जितः सममतिभिः
साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता ।
विजितास्तेऽपि च भजतां
अकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥ ३४ ॥
चित्रकेतने कहा-अजित! जितेन्द्रिय एवं समदर्शी साधओंने आपको जीत लिया है। आपने भी अपने सौन्दर्य, माधुर्य, कारुण्य आदि गुणोंसे उनको अपने वशमें कर लिया है। अहो, आप धन्य हैं! क्योंकि जो निष्कामभावसे आपका भजन करते हैं, उन्हें आप करुणापरवश होकर अपने-आपको भी दे डालते हैं ||३४।।
तव विभवः खलु भगवन्
जगदुदयस्थितिलयादीनि ।
विश्वसृजस्तेंऽशांशास्तत्र
मृषा स्पर्धन्ति पृथगभिमत्या ॥ ३५ ॥
भगवन्! जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आपके लीला-विलास हैं। विश्वनिर्माता ब्रह्मा आदि आपके अंशके भी अंश हैं। फिर भी वे पृथक्-पृथक् अपनेको जगत्कर्ता मानकर झूठमूठ एक-दूसरेसे स्पर्धा करते हैं ||३५||
परमाणुपरममहतोः
त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रयविधुरः ।
आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां
यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि ॥ ३६ ॥
नन्हे-से-नन्हे परमाणुसे लेकर बड़े-से-बड़े महत्तत्त्वपर्यन्त सम्पूर्ण वस्तुओंके आदि, अन्त और मध्यमें आप ही विराजमान हैं तथा स्वयं आप आदि, अन्त और मध्यसे रहित हैं। क्योंकि किसी भी पदार्थके आदि और अन्तमें जो वस्तु रहती है, वही मध्यमें भी रहती है ।।३६।।
क्षित्यादिभिरेष किलावृतः
सप्तभिर्दशगुणोत्तरैरण्डकोशः ।
यत्र पतत्यणुकल्पः
सहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः ॥ ३७ ॥
यह ब्रह्माण्डकोष, जो पृथ्वी आदि एक-से-एक दसगुने सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्माण्डोंके सहित आपमें एक परमाणके समान घूमता रहता और फिर भी उसे आपकी सीमाका पता नहीं है। इसलिये आप अनन्त हैं ||३७||
विषयतृषो नरपशवो
य उपासते विभूतीर्न परं त्वाम् ।
तेषामाशिष ईश तदनु
विनश्यन्ति यथा राजकुलम् ॥ ३८ ॥
जो नरपशु केवल विषयभोग ही चाहते हैं, वे आपका भजन न करके आपके विभतिस्वरूप इन्द्रादि देवताओंकी उपासना करते हैं। प्रभो! जैसे राजकुलका नाश होनेके पश्चात् उसके अनुयायियोंकी जीविका भी जाती रहती है, वैसे ही क्षुद्र उपास्यदेवोंका नाश होनेपर उनके दिये हुए भोग भी नष्ट हो जाते हैं ||३८||
कामधियस्त्वयि रचिता
न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि ।
ज्ञानात्मन्यगुणमये
गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि ॥ ३९ ॥
परमात्मन्! आप ज्ञानस्वरूप और निर्गुण हैं। इसलिये आपके प्रति की हुई सकाम भावना भी अन्यान्य कर्मोंके समान जन्म-मृत्युरूप फल देनेवाली नहीं होती, जैसे भुने हुए बीजोंसे अंकुर नहीं उगते। क्योंकि जीवको जो सुख-दुःख आदि द्वन्द्व प्राप्त होते हैं, वे सत्त्वादि गुणोंसे ही होते हैं, निर्गुणसे नहीं ||३९।।
जितमजित तदा भवता
यदाह भागवतं धर्ममनवद्यम् ।
निष्किञ्चना ये मुनय
आत्मारामा यमुपासतेऽपवर्गाय ॥ ४० ॥
हे अजित! जिस समय आपने विशुद्ध भागवतधर्मका उपदेश किया था, उसी समय आपने सबको जीत लिया। क्योंकि अपने पास कुछ भी संग्रह-परिग्रह न रखनेवाले, किसी भी वस्तुमें अहंता-ममता न करनेवाले आत्माराम सनकादि परमर्षि भी परम साम्य और मोक्ष प्राप्त करनेके लिये उसी भागवतधर्मका आश्रय लेते हैं ।।४०||
विषममतिर्न यत्र नृणां
त्वमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र ।
विषमधिया रचितो यः
स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्मबहुलः ॥ ४१ ॥
वह भागवतधर्म इतना शुद्ध है कि उसमें सकाम धर्मों के समान मनुष्योंकी वह विषमबुद्धि नहीं होती कि ‘यह मैं हूँ, यह मेरा है, यह तू है और यह तेरा है।’ इसके विपरीत जिस धर्मके मूलमें ही विषमताका बीज बो दिया जाता है, वह तो अशुद्ध, नाशवान् और अधर्मबहुल होता है ।।४१।।
कः क्षेमो निजपरयोः
कियान्वार्थः स्वपरद्रुहा धर्मेण ।
स्वद्रोहात्तव कोपः
परसम्पीडया च तथाधर्मः ॥ ४२ ॥
सकाम धर्म अपना और दूसरेका भी अहित करनेवाला है। उससे अपना या परायाकिसीका कोई भी प्रयोजन और हित सिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सकाम धर्मसे जब अनुष्ठान करनेवालेका चित्त दुखता है, तब आप रुष्ट होते हैं और जब दूसरेका चित्त दुखता है, तब वह धर्म नहीं रहता-अधर्म हो जाता है ||४२।।
न व्यभिचरति तवेक्षा
यया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः ।
स्थिरचरसत्त्वकदम्बेष्व
पृथग्धियो यमुपासते त्वार्याः ॥ ४३ ॥
भगवन्! आपने जिस दृष्टिसे भागवतधर्मका निरूपण किया है, वह कभी परमार्थसे विचलित नहीं होती। इसलिये जो संत पुरुष चर-अचर समस्त प्राणियोंमें समदृष्टि रखते हैं, वे ही उसका सेवन करते हैं ||४३||
न हि भगवन्नघटितमिदं
त्वद्दर्शनान् नृणामखिलपापक्षयः ।
यन्नाम सकृच्छ्रवणात्
पुल्कसकोऽपि विमुच्यते संसारात् ॥ ४४ ॥
भगवन्! आपके दर्शनमात्रसे ही मनुष्योंके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, यह कोई असम्भव बात नहीं है; क्योंकि आपका नाम एक बार सुननेसे ही नीच चाण्डाल भी संसारसे मुक्त हो जाता है ||४४||
अथ भगवन् वयमधुना
त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः ।
सुरऋषिणा यदुदितं
तावकेन कथमन्यथा भवति ॥ ४५ ॥
भगवन्! इस समय आपके दर्शनमात्रसे ही मेरे अन्तःकरणका सारा मल धुल गया है, सो ठीक ही है। क्योंकि आपके अनन्यप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने जो कुछ कहा है, वह मिथ्या कैसे हो सकता है ।।४५।।
विदितमनन्त समस्तं
तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम् ।
विज्ञाप्यं परमगुरोः
कियदिव सवितुरिव खद्योतैः ॥ ४६ ॥
हे अनन्त! आप सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हैं। अतएव संसारमें प्राणी जो कुछ करते हैं, वह सब आप जानते ही रहते हैं। इसलिये जैसे जगन सूर्यको प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही परमगुरु आपसे मैं क्या निवेदन करूँ ||४६||
नमस्तुभ्यं भगवते
सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय ।
दुरवसितात्मगतये
कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥ ४७ ॥
भगवन्! आपकी ही अध्यक्षतामें सारे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं। कुयोगीजन भेददष्टिके कारण आपका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाते। आपका स्वरूप वास्तवमें अत्यन्त शुद्ध है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ।।४७।।
यं वै श्वसन्तमनु विश्वसृजः श्वसन्ति
यं चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति ।
भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि
तस्मै नमो भगवतेऽस्तु सहस्रमूर्ध्ने ॥ ४८ ॥
आपकी चेष्टासे शक्ति प्राप्त करके ही ब्रह्मा आदि लोकपालगण चेष्टा करने में समर्थ होते हैं। आपकी दृष्टिसे जीवित होकर ही ज्ञानेन्द्रियाँ अपनेअपने विषयोंको ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। यह भूमण्डल आपके सिरपर सरसोंके दानेके समान जान पड़ता है। मैं आप सहस्रशीर्षा भगवान्को बार-बार नमस्कार करता हूँ ।।४८।।
श्रीशुक उवाच –
संस्तुतो भगवान् एवं अनन्तस्तमभाषत ।
विद्याधरपतिं प्रीतः चित्रकेतुं कुरूद्वह ॥ ४९ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! जब विद्याधरोंके अधिपति चित्रकेतुने अनन्तभगवान्की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा ।।४९।।
श्रीभगवान् उवाच –
यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम् ।
संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे ॥ ५० ॥
श्रीभगवान्ने कहा—चित्रकेतो! देवर्षि नारद और महर्षि अंगिराने तुम्हें मेरे सम्बन्धमें जिस विद्याका उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शनसे तुम भलीभाँति सिद्ध हो चुके हो ||५०||
अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः ।
शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनू ॥ ५१ ॥
मैं ही समस्त प्राणियोंके रूपमें हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालनकर्ता भी हूँ। शब्दब्रह्म (वेद) और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन रूप हैं ||५१||
लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् ।
उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम् ॥ ५२ ॥
आत्मा कार्यकारणात्मक जगत्में व्याप्त है और कार्य-कारणात्मक जगत् आत्मामें स्थित है तथा इन दोनोंमें मैं अधिष्ठानरूपसे व्याप्त हूँ और मुझमें ये दोनों कल्पित हैं ||५२||
यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि ।
आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः ॥ ५३ ॥
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः ।
मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् ॥ ५४ ॥
जैसे स्वप्नमें सोया हुआ पुरुष स्वप्नान्तर होनेपर सम्पूर्ण जगत्को अपने में ही देखता है और स्वप्नान्तर टूट जानेपर स्वप्नमें ही जागता है तथा अपनेको संसारके एक कोनेमें स्थित देखता है, परन्तु वास्तवमें वह भी स्वप्न ही है, वैसे ही जीवकी जाग्रत् आदि अवस्थाएँ परमेश्वरकी ही माया हैं—यों जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्माका ही स्मरण करना चाहिये ।।५३-५४||
येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा ।
सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम् ॥ ५५ ॥
सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ; उसे तुम अपनी आत्मा समझो ||५५।।
उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः ।
अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम् ॥ ५६ ॥
पुरुष निद्रा और जागति–इन दोनों अवस्थाओंका अनुभव करनेवाला है। वह उन अवस्थाओंमें अनुगत होनेपर भी वास्तवमें उनसे पृथक् है। वह सब अवस्थाओंमें रहनेवाला अखण्ड एकरस ज्ञान ही ब्रह्म है, वही परब्रह्म है ।।५६।।
यदेतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ।
ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृतेर्मृतिः ॥ ५७ ॥
जब जीव मेरे स्वरूपको भूल जाता है, तब वह अपनेको अलग मान बैठता है; इसीसे उसे संसारके चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म-पर-जन्म तथा मृत्यु-पर-मृत्यु
प्राप्त होती है ।।५७।।
लब्ध्वेह मानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् ।
आत्मानं यो न बुद्ध्येत न क्वचिन् शममाप्नुयात् ॥ ५८ ॥
यह मनुष्ययोनि ज्ञान और विज्ञानका मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी अपने आत्मस्वरूप परमात्माको नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनिमें शान्ति नहीं मिल सकती ।।५८।।
स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् ।
अभयं चाप्यनीहायां सङ्कल्पाद् विरमेत्कविः ॥ ५९ ॥
राजन्! सांसारिक सुखके लिये जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनमें श्रम है, क्लेश है और जिस परम सुखके उद्देश्यसे वे की जाती हैं, उसके ठीक विपरीत परम दुःख देती हैं; किन्तु कर्मोंसे निवृत्त हो जानेमें किसी प्रकारका भय नहीं है—यह सोचकर बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि किसी प्रकारके कर्म अथवा उनके फलोंका संकल्प न करे ।।५९।।
सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पती क्रियाः ।
ततोऽनिवृत्तिः अप्राप्तिः दुखस्य च सुखस्य च ॥ ६० ॥
जगत्के सभी स्त्री-पुरुष इसलिये कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दःखोंसे पिण्ड छटे; परन्त उन कर्मोंसे न तो उनका दुःख दूर होता है और न उन्हें सुखकी ही प्राप्ति होती है ।।६०।।
एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम् ।
आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम् ॥ ६१ ॥
जो मनुष्य अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान् मानकर कर्मके पचड़ोंमें पड़े हुए हैं, उनको विपरीत फल मिलता है—यह बात समझ लेनी चाहिये; साथ ही यह भी जान लेना चाहिये कि आत्माका स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है, जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति-इन तीनों अवस्थाओं तथा इनके अभिमानियोंसे विलक्षण है ।।६१।।
दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिः निर्मुक्तः स्वेन तेजसा ।
ज्ञानविज्ञानसन्तृप्तो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् ॥ ६२ ॥
यह जानकर इस लोकमें देखे और परलोकके सुने हुए विषय-भोगोंसे विवेकबुद्धिके द्वारा अपना पिण्ड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञानमें ही सन्तुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाय ।।६२।।
एतावानेव मनुजैः योगनैपुण्यबुद्धिभिः ।
स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम् ॥ ६३ ॥
जो लोग योगमार्गका तत्त्व समझने में निपुण हैं, उनको भलीभाँति समझ लेना चाहिये कि जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्माकी एकताका अनुभव कर ले ।।६३।।
त्वमेतच्छ्रद्धया राजन् अप्रमत्तो वचो मम ।
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिध्यसि ॥ ६४ ॥
राजन्! यदि तुम मेरे इस उपदेशको सावधान होकर श्रद्धाभावसे धारण करोगे तो ज्ञान एवं विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही सिद्ध हो जाओगे ।।६४।।
श्रीशुक उवाच –
आश्वास्य भगवानित्थं चित्रकेतुं जगद्गुरुः ।
पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरिः ॥ ६५ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-राजन्! जगद्गुरु विश्वात्मा भगवान् श्रीहरि चित्रकेतुको इस प्रकार समझा-बुझाकर उनके सामने ही वहाँसे अन्तर्धान हो गये ।।६५।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
षष्ठस्कन्धे चित्रकेतोः परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥