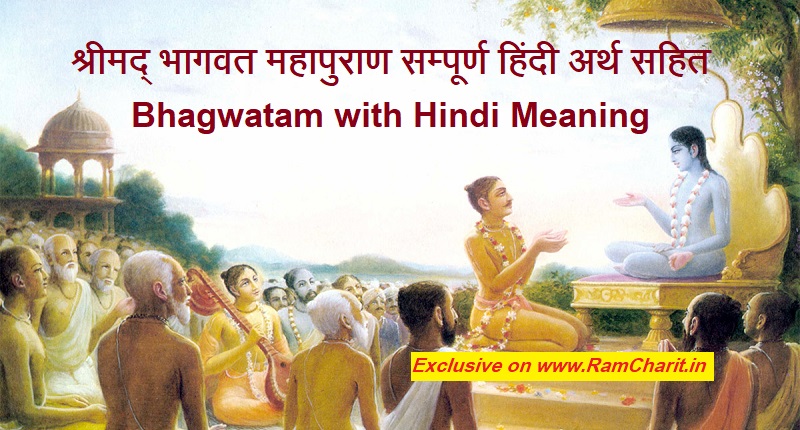श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 7 अध्याय 11
अध्यायः ११
श्रीमद्भागवत महापुराण
सप्तमः स्कंधः – एकादशोऽध्यायः
नृणां सनातनो धर्मः, वर्णधर्माः, स्त्रीधर्माश्च –
श्रीशुक उवाच –
श्रुत्वेहितं साधु सभासभाजितं
महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः ।
युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदा युतः
पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयम्भुवः ॥ १ ॥
। श्रीशकदेवजी कहते हैं-भगवन्मय प्रह्लादजीके साधसमाजमें सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संतशिरोमणि युधिष्ठिरको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने नारदजीसे और भी पूछा ।।१।।
युधिष्ठिर उवाच –
(अनुष्टुप्)
भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनम् ।
वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम् ॥ २ ॥
युधिष्ठिरजीने कहा-भगवन्! अब मैं वर्ण और आश्रमोंके सदाचारके साथ मनुष्योंके सनातनधर्मका श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्मसे ही मनुष्यको ज्ञान, भगवत्प्रेम और साक्षात् परम पुरुष भगवान्की प्राप्ति होती है ।।२।।
भवान् प्रजापतेः साक्षात् आत्मजः परमेष्ठिनः ।
सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तपोयोगसमाधिभिः ॥ ३ ॥
आप स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र हैं और नारदजी! आपकी तपस्या, योग एवं समाधिके कारण वे अपने दूसरे पुत्रोंकी अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं ||३||
नारायणपरा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः ।
करुणाः साधवः शान्ताः त्वद्विधा न तथापरे ॥ ४ ॥
आपके समान नारायण-परायण, दयालु, सदाचारी और शान्त ब्राह्मण धर्मके गुप्त-से-गुप्त रहस्यको जैसा यथार्थरूपसे जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते ।।४।।
नारद उवाच –
नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धर्महेतवे ।
वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायणमुखात् श्रुतम् ॥ ५ ॥
योऽवतीर्यात्मनोंऽशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः ।
लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥ ६ ॥
नारदजीने कहा-युधिष्ठिर! अजन्मा भगवान् ही समस्त धर्मोंके मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत्के कल्याणके लिये धर्म और दक्षपुत्री मूर्तिके द्वारा अपने अंशसे अवतीर्ण होकर बदरिकाश्रममें तपस्या कर रहे हैं। उन नारायणभगवान्को नमस्कार करके उन्हींके मुखसे सुने हुए सनातनधर्मका मैं वर्णन करता हूँ ।।५-६।।
धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिः ।
स्मृतं च तद्विदां राजन् येन चात्मा प्रसीदति ॥ ७ ॥
युधिष्ठिर! सर्ववेदस्वरूप भगवान् श्रीहरि, उनका तत्त्व जाननेवाले महर्षियोंकी स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्मप्रसादकी उपलब्धि हो, वह कर्म धर्मके मूल हैं ||७||
सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः ।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥ ८ ॥
सन्तोषः समदृक् सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः ।
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनं आत्मविमर्शनम् ॥ ९ ॥
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः ।
तेष्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव ॥ १० ॥
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः ।
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्म समर्पणम् ॥ ११ ॥
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः ।
त्रिंशत् लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति ॥ १२ ॥
यधिष्ठिर! धर्मके ये तीस लक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं—सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित-अनुचितका विचार, मनका संयम, इन्द्रियोंका संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्तोष, समदर्शी महात्माओंकी सेवा, धीरे-धीरे सांसारिक भोगोंकी चेष्टासे निवृत्ति, मनुष्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उलटा ही होता है-ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंको अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नामगुण-लीला आदिका श्रवण, कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार; उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है। इसके पालनसे सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं ।।८-१२।।
संस्कारा यदविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगाद यम् ।
इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम् ।
जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः ॥ १३ ॥
धर्मराज! जिनके वंशमें अखण्डरूपसे संस्कार होते आये हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने संस्कारके योग्य स्वीकार किया है, उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्मसे शुद्ध द्विजोंके लिये यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोंके विशेष कर्मोंका विधान है ।।१३।।
विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्याप्रतिग्रहः ।
राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तुः अविप्राद् वा करादिभिः ॥ १४ ॥
अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना–ये छः कर्म ब्राह्मणके हैं। क्षत्रियको दान नहीं लेना चाहिये। प्रजाकी रक्षा करनेवाले क्षत्रियका जीवननिर्वाह ब्राह्मणके सिवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दण्ड (जुर्माना) आदिके द्वारा होता है ।।१४।।
वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः ।
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् ॥ १५ ॥
वैश्यको सर्वदा ब्राह्मणवंशका अनुयायी रहकर गोरक्षा, कृषि एवं व्यापारके द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिये। शूद्रका धर्म है द्विजातियोंकी सेवा। उसकी जीविकाका निर्वाह उसका स्वामी करता है ।।१५।।
वार्ता विचित्रा शालीन यायावरशिलोञ्छनम् ।
विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा ॥ १६ ॥
ब्राह्मणके जीवन-निर्वाहके साधन चार प्रकारके हैं—वार्ता, शालीन,२ यायावर३ और शिलोञ्छन। इनमेंसे पीछे-पीछेकी वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं ||१६||
जघन्यो नोत्तमां वृत्तिं अनापदि भजेन्नरः ।
ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ॥ १७ ॥
निम्नवर्णका पुरुष बिना आपत्तिकालके उत्तम वर्णकी वृत्तियोंका अवलम्बन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मणकी शेष पाँचों वृत्तियोंका अवलम्बन ले सकता है। आपत्तिकालमें सभी सब वृत्तियोंको स्वीकार कर सकते हैं ।।१७।।
ऋतां ऋताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा ।
सत्यानृताभ्यां जीवेत न श्ववृत्त्या कदाचन ॥ १८ ॥
ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत और सत्यानृत–इनमेंसे किसी भी वृत्तिका आश्रय ले, परन्तु श्वानवृत्तिका अवलम्बन कभी न करे ||१८||
ऋतमुञ्छशिलं प्रोक्तं अमृतं यद् अयाचितम् ।
मृतं तु नित्ययांच्या स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतम् ॥ १९ ॥
बाजारमें पड़े हुए अन्न (उञ्छ) तथा खेतोंमें पड़े हुए अन्न (शिल)-को बीनकर ‘शिलोञ्छ’ वृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना ‘ऋत’ है। बिना माँगे जो कुछ मिल जाय, उसी अयाचित (शालीन) वृत्तिके द्वारा जीवन-निर्वाह करना ‘अमत’ है। नित्य माँगकर लाना अर्थात् ‘यायावर’ वृत्तिके द्वारा जीवन-यापन करना ‘मृत’ है। कृषि आदिके द्वारा ‘वार्ता’ वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करना ‘प्रमृत’ है ।।१९।।
सत्यानृतं च वाणिज्यं श्ववृत्तिर्नीचसेवनम् ।
वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम् ।
सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः ॥ २० ॥
वाणिज्य ‘सत्यानृत’ है और निम्नवर्णकी सेवा करना ‘श्वानवृत्ति’ है। ब्राह्मण और क्षत्रियको इस अन्तिम निन्दित वृत्तिका कभी आश्रय नहीं लेना चाहिये। क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय (राजा) सर्वदेवमय है ।।२०।।
शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम् ।
ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम् ॥ २१ ॥
शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत्परायणता और सत्य–ये ब्राह्मणके लक्षण हैं ।।२१।।
शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजः त्याग आत्मजयः क्षमा ।
ब्रह्मण्यता प्रसादश्च सत्यं च क्षत्रलक्षणम् ॥ २२ ॥
युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजाको रक्षा करना-ये क्षत्रियके लक्षण हैं ।।२२।।
देवगुर्वच्युते भक्तिः त्रिवर्गपरिपोषणम् ।
आस्तिक्यं उद्यमो नित्यं नैपुण्यं वैश्यलक्षणम् ॥ २३ ॥
देवता, गुरु और भगवान्के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम-इन तीनों पुरुषार्थोंकी रक्षा करना; आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता-ये वैश्यके लक्षण हैं ||२३||
शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेवा स्वामिन्यमायया ।
अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्र रक्षणम् ॥ २४ ॥
उच्च वर्गों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामीकी निष्कपट सेवा, वैदिक मन्त्रोंसे रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ, ब्राह्मणोंकी रक्षा करना—ये शूद्रके लक्षण हैं ।।२४।।
स्त्रीणां च पतिदेवानां तत् शुश्रूषानुकूलता ।
तद्बन्धुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम् ॥ २५ ॥
पतिकी सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पतिके सम्बन्धियोंको प्रसन्न रखना और सर्वदा पतिके नियमोंकी रक्षा करना—ये पतिको ही ईश्वर माननेवाली पतिव्रता स्त्रियोंके धर्म हैं ||२५||
सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डनवर्तनैः ।
स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥ २६ ॥
साध्वी स्त्रीको चाहिये कि झाड़ने-बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदिसे घरको
और मनोहर वस्त्राभूषणोंसे अपने शरीरको अलंकृत रखे। सामग्रियोंको साफ-सुथरी रखे ।।२६।।
कामैरुच्चावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च ।
वाक्यैः सत्यैः प्रियैः प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिम् ॥ २७ ॥
अपने पतिदेवकी छोटी-बड़ी इच्छाओंको समयके अनुसार पूर्ण करे। विनय, इन्द्रिय-संयम, सत्य एवं प्रिय वचनोंसे प्रेमपूर्वक पतिदेवकी सेवा करे ||२७||
सन्तुष्टालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् ।
अप्रमत्ता शुचिः स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् ॥ २८ ॥
जो कुछ मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे; किसी भी वस्तुके लिये ललचावे नहीं। सभी कार्यों में चतर एवं धर्मज्ञ हो। सत्य और प्रिय बोले। अपने कर्तव्यमें सावधान रहे। पवित्रता और प्रेमसे परिपूर्ण रहकर, यदि पति पतित न हो तो, उसका सहवास करे ।।२८।।
या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्परा ।
हर्यात्मना हरेर्लोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥ २९ ॥
जो लक्ष्मीजीके समान पतिपरायणा होकर अपने पतिकी उसे साक्षात् भगवान्का स्वरूप समझकर सेवा करती है, उसके पतिदेव वैकुण्ठलोकमें भगवत्सारूप्यको प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मीजीके समान उनके साथ आनन्दित होती है ।।२९।।
वृत्तिः सङ्करजातीनां तत्तत्कुलकृता भवेत् ।
अचौराणां अपापानां अन्त्यजान्तेऽवसायिनाम् ॥ ३० ॥
युधिष्ठिर! जो चोरी तथा अन्यान्य पाप-कर्म नहीं करते-उन अन्त्यज तथा चाण्डाल आदि अन्तेवसायी वर्णसंकर जातियोंकी वृत्तियाँ वे ही हैं, जो कुल-परम्परासे उनके यहाँ चली आयी हैं ||३०||
प्रायः स्वभावविहितो नृणां धर्मो युगे युगे ।
वेददृग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्य चेह च शर्मकृत् ॥ ३१ ॥
वेददर्शी ऋषि-मुनियोंने युग-युगमें प्रायः मनुष्योंके स्वभावके अनुसार धर्मकी व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिये इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी है ||३१||
वृत्त्या स्वभावकृतया वर्तमानः स्वकर्मकृत् ।
हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर्निर्गुणतामियात् ॥ ३२ ॥
जो स्वाभाविक वृत्तिका आश्रय लेकर अपने स्वधर्मका पालन करता है, वह धीरे-धीरे उन स्वाभाविक कर्मोंसे भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है ।।३२।।
उप्यमानं मुहुः क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतामियात् ।
न कल्पते पुनः सूत्यै उप्तं बीजं च नश्यति ॥ ३३ ॥
एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेवया ।
विरज्येत यथा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः ॥ ३४ ॥
महाराज! जिस प्रकार बार-बार बोनेसे खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँतक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है उसी प्रकार यह चित्त, जो वासनाओंका खजाना है, विषयोंका अत्यन्त सेवन करनेसे स्वयं ही ऊब जाता है। परन्तु स्वल्प भोगोंसे ऐसा नहीं होता। जैसे एक-एक बूंद घी डालनेसे आग नहीं बुझती, परन्तु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाय तो वह बुझ जाती है ||३३-३४।।
यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम् ।
यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत् ॥ ३५ ॥
जिस पुरुषके वर्णको बतलानेवाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी उसी वर्णका समझना चाहिये ।।३५।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥