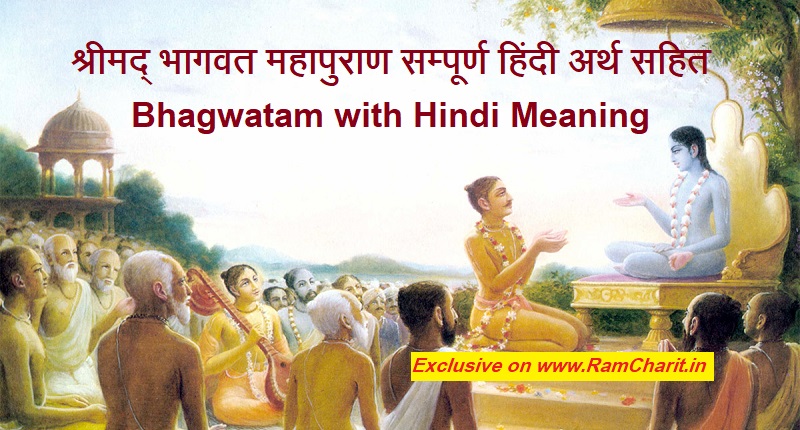श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 8 अध्याय 12
अध्यायः १२
श्रीमद्भागवत महापुराण
अष्टमः स्कन्धः – द्वादशोऽध्यायः
भगवतो मोहिनीरूपं दृष्ट्वा महादेवस्य मोहः –
श्रीबादरायणिरुवाच –
(अनुष्टुप्)
वृषध्वजो निशम्येदं योषिद् रूपेण दानवान् ।
मोहयित्वा सुरगणान् हरिः सोममपाययत् ॥ १ ॥
वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणैर्वृतः ।
सह देव्या ययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदनः ॥ २ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! जब भगवान् शंकरने यह सुना कि श्रीहरिने स्त्रीका रूप धारण करके असुरोंको मोहित कर लिया और देवताओंको अमृत पिला दिया, तब वे सतीदेवीके साथ बैलपर सवार हो समस्त भूतगणोंको लेकर वहाँ गये, जहाँ भगवान् मधुसूदन निवास करते हैं ||१-२।।
सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः ।
सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्हरिम् ॥ ३ ॥
भगवान श्रीहरिने बडे प्रेमसे गौरी-शंकरभगवानका स्वागत-सत्कार किया। वे भी सुखसे बैठकर भगवान्का सम्मान करके मुसकराते हुए बोले ।।३।।
श्रीमहादेव उवाच –
देवदेव जगद्व्यापिन् जगदीश जगन्मय ।
सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥ ४ ॥
श्रीमहादेवजीने कहा-समस्त देवोंके आराध्यदेव! आप विश्वव्यापी, जगदीश्वर एवं जगत्स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल कारण, ईश्वर और आत्मा भी आप ही हैं ।।४।।
आद्यन्तौ अस्य यन्मध्यं इदं अन्यदहं बहिः ।
यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्सत्यं ब्रह्म चिद्भवान् ॥ ५ ॥
इस जगत्के आदि, अन्त और मध्य आपसे ही होते हैं; परन्तु आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं। आपके अविनाशी स्वरूपमें द्रष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्यका भेदभाव नहीं है। वास्तवमें आप सत्य, चिन्मात्र ब्रह्म ही हैं ।।५।।
तवैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः ।
विसृज्योभयतः संगं मुनयः समुपासते ॥ ६ ॥
कल्याणकामी महात्मालोग इस लोक और परलोक दोनोंकी आसक्ति एवं समस्त कामनाओंका परित्याग करके आपके चरणकमलोंकी ही आराधना करते हैं ।।६।।
त्वं ब्रह्म पूर्णममृतं विगुणं विशोकं
आनन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत् ।
विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानां
आत्मेश्वरश्च तदपेक्षतयानपेक्षः ॥ ७ ॥
आप अमृतस्वरूप, समस्त प्राकृत गुणोंसे रहित, शोककी छायासे भी दूर, स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म हैं। आप केवल आनन्दस्वरूप हैं। आप निर्विकार हैं। आपसे भिन्न कुछ नहीं है, परन्तु आप सबसे भिन्न हैं। आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके परम कारण हैं। आप समस्त जीवोंके शुभाशुभ कर्मका फल देनेवाले स्वामी हैं। परन्तु यह बात भी जीवोंकी अपेक्षासे ही कही जाती है; वास्तवमें आप सबकी अपेक्षासे रहित, अनपेक्ष हैं ।।७।।
एकस्त्वमेव सदसद् द्वयमद्वयं च
स्वर्णं कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः ।
अज्ञानतस्त्वयि जनैर्विहितो विकल्पो ।
यस्माद् गुणव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥ ८ ॥
स्वामिन्! कार्य और कारण, द्वैत और अद्वैत–जो कुछ है, वह सब एकमात्र आप ही हैं; ठीक वैसे ही जैसे आभूषणोंके रूपमें स्थित सुवर्ण और मूल सुवर्णमें कोई अन्तर नहीं है,दोनों एक ही वस्तु हैं। लोगोंने आपके वास्तविक स्वरूपको न जाननेके कारण आपमें नाना प्रकारके भेदभाव और विकल्पोंकी कल्पना कर रखी है। यही कारण है कि आपमें किसी प्रकारकी उपाधि न होनेपर भी गुणोंको लेकर भेदकी प्रतीति होती है ।।८।।
त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके
एके परं सदसतोः पुरुषं परेशम् ।
अन्येऽवयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां
केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम् ॥ ९ ॥
प्रभो! कोई-कोई आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको धर्म कहकर वर्णन करते हैं। इसी प्रकार कोई आपको प्रकृति और पुरुषसे परे परमेश्वर मानते हैं तो कोई विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुग्रहा—इन नौ शक्तियोंसे युक्त परम पुरुष तथा दूसरे क्लेश-कर्म आदिके बन्धनसे रहित, पूर्वजोंके भी पूर्वज, अविनाशी पुरुषविशेषके रूपमें मानते हैं ||९||
नाहं परायुरृषयो न मरीचिमुख्या
जानन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः ।
यन्मायया मुषितचेतस ईश दैत्य
मर्त्यादयः किमुत शश्वदभद्रवृत्ताः ॥ १० ॥
प्रभो! मैं, ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि-जो सत्त्वगुणकी सृष्टिके अन्तर्गत हैं-जब आपकी बनायी हुई सृष्टिका भी रहस्य नहीं जान पाते, तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त मायाने अपने वशमें कर रखा है और जो सर्वदा रजोगुणी और तमोगुणी कर्मोंमें लगे रहते हैं, वे असुर और मनुष्य आदि तो भला जानेंगे ही क्या ||१०||
स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं
भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ ।
वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं
सर्वं तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्से ॥ ११ ॥
प्रभो! आप सर्वात्मक एवं ज्ञानस्वरूप हैं। इसीलिये वायुके समान आकाशमें अदृश्य रहकर भी आप सम्पूर्ण चराचर जगत्में सदा-सर्वदा विद्यमान रहते हैं तथा इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियोंके कर्म एवं संसारके बन्धन, मोक्षसभीको जानते हैं ।।११।।
(अनुष्टुप्)
अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः ।
सोऽहं तद् द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषिद् वपुर्धृतम् ॥ १२ ॥
प्रभो! आप जब गुणोंको स्वीकार करके लीला करनेके लिये बहतसे अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। अब मैं आपके उस अवतारका भी दर्शन करना चाहता हूँ, जो आपने स्त्रीरूपमें ग्रहण किया था ।।१२।।
येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताश्चामृतं सुराः ।
तद् दिदृक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥ १३ ॥
जिससे दैत्योंको मोहित करके आपने देवताओंको अमृत पिलाया, स्वामिन्! उसीको देखनेके लिये हम सब आये हैं। हमारे मनमें उसके दर्शनका बड़ा कौतूहल है ।।१३।।
श्रीशुक उवाच –
एवं अभ्यर्थितो विष्णुः भगवान् शूलपाणिना ।
प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ॥ १४ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं जब भगवान् शंकरने विष्णुभगवान्से यह प्रार्थना की, तब वे गम्भीरभावसे हँसकर शंकरजीसे बोले ।।१४।।
श्रीभगवानुवाच –
कौतूहलाय दैत्यानां योषिद्वेषो मया कृतः ।
पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूषभाजने ॥ १५ ॥
श्रीविष्णुभगवान्ने कहा-शंकरजी! उस समय अमृतका कलश दैत्योंके हाथमें चला गया था। अतः देवताओंका काम बनानेके लिये और दैत्योंका मन एक नये कौतूहलकी ओर खींच लेनेके लिये ही मैंने वह स्त्रीरूप धारण किया था ।।१५।।
तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम ।
कामिनां बहु मन्तव्यं संकल्पप्रभवोदयम् ॥ १६ ॥
देवशिरोमणे! आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिये मैं आपको वह रूप दिखाऊँगा। परन्तु वह रूप तो कामी पुरुषोंका ही आदरणीय है, क्योंकि वह कामभावको उत्तेजित करनेवाला है ।।१६।।
श्रीशुक उवाच –
इति ब्रुवाणो भगवान् तत्रैवान्तरधीयत ।
सर्वतश्चारयन् चक्षुः भव आस्ते सहोमया ॥ १७ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं इस तरह कहते-कहते विष्णुभगवान् वहीं अन्तर्धान हो गये और भगवान् शंकर सती देवीके साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए वहीं बैठे रहे ।।१७।।
ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं
विचित्रपुष्पारुणपल्लवद्रुमे ।
विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्
दुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम् ॥ १८ ॥
इतने में ही उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुन्दर उपवन है। उसमें भाँति-भाँतिके वक्ष लग रहे हैं, जो रंग-बिरंगे फूल और लाल-लाल कोंपलोंसे भरे-पूरे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवनमें एक सुन्दरी स्त्री गेंद उछाल-उछालकर खेल रही है। वह बड़ी ही सुन्दर साड़ी पहने हुए है और उसकी कमरमें करधनीकी लड़ियाँ लटक रही हैं ||१८||
आवर्तनोद्वर्तनकम्पितस्तन
प्रकृष्टहारोरुभरैः पदे पदे ।
प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलउ
पदप्रवालं नयतीं ततस्ततः ॥ १९ ॥
गेंदके उछालने और लपककर पकड़नेसे उसके स्तन और उनपर पड़े हुए हार हिल रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था, मानो इनके भारसे उसकी पतली कमर पग-पगपर टूटते-टते बच जाती है। वह अपने लाललाल पल्लवोंके समान सुकुमार चरणोंसे बड़ी कलाके साथ ठुमुक-ठुमुक चल रही थी ।।१९।।
दिक्षु भ्रमत्कन्दुकचापलैर्भृशं
प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनाम् ।
स्वकर्णविभ्राजितकुण्डलोल्लसत्
कपोलनीलालकमण्डिताननाम् ॥ २० ॥
उछलता हुआ गेंद जब इधर-उधर छलक जाता था, तब वह लपककर उसे रोक लेती थी। इससे उसकी बडी-बडी चंचल आँखें कछ उद्विग्न-सी हो रही थीं। उसके कपोलोंपर कानोंके कुण्डलोंकी आभा जगमगा रही थी और घुघराली काली-काली अलकें उनपर लटक आती थीं, जिससे मुख और भी उल्लसित हो उठता था ।।२०।।
श्लथद् दुकूलं कबरीं च विच्युतां
सन्नह्यतीं वामकरेण वल्गुना ।
विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुकं
विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ॥ २१ ॥
जब कभी साड़ी सरक जाती और केशोंकी वेणी खुलने लगती, तब अपने अत्यन्त सुकुमार बायें हाथसे वह उन्हें सम्हाल-सँवार लिया करती। उस समय भी वह दाहिने हाथसे गेंद उछाल-उछालकर सारे जगत्को अपनी मायासे मोहित कर रही थी ।।२१।।
तां वीक्ष्य देव इति कन्दुकलीलयेषद्
व्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्टः ।
स्त्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविह्वलात्मा
नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च वेद ॥ २२ ॥
गेंदसे खेलतेखेलते उसने तनिक सलज्जभावसे मुसकराकर तिरछी नजरसे शंकरजीकी ओर देखा। बस, उनका मन हाथसे निकल गया। वे मोहिनीको निहारने और उसकी चितवनके रसमें डूबकर इतने विह्वल हो गये कि उन्हें अपने-आपकी भी सुधि न रही। फिर पास बैठी हुई सती और गणोंकी तो याद ही कैसे रहती ||२२||
तस्याः कराग्रात्स तु कन्दुको यदा
गतो विदूरं तमनुव्रजत्स्त्रियाः ।
वासः ससूत्रं लघु मारुतोऽहरद्
भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः ॥ २३ ॥
एक बार मोहिनीके हाथसे उछलकर गेंद थोड़ी दूर चला गया। वह भी उसीके पीछे दौड़ी। उसी समय शंकरजीके देखते-देखते वायुने उसकी झीनी-सी साड़ी करधनीके साथ ही उड़ा ली ||२३||
(अनुष्टुप्)
एवं तां रुचिरापाङ्गीं दर्शनीयां मनोरमाम् ।
दृष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां भवः किल ॥ २४ ॥
मोहिनीका एक-एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आँखें लग जातीं, लगी ही रहतीं। यही नहीं, मन भी वहीं रमण करने लगता। उसको इस दशामें देखकर भगवान् शंकर उसकी ओर अत्यन्त आकृष्ट हो गये। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी ।।२४।।
तयापहृतविज्ञानः तत्कृतस्मरविह्वलः ।
भवान्या अपि पश्यन्त्या गतह्रीस्तत्पदं ययौ ॥ २५ ॥
उसने शंकरजीका विवेक छीन लिया। वे उसके हाव-भावोंसे कामातुर हो गये और भवानीके सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े ||२५||
सा तं आयान्तमालोक्य विवस्त्रा व्रीडिता भृशम् ।
निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥ २६ ॥
मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी, शंकरजीको अपनी ओर आते देख बहुत लज्जित हो गयी। वह एक वृक्षसे दूसरे वृक्षकी आड़में जाकर छिप जाती और हँसने लगती। परन्तु कहीं ठहरती न थी ।।२६।।
तां अन्वगच्छद् भगवान् भवः प्रमुषितेन्द्रियः ।
कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥ २७ ॥
भगवान् शंकरकी इन्द्रियाँ अपने वशमें नहीं रहीं, वे कामवश हो गये थे; अतः हथिनीके पीछे हाथीकी तरह उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे ||२७||
सोऽनुव्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं स्त्रियम् ।
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥ २८ ॥
उन्होंने अत्यन्त वेगसे उसका पीछा करके पीछेसे उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होनेपर भी उसे दोनों भुजाओंमें भरकर हृदयसे लगा लिया ।।२८।।
सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा ।
इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीर्णशिरोरुहा ॥ २९ ॥
जैसे हाथी हथिनीका आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान् शंकरने उसका आलिंगन किया। वह इधर-उधर खिसककर छुड़ानेकी चेष्टा करने लगी, इसी छीना-झपटीमें उसके सिरके बाल बिखर गये ||२९||
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरर्षभभुजान्तरात् ।
प्राद्रवत्सा पृथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥ ३० ॥
वास्तवमें वह सुन्दरी भगवान्की रची हुई माया ही थी, इससे उसने किसी प्रकार शंकरजीके भुजपाशसे अपनेको छुड़ा लिया और बड़े वेगसे भागी ।।३०।।
तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोरद्भुतकर्मणः ।
प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेव विनिर्जितः ॥ ३१ ॥
भगवान् शंकर भी उन मोहिनीवेषधारी अद्भुतकर्मा भगवान् विष्णुके पीछे-पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो उनके शत्रु कामदेवने इस समय उनपर विजय प्राप्त कर ली है ||३१||
तस्यानुधावतो रेतः चस्कन्दामोघरेतसः ।
शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावतः ॥ ३२ ॥
कामुक हथिनीके पीछे दौड़नेवाले मदोन्मत्त हाथीके समान वे मोहिनीके पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान् शंकरका वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनीकी मायासे वह स्खलित हो गया ||३२||
यत्र यत्रापतन् मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः ।
तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्राण्यासन् महीपते ॥ ३३ ॥
भगवान् शंकरका वीर्य पृथ्वीपर जहाँ-जहाँ गिरा, वहाँ-वहाँ सोने-चाँदीकी खानें बन गयीं ।।३३।।
सरित्सरःसु शैलेषु वनेषु उपवनेषु च ।
यत्र क्व चासन् ऋषयः तत्र सन्निहितो हरः ॥ ३४ ॥
परीक्षित्! नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवनमें एवं जहाँ-जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते थे, वहाँ वहाँ मोहिनीके पीछे-पीछे भगवान शंकर गये थे ।।३४।।
स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यत् आत्मानं देवमायया ।
जडीकृतं नृपश्रेष्ठ सन्न्यवर्तत कश्मलात् ॥ ३५ ॥
परीक्षित्! वीर्यपात हो जानेके बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे, भगवान्की मायाने तो मुझे खूब छकाया! वे तुरंत उस दुःखद प्रसंगसे अलग हो गये ।।३५।।
अथ अवगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः ।
अपरिज्ञेयवीर्यस्य न मेने तदु हाद्भुतम् ॥ ३६ ॥
इसके बाद आत्मस्वरूप सर्वात्मा भगवान्की यह महिमा जानकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भला, भगवान्की शक्तियोंका पार कौन पा सकता है ।।३६।।
तमविक्लवमव्रीडं आलक्ष्य मधुसूदनः ।
उवाच परमप्रीतो बिभ्रत् स्वां पौरुषीं तनुम् ॥ ३७ ॥
भगवान्ने देखा कि भगवान् शंकरको इससे विषाद या लज्जा नहीं हुई है, तब वे पुरुषशरीर धारण करके फिर प्रकट हो गये और बड़ी प्रसन्नतासे उनसे कहने लगे ।।३७।।
श्रीभगवानुवाच –
दिष्ट्या त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठां आत्मना स्थितः ।
यन्मे स्त्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया ॥ ३८ ॥
श्रीभगवानने कहा-देवशिरोमणे! मेरी स्त्रीरूपिणी मायासे विमोहित होकर भी आप स्वयं ही अपनी निष्ठामें स्थित हो गये। यह बड़े ही आनन्दकी बात है ।।३८।।
को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदृते पुमान् ।
तान् तान् विसृजतीं भावान् दुस्तरामकृतात्मभिः ॥ ३९ ॥
मेरी माया अपार है। वह ऐसे-ऐसे हाव-भाव रचती है कि अजितेन्द्रिय पुरुष तो किसी प्रकार उससे छुटकारा पा ही नहीं सकते। भला, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है, जो एक बार मेरी मायाके फंदेमें फँसकर फिर स्वयं ही उससे निकल सके ।।३९।।
सेयं गुणमयी माया न त्वां अभिभविष्यति ।
मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥ ४० ॥
यद्यपि मेरी यह गुणमयी माया बड़ों-बड़ोंको मोहित कर देती है, फिर भी अब यह आपको कभी मोहित नहीं करेगी। क्योंकि सष्टि आदिके लिये समयपर उसे क्षोभित करनेवाला काल मैं ही हूँ, इसलिये मेरी इच्छाके विपरीत वह रजोगुण आदिकी सृष्टि नहीं कर सकती ।।४०।।
श्रीशुक उवाच –
एवं भगवता राजन् श्रीवत्सांकेन सत्कृतः ।
आमंत्र्य तं परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ ॥ ४१ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इस प्रकार भगवान् विष्णुने भगवान् शंकरका सत्कार किया। तब उनसे विदा लेकर एवं परिक्रमा करके वे अपने गणोंके साथ कैलासको चले गये ||४१||
आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान् भवः ।
शंसतां ऋषिमुख्यानां प्रीत्याचष्टाथ भारत ॥ ४२ ॥
भरतवंशशिरोमणे! भगवान शंकरने बड़े-बड़े ऋषियोंकी सभामें अपनी अर्धांगिनी सती देवीसे अपने विष्णुरूपकी अंशभूता मायामयी मोहिनीका इस प्रकार बड़े प्रेमसे वर्णन किया ।।४२।।
अयि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां
परस्य पुंसः परदेवतायाः ।
अहं कलानां ऋषभो विमुह्ये
ययावशोऽन्ये किमुतास्वतंत्राः ॥ ४३ ॥
‘देवि! तुमने परम पुरुष परमेश्वर भगवान् विष्णुकी माया देखी? देखो, यों तो मैं समस्त कलाकौशल, विद्या आदिका स्वामी और स्वतन्त्र हूँ, फिर भी उस मायासे विवश होकर मोहित हो जाता हूँ। फिर दूसरे जीव तो परतन्त्र हैं ही; अतः वे मोहित हो जायँ—इसमें कहना ही क्या है ||४३||
यं मां अपृच्छस्त्वमुपेत्य योगात्
समासहस्रान्त उपारतं वै ।
स एष साक्षात्पुरुषः पुराणो
न यत्र कालो विशते न वेदः ॥ ४४ ॥
जब मैं एक हजार वर्षकी समाधिसे उठा था, तब तुमने मेरे पास आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। वे यही साक्षात् सनातन पुरुष हैं। न तो काल ही इन्हें अपनी सीमामें बाँध सकता है और न वेद ही इनका वर्णन कर सकता है। इनका वास्तविक स्वरूप अनन्त और अनिर्वचनीय है’ ||४४।।
श्रीशुक उवाच –
इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शारंगधन्वनः ।
सिन्धोर्निर्मथने येन धृतः पृष्ठे महाचलः ॥ ४५ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-प्रिय परीक्षित्! मैंने विष्णुभगवान्की यह ऐश्वर्यपूर्ण लीला तुमको सुनायी, जिसमें समुद्रमन्थनके समय अपनी पीठपर मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान्का वर्णन है ।।४५।।
एतन्मुहुः कीर्तयतोऽनुश्रृण्वतो
न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित् ।
यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्णनं
समस्तसंसारपरिश्रमापहम् ॥ ४६ ॥
जो पुरुष बार-बार इसका कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी और कहीं निष्फल नहीं होता। क्योंकि पवित्रकीर्ति भगवानके गण और लीलाओंका गान संसारके समस्त क्लेश और परिश्रमको मिटा देनेवाला है ।।४६।।
असद् अविषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नान्
अमृतममरवर्यानाशयत् सिन्धुमथ्यम् ।
कपटयुवतिवेषो मोहयन् यः सुरारीन्
तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ॥ ४७ ॥
दुष्ट पुरुषोंको भगवान्के चरणकमलोंकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। वे तो भक्तिभावसे युक्त पुरुषको ही प्राप्त होते हैं। इसीसे उन्होंने स्त्रीका मायामय रूप धारण करके दैत्योंको मोहित किया और अपने चरणकमलोंके शरणागत देवताओंको समुद्रमन्थनसे निकले हुए अमृतका पान कराया। केवल उन्हींकी बात नहीं चाहे जो भी उनके चरणोंकी शरण ग्रहण करे, वे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं। मैं उन प्रभुके चरणकमलोंमें नमस्कार करता हूँ ।।४७।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
अष्टमस्कन्धे शंकरमोहनं द्वादशोध्याऽयः ॥ १२ ॥