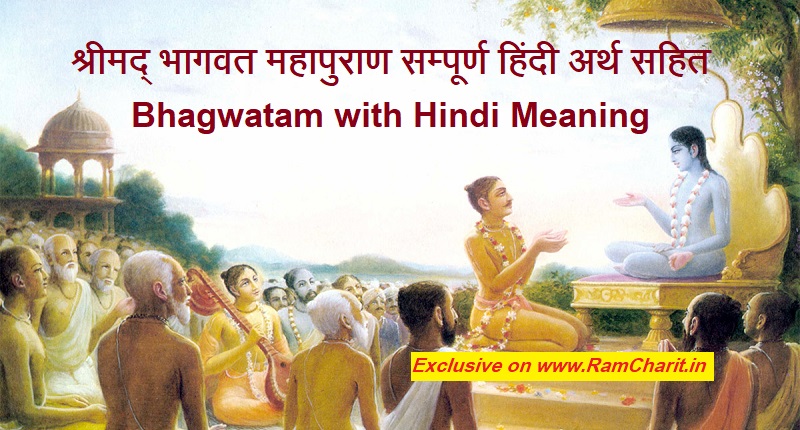श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 8 अध्याय 19
अध्यायः १९
श्रीमद्भागवत महापुराण
अष्टमः स्कन्धः – एकोनविंशोऽध्यायः
बलिवामनसंवादः, पदत्रयभूमियाचनम्, शुक्रद्वारा दाननिषेधश्च –
श्रीशुक उवाच –
(अनुष्टुप्)
इति वैरोचनेर्वाक्यं धर्मयुक्तं स सूनृतम् ।
निशम्य भगवान् प्रीन्प्रीतः प्रतिनन्द्येदमब्रवीत् ॥ १ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं राजा बलिके ये वचन धर्मभावसे भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान् वामनने बड़ी प्रसन्नतासे उनका अभिनन्दन किया और कहा ।।१।।
श्रीभगवानुवाच –
वचस्तवैतत् जनदेव सूनृतं
कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम् ।
यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये
पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः ॥ २ ॥
श्रीभगवानने कहा–राजन! आपने जो कुछ कहा, वह आपकी कुलपरम्पराके अनुरूप, धर्मभावसे परिपूर्ण, यशको बढ़ानेवाला और अत्यन्त मधुर है। क्यों न हो, परलोकहितकारी धर्मके सम्बन्धमें आप भगपुत्र शुक्राचार्यको परम प्रमाण जो मानते हैं। साथ ही अपने कुलवृद्ध पितामह परम शान्त प्रह्लादजीकी आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं ।।२।।
(अनुष्टुप्)
न ह्येतस्मिन्कुले कश्चित् निःसत्त्वः कृपणः पुमान् ।
प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये ॥ ३ ॥
आपकी वंशपरम्परामें कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा भी कोई नहीं हुआ, जिसने ब्राह्मणको कभी दान न दिया हो अथवा जो एक बार किसीको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा करके बादमें मुकर गया हो ||३||
न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः
पराङ्मुखा ये त्वमनस्विनो नृपाः ।
युष्मत्कुले यद् यशसामलेन
प्रह्राद उद्भाति यथोडुपः खे ॥ ४ ॥
दानके अवसरपर याचकोंकी याचना सुनकर और युद्धके अवसरपर शत्रुके ललकारनेपर उनकी ओरसे मुँह मोड़ लेनेवाला कायर आपके वंशमें कोई भी नहीं हुआ। क्यों न हो, आपकी कुलपरम्परामें प्रह्लाद अपने निर्मल यशसे वैसे ही शोभायमान होते हैं, जैसे आकाशमें चन्द्रमा ।।४।।
(अनुष्टुप्)
यतो जातो हिरण्याक्षः चरन्नेक इमां महीम् ।
प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ॥ ५ ॥
आपके कुलमें ही हिरण्याक्ष-जैसे वीरका जन्म हुआ था। वह वीर जब हाथमें गदा लेकर अकेला ही दिग्विजयके लिये निकला, तब सारी पृथ्वीमें घूमनेपर भी उसे अपनी जोड़का कोई वीर न मिला ||५||
यं विनिर्जित्य कृच्छ्रेण विष्णुः क्ष्मोद्धार आगतम् ।
आत्मानं जयिनं मेने तद्वीर्यं भूर्यनुस्मरन् ॥ ६ ॥
जब विष्णुभगवान् जलमेंसे पृथ्वीका उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाईसे उन्होंने उसपर विजय प्राप्त की। परन्तु उसके बहुत बाद भी उन्हें बार-बार हिरण्याक्षकी शक्ति और बलका स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेनेपर भी वे अपनेको विजयी नहीं समझते थे ||६||
निशम्य तद्वधं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा ।
हन्तुं भ्रातृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरेः ॥ ७ ॥
जब हिरण्याक्षके भाई हिरण्यकशिपुको उसके वधका वृत्तान्त मालूम हुआ, तब वह अपने भाईका वध करनेवालेको मार डालनेके लिये क्रोध करके भगवान्के निवासस्थान वैकुण्ठधाममें पहुँचा ।।७।।
तं आयान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत् ।
चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वरः ॥ ८ ॥
विष्णुभगवान् माया रचनेवालोंमें सबसे बड़े हैं और समयको खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथमें शूल लेकर कालकी भाँति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया ।।८।।
यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः प्राणभृतामिव ।
अतोऽहं अस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दृशः ॥ ९ ॥
‘जैसे संसारके प्राणियोंके पीछे मृत्यु लगी रहती हैवैसे ही मैं जहाँ-जहाँ जाऊँगा, वहीं-वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिये मैं इसके हृदयमेंप्रवेश कर जाऊँ, जिससे यह मुझे देख न सके; क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहरकी वस्तुएँ ही देखता है ||९||
एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरं
आधावतो निर्विविशेऽसुरेन्द्र ।
श्वासानिलान्तर्हितसूक्ष्मदेहः
तत्प्राणरन्ध्रेण विविग्नचेताः ॥ १० ॥
असुरशिरोमणे! जिस समय हिरण्यकशिप उनपर झपट रहा था, उसी समय ऐसा निश्चय करके डरसे काँपते हुए विष्णुभगवान्ने अपने शरीरको सूक्ष्म बना लिया और उसके प्राणोंके द्वारा नासिकामेंसे होकर हृदयमें जा बैठे ।।१०।।
स तन्निकेतं परिमृश्य
शून्यमपश्यमानः कुपितो ननाद ।
क्ष्मां द्यां दिशः खं विवरान्समुद्रान्
विष्णुं विचिन्वन् न ददर्श वीरः ॥ ११ ॥
हिरण्यकशिपुने उनके लोकको भलीभाँति छान डाला, परन्तु उनका कहीं पता न चला। इसपर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीरने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र-सब कहीं विष्णुभगवान्को ढूँढ़ा, परन्तु वे कहीं भी उसे दिखायी न दिये ।।११।।
(अनुष्टुप्)
अपश्यन् इति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत् ।
भ्रातृहा मे गतो नूनं यतो नावर्तते पुमान् ॥ १२ ॥
उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा-मैंने सारा जगत् छान डाला, परन्तु वह मिला नहीं। अवश्य ही वह भ्रातघाती उस लोकमें चला गया, जहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता ||१२||
वैरानुबन्ध एतावान् आमृत्योरिह देहिनाम् ।
अज्ञानप्रभवो मन्युः अहंमानोपबृंहितः ॥ १३ ॥
बस, अब उससे वैरभाव रखनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैर तो देहके साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोधका कारण अज्ञान है और अहंकारसे उसकी वृद्धि होती है ।।१३।।
पिता प्रह्रादपुत्रस्ते तद्विद्वान् द्विजवत्सलः ।
स्वमायुर्द्विजलिंगेभ्यो देवेभ्योऽदात् स याचितः ॥ १४ ॥
राजन्! आपके पिता प्रह्लादनन्दन विरोचन बड़े ही ब्राह्मणभक्त थे। यहाँतक कि । उनके शत्रु देवताओंने ब्राह्मणोंका वेष बनाकर उनसे उनकी आयुका दान माँगा और उन्होंने ब्राह्मणोंके छलको जानते हुए भी अपनी आयु दे डाली ||१४||
भवान् आचरितान् धर्मान् आस्थितो गृहमेधिभिः ।
ब्राह्मणैः पूर्वजैः शूरैः अन्यैश्चोद्दामकीर्तिभिः ॥ १५ ॥
आप भी उसी धर्मका आचरण करते हैं, जिसका शुक्राचार्य आदि गहस्थ ब्राह्मण, आपके पूर्वज प्रह्लाद और दूसरे यशस्वी वीरोंने पालन किया है ।।१५।।
तस्मात् त्वत्तो महीमीषद् वृणेऽहं वरदर्षभात् ।
पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम ॥ १६ ॥
दैत्येन्द्र! आप मुँहमाँगी वस्तु देनेवालोंमें श्रेष्ठ हैं। इसीसे मैं आपसे थोड़ी-सी पृथ्वी केवल अपने पैरोंसे तीन डग माँगता हूँ ||१६||
न अन्यत् ते कामये राजन् वदान्यात् जगदीश्वरात् ।
नैनः प्राप्नोति वै विद्वान् यावदर्थप्रतिग्रहः ॥ १७ ॥
माना कि आप सारे जगत्के स्वामी और बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान् पुरुषको केवल अपनी आवश्यकताके अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिये। इससे वह प्रतिग्रहजन्य पापसे बच जाता है ।।१७।।
श्रीबलिरुवाच –
अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसम्मताः ।
त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा ॥ १८ ॥
राजा बलिने कहा—ब्राह्मणकुमार! तुम्हारी बातें तो वृद्धों-जैसी हैं, परन्तु तुम्हारी बुद्धि अभी बच्चोंकी-सी ही है। अभी तुम हो भी तो बालक ही न, इसीसे अपना हानि-लाभ नहीं समझ रहे हो ।।१८।।
मां वचोभिः समाराध्य लोकानां एकमीश्वरम् ।
पदत्रयं वृणीते यो अबुद्धिमान् द्वीपदाशुषम् ॥ १९ ॥
मैं तीनों लोकोंका एकमात्र अधिपति हूँ और द्वीप-का-द्वीप दे सकता हूँ। जो मुझे अपनी वाणीसे प्रसन्न कर ले और मुझसे केवल तीन डग भूमि माँगे—वह भी क्या बुद्धिमान् कहा जा सकता है? ।।१९।।
न पुमान् मां उपव्रज्य भूयो याचितुमर्हति ।
तस्माद् वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे ॥ २० ॥
ब्रह्मचारीजी! जो एक बार कुछ माँगनेके लिये मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसीसे कुछ माँगनेकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिये। अतः अपनी जीविका चलानेके लिये तम्हें जितनी भूमिकी आवश्यकता हो, उतनी मुझसे माँग लो ।।२०।।
श्रीभगवानुवाच –
यावन्तो विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्यां अजितेन्द्रियम् ।
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप ॥ २१ ॥
श्रीभगवान्ने कहा-राजन्! संसारके सब-के-सब प्यारे विषय एक मनुष्यकी कामनाओंको भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं हैं, यदि वह अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखनेवालासन्तोषी न हो ।।२१।।
त्रिभिः क्रमैः असन्तुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते ।
नववर्षसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया ॥ २२ ॥
जो तीन पग भूमिसे सन्तोष नहीं कर लेता, उसे नौ वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाय तो भी वह सन्तुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि उसके मनमें सातों द्वीप पानेकी इच्छा बनी ही रहेगी ।।२२।।
सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वैन्यगयादयः ।
अर्थैः कामैर्गता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रुतम् ॥ २३ ॥
मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश सातों द्वीपोंके अधिपति थे; परन्तु उतने धन और भोगकी सामग्रियोंके मिलनेपर भी वे तृष्णाका पार न पा सके ।।२३।।
यदृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम् ।
नासन्तुष्टः त्रिभिर्लोकैः अजितात्मोपसादितैः ॥ २४ ॥
जो कुछ प्रारब्धसे मिल जाय, उसीसे सन्तुष्ट हो रहनेवाला पुरुष अपना जीवन सुखसे व्यतीत करता है। परन्तु अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला तीनों लोकोंका राज्य पानेपर भी दुःखी ही रहता है। क्योंकि उसके हृदयमें असन्तोषकी आग धधकती रहती है ।।२४।।
पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुः असन्तोषोऽर्थकामयोः ।
यदृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः ॥ २५ ॥
धन और भोगोंसे सन्तोष न होना ही जीवके जन्म-मृत्युके चक्करमें गिरनेका कारण है। तथा जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें सन्तोष कर लेना मुक्तिका कारण है ।।२५।।
यदृच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते ।
तत्प्रशाम्यति असन्तोषाद् अम्भसेवाशुशुक्षणिः ॥ २६ ॥
जो ब्राह्मण स्वयंप्राप्त वस्तुसे ही सन्तुष्ट हो रहता है, उसके तेजकी वृद्धि होती है। उसके असन्तोषी हो जानेपर उसका तेज वैसे ही शान्त हो जाता है जैसे जलसे अग्नि ।।२६।।
तस्मात्त्रीणि पदान्येव वृणे त्वद् वरदर्षभात् ।
एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम् ॥ २७ ॥
इसमें सन्देह नहीं कि आप मुँहमाँगी वस्तु देनेवालोंमें शिरोमणि हैं। इसलिये मैं आपसे केवल तीन पग भूमि ही माँगता हूँ। इतनेसे ही मेरा काम बन जायगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिये, जितनेकी आवश्यकता हो ।।२७।।
श्रीशुक उवाच –
इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम् ।
वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम् ॥ २८ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-भगवान्के इस प्रकार कहनेपर राजा बलि हँस पड़े। उन्होंनेकहा-‘अच्छी बात है; जितनी तुम्हारी इच्छा हो, उतनी ही ले लो।’ यों कहकर वामनभगवानको तीन पग पथ्वीका संकल्प करनेके लिये उन्होंने जलपात्र उठाया ।।२८।।
विष्णवे क्ष्मां प्रदास्यन्तं उशना असुरेश्वरम् ।
जानन् चिकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदां वरः ॥ २९ ॥
शुक्राचार्यजी सब कुछ जानते थे। उनसे भगवान्की यह लीला भी छिपी नहीं थी। उन्होंने राजा बलिको पृथ्वी देनेके लिये तैयार देखकर उनसे कहा ||२९||
श्रीशुक्र उवाच –
एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुरव्ययः ।
कश्यपाद् अदितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥ ३० ॥
शुक्राचार्यजीने कहा-विरोचनकुमार! ये स्वयं अविनाशी भगवान् विष्णु हैं। देवताओंका काम बनानेके लिये कश्यपकी पत्नी अदितिके गर्भसे अवतीर्ण हए हैं ||३०||
प्रतिश्रुतं त्वयैतस्मै यद् अनर्थं अजानता ।
न साधु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥ ३१ ॥
तुमने यह अनर्थ न जानकर कि ये मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। यह तो दैत्योंपर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है। इसे मैं ठीक नहीं समझता ||३१||
एष ते स्थानमैश्वर्यं श्रियं तेजो यशः श्रुतम् ।
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरिः ॥ ३२ ॥
स्वयं भगवान ही अपनी योगमायासे यह ब्रह्मचारी बनकर बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्वविख्यात कीर्ति-सब कुछ तुमसे छीनकर इन्द्रको दे देंगे ||३२||
त्रिभिः क्रमैः इमान् लोकान् विश्वकायः क्रमिष्यति ।
सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम् ॥ ३३ ॥
ये विश्वरूप हैं। तीन पगमें तो ये सारे लोकोंको नाप लेंगे। मूर्ख! जब तुम अपना सर्वस्व ही विष्णुको दे डालोगे, तो तुम्हारा जीवन-निर्वाह कैसे होगा ।।३३।।
क्रमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभोः ।
खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥ ३४ ॥
ये विश्वव्यापक भगवान् एक पगमें पृथ्वी और दूसरे पगमें स्वर्गको नाप लेंगे। इनके विशाल शरीरसे आकाश भर जायगा। तब इनका तीसरा पग कहाँ जायगा? ||३४।।
निष्ठां ते नरके मन्ये हि अप्रदातुः प्रतिश्रुतम् ।
प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान् ॥ ३५ ॥
तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशामें मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पानेके कारण तुम्हें नरकमें ही जाना पड़ेगा। क्योंकि तुम अपनी की हुई प्रतिज्ञाको पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ होओगे ||३५||
न तद्दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते ।
दानं यज्ञस्तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः ॥ ३६ ॥
विद्वान् पुरुष उस दानकी प्रशंसा नहीं करते, जिसके बाद जीवन-निर्वाहके लिये कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन-निर्वाह ठीक-ठीक चलता है-वही संसारमें दान, यज्ञ, तप और परोपकारके कर्म कर सकता है ।।३६।।
धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च ।
पञ्चधा विभजन् वित्तं इहामुत्र च मोदते ॥ ३७ ॥
जो मनुष्य अपने धनको पाँच भागोंमें बाँट देता है— कुछ धर्मके लिये, कुछ यशके लिये, कुछ धनकी अभिवृद्धिके लिये, कुछ भोगोंके लिये और कुछ अपने स्वजनोंके लिये—वही इस लोक और परलोक दोनोंमें ही सुख पाता है ।।३७।।
अत्रापि बह्वृचैर्गीतं शृणु मेऽसुरसत्तम ।
सत्यं ॐ इति यत्प्रोक्तं यत् नेति आहानृतं हि तत् ॥ ३८ ॥
असुरशिरोमणे! यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जानेकी चिन्ता हो, तो मैं इस विषयमें तुम्हें कुछ ऋग्वेदकी श्रुतियोंका आशय सुनाता हूँ, तुम सुनो। श्रुति कहती है—’किसीको कुछ देनेकी बात स्वीकार कर लेना सत्य है और नकार जाना अर्थात् अस्वीकार कर देना असत्य है ||३८।।
सत्यं पुष्पफलं विद्याद् आत्मवृक्षस्य गीयते ।
वृक्षेऽजीवति तन्न स्यात् अनृतं मूलमात्मनः ॥ ३९ ॥
यह शरीर एक वृक्ष है और सत्य इसका फल-फूल है। परन्तु यदि वृक्ष ही न रहे तो फल-फूल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि नकार जाना, अपनी वस्तु दसरेको न देना, दूसरे शब्दोंमें अपना संग्रह बचाये रखना—यही शरीररूप वृक्षका मूल है ||३९||
तद् यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्यति उद्वर्ततेऽचिरात् ।
एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संशयः ॥ ४० ॥
जैसे जड़ न रहनेपर वृक्ष सूखकर थोड़े ही दिनोंमें गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देनेसे अस्वीकार न किया जाय तो यह जीवन सूख जाता है—इसमें सन्देह नहीं ।।४०।।
पराग् रिक्तमपूर्णं वा अक्षरं यत् तदोमिति ।
यत्किञ्चित् ओमिति ब्रूयात् तेन रिच्येत वै पुमान् ।
भिक्षवे सर्वं ॐकुन् नालं कामेन चात्मने ॥ ४१ ॥
‘हाँ मैं दूँगा’—यह वाक्य ही धनको दूर हटा देता है। इसलिये इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात् धनसे खाली कर देनेवाला है। यही कारण है कि जो पुरुष ‘हाँ मैं दूँगा’—ऐसा कहता है, वह धनसे खाली हो जाता है। जो याचकको सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने लिये भोगकी कोई सामग्री नहीं रख सकता ।।४१।।
अथैतत्पूर्णमभ्यात्मं यच्च नेति अनृतं वचः ।
सर्वं नेति अनृतं ब्रूयात् स दुष्कीर्तिः श्वसन्मृतः ॥ ४२ ॥
इसके विपरीत ‘मैं नहीं दंगा’—यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है, वह अपने धनको सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करनेवाला है। परन्तु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिये। जो सबसे, सभी वस्तुओंके लिये नहीं करता रहता है, उसकी अपकीर्ति हो जाती है। वह तो जीवित रहनेपर भी मृतकके समान ही है ||४२||
स्त्रीषु नर्मविवाहे च वृत्त्यर्थे प्राणसंकटे ।
गोब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम् ॥ ४३ ॥
स्त्रियोंको प्रसन्न करनेके लिये, हासपरिहासमें, विवाहमें, कन्या आदिकी प्रशंसा करते समय, अपनी जीविकाकी रक्षाके लिये, प्राणसंकट उपस्थित होनेपर, गौ और ब्राह्मणके हितके लिये तथा किसीको मृत्युसे बचानेके लिये असत्य-भाषण भी उतना निन्दनीय नहीं है ।।४३।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥