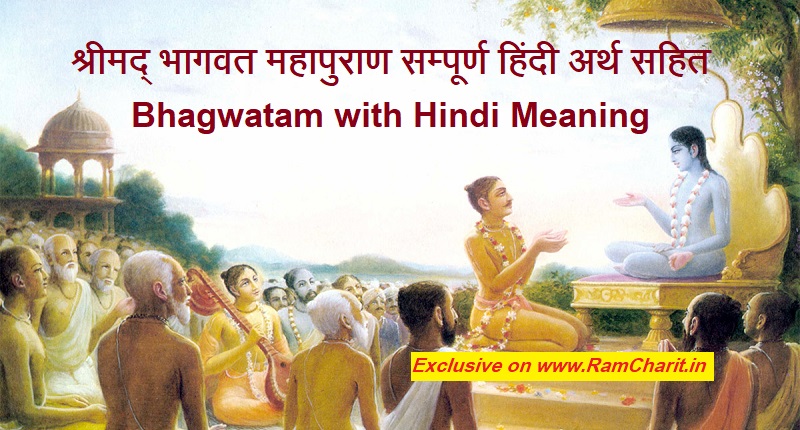श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 8 अध्याय 22
अध्यायः २२
श्रीमद्भागवत महापुराण
अष्टमः स्कन्धः – द्वाविंशोऽध्यायः
बलिवचनं ब्रह्मणो वचनं भगवकृतं बलेः प्रशसनं तस्मै वरदानं च –
श्रीशुक उवाच –
(अनुष्टुप्)
एवं विप्रकृतो राजन् बलिर्भगवतासुरः ।
भिद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः ॥ १ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! इस प्रकार भगवान्ने असुरराज बलिका बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्यसे विचलित करना चाहा। परन्तु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले ।।१।।
श्रीबलिरुवाच –
यद्युत्तमश्लोक भवान्ममेरितं
वचो व्यलीकं सुरवर्य मन्यते ।
करोम्यृतं तन्न भवेत्प्रलम्भनं
पदं तृतीयं कुरु शीर्ष्णि मे निजम् ॥ २ ॥
दैत्यराज बलिने कहा-देवताओंके आराध्यदेव! आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बातको असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है। मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखेमेंनहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिरपर रख दीजिये ।।२।।
बिभेमि नाहं निरयात् पदच्युतो
न पाशबन्धाद्व्यसनाद् दुरत्ययात् ।
नैवार्थकृच्छ्राद्भवतो विनिग्रहाद्
असाधुवादाद्भृशमुद्विजे यथा ॥ ३ ॥
मुझे नरकमें जानेका अथवा राज्यसे च्युत होनेका भय नहीं है। मैं पाशमें बँधने अथवा अपार दुःखमें पड़नेसे भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दण्ड दें यह भी मेरे भयका कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्तिसे! ||३||
(अनुष्टुप्)
पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हत्तमार्पितम् ।
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥ ४ ॥
अपने पूजनीय गुरुजनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त वाञ्छनीय है। क्योंकि वैसा दण्ड माता, पिता, भाई और सुहृद् भी मोहवश नहीं दे पाते ।।४।।
त्वं नूनमसुराणां नः परोक्षः परमो गुरुः ।
यो नोऽनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत् ॥ ५ ॥
आप छिपे रूपसे अवश्य ही हम असुरोंको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हमलोग धन, कुलीनता, बल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं ||५||
यस्मिन् वैरानुबन्धेन व्यूढेन विबुधेतराः ।
बहवो लेभिरे सिद्धिं यामु हैकान्तयोगिनः ॥ ६ ॥
आपसे हमलोगोंका जो उपकार होता है, उसे मैं क्या बताऊँ? अनन्यभावसे योग करनेवाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत-से असुरोंको आपके साथ दृढ़ वैरभाव करनेसे ही प्राप्त हो गयी है ।।६।।
तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकर्मणा ।
बद्धश्च वारुणैः पाशैः नातिव्रीडे न च व्यथे ॥ ७ ॥
जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनन्त लीलाएँ हैं, वही आप मुझे दण्ड दे रहे हैं और वरुणपाशसे बाँध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकारकी व्यथा ही ।।७।।
पितामहो मे भवदीयसम्मतः
प्रह्राद आविष्कृतसाधुवादः ।
भवद्विपक्षेण विचित्रवैशसं
संप्रापितस्त्वं परमः स्वपित्रा ॥ ८ ॥
प्रभो! मेरे पितामह प्रह्लादजीकी कीर्ति सारे जगत्में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपुने आपसे वैर-विरोध रखनेके कारण उन्हें अनेकों प्रकारके दुःख दिये। परन्तु वे आपके ही परायण रहे, उन्होंने अपना जीवन आपपर ही निछावर कर दिया ।।८।।
किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः
किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः ।
किं जायया संसृतिहेतुभूतया
मर्त्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥ ९ ॥
उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीरको लेकर क्या करना है, जब यह एक-न-एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन-सम्पत्ति लेनेके लिये स्वजन बने हुए हैं, । उन डाकुओंसे अपना स्वार्थ ही क्या है? पत्नीसे भी क्या लाभ है, जब वह जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें डालनेवाली ही है। जब मर ही जाना है, तब घरसे मोह करने में भी क्या स्वार्थ है? इन सब वस्तुओंमें उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है ।।९।।
इत्थं स निश्चित्य पितामहो महान्
अगाधबोधो भवतः पादपद्मम् ।
ध्रुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्
भीतः स्वपक्षक्षपणस्य सत्तम ॥ १० ॥
ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रह्लादजीने, यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टिसे उनके भाईबन्धुओंके नाश करनेवाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भयरहित एवं अविनाशी चरणकमलोंकी शरण ग्रहण की थी। क्यों न हो-वे संसारसे परम विरक्त, अगाध बोधसम्पन्न, उदारहृदय एवं संत-शिरोमणि जो हैं ।।१०।।
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं
दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः ।
इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितं
ययाध्रुवं स्तब्धमतिर्न बुध्यते ॥ ११ ॥
आप उस दृष्टिसे मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाताने मुझे बलात् – ऐश्वर्य-लक्ष्मीसे अलग करके आपके पास पहँचा दिया है। अच्छा ही हआ; क्योंकि ऐश्वर्यलक्ष्मीके कारण जीवकी बुद्धि जड हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि ‘मेरा यह जीवन मृत्युके पंजेमें पड़ा हुआ और अनित्य है’ ||११||
श्रीशुक उवाच –
(अनुष्टुप्)
तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्रादो भगवत्प्रियः ।
आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः ॥ १२ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चन्द्रमाके समान भगवान्के प्रेमपात्र प्रह्लादजी वहाँ आ पहुँचे ।।१२।।
तमिन्द्रसेनः स्वपितामहं श्रिया
विराजमानं नलिनायतेक्षणम् ।
प्रांशुं पिशंगांबरमञ्जनत्विषं
प्रलंबबाहुं शुभगर्षभमैक्षत ॥ १३ ॥
राजा बलिने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्रीसम्पन्न हैं। कमलके समान कोमल नेत्र हैं, लंबी-लंबी भुजाएँ हैं, सुन्दर ऊँचे और श्यामल शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं ।।१३।।
तस्मै बलिर्वारुणपाशयन्त्रितः
समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् ।
ननाम मूर्ध्नाश्रुविलोललोचनः
सव्रीडनीचीनमुखो बभूव ह ॥ १४ ॥
बलि इस समय वरुणपाशमें बँधे हुए थे। इसलिये प्रह्लादजीके आनेपर जैसे पहले वेउनकी पूजा किया करते थे, उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आँसुओंसे चंचल हो उठे, लज्जाके मारे मुँह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया ।।१४।।
स तत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं
हरिं सुनन्दाद्यनुगैरुपासितम् ।
उपेत्य भूमौ शिरसा महामना
ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रुविक्लवः ॥ १५ ॥
प्रह्लादजीने देखा कि भक्तवत्सल भगवान् वहीं विराजमान हैं और सुनन्द, नन्द आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेमके उद्रेकसे प्रह्लादजीका शरीर पुलकित हो गया, उनकी आँखोंमें आँसू छलक आये। वे आनन्दपूर्ण हृदयसे सिर झुकाये अपने स्वामीके पास गये और पृथ्वीपर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया ।।१५।।
श्रीप्रह्राद उवाच –
त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं
हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम् ।
मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो
विभ्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात् ॥ १६ ॥
प्रह्लादजीने कहा-प्रभो! आपने ही बलिको यह ऐश्वर्यपूर्ण इन्द्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुन्दर है, वैसा ही सुन्दर लेना भी! मैं समझता हूँ कि आपने इसपर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्माको मोहित करनेवाली राज्यलक्ष्मीसे इसे अलग कर दिया ||१६||
यया हि विद्वानपि मुह्यते यतः
तत् को विचष्टे गतिमात्मनो यथा ।
तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै
नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥ १७ ॥
प्रभो! लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक-ठीक कौन जान सकता है? अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महान् ईश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम साक्षी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।।१७।।
श्रीशुक उवाच –
(अनुष्टुप्)
तस्यानुश्रृवतो राजन् प्रह्रादस्य कृताञ्जलेः ।
हिरण्यगर्भो भगवान् उवाच मधुसूदनम् ॥ १८ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! प्रह्लादजी अंजलि बाँधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान् ब्रह्माजीने वामनभगवान्से कुछ कहना चाहा ।।१८।।
बद्धं वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पत्नी भयविह्वला ।
प्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं बभाषेऽवांमुखी नृप ॥ १९ ॥
परन्तु इतनेमें ही राजा बलिकी परम साध्वी पत्नी विन्ध्यावलीने अपने पतिको बँधा देखकर भयभीत हो भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया और हाथ जोड़, मुँह नीचा कर वह भगवान्से बोली ।।१९।।
श्रीविन्ध्यावलिरुवाच –
क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः ।
कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति
त्यक्तह्रियस्त्वदवरोपितकर्तृवादाः ॥ २० ॥
विन्ध्यावलीने कहा-प्रभो! आपने अपनी क्रीडाके लिये ही इस सम्पूर्ण जगतकी रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं, वे ही अपनेको इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता, भर्ता और संहर्ता हैं, तब आपकी मायासे मोहित होकर अपनेको झूठमूठ कर्ता माननेवाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे? ।।२०।।
श्रीब्रह्मोवाच –
(अनुष्टुप्)
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय ।
मुञ्चैनं हृतसर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम् ॥ २१ ॥
ब्रह्माजीने कहा-समस्त प्राणियोंके जीवनदाता, उनके स्वामी और जगत्स्वरूप देवाधिदेव प्रभो! अब आप इसे छोड़ दीजिये। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दण्डका पात्र नहीं है ।।२१।।
कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्मार्जिताश्च ये ।
निवेदितं च सर्वस्वं आत्माविक्लवया धिया ॥ २२ ॥
इसने अपनी सारी भूमि और पुण्यकर्मोंसे उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मातक आपको समर्पित कर दिया है एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, यह धैर्यसे च्युत नहीं हुआ है ।।२२।।
यत्पादयोरशठधीः सलिलं प्रदाय
दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् ।
अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं
दाश्वानविक्लवमनाः कथमार्तिमृच्छेत् ॥ २३ ॥
प्रभो! जो मनुष्य सच्चे हृदयसे कृपणता छोड़कर आपके चरणोंमें जलका अर्घ्य देता है और केवल दूर्वादलसे भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है। फिर बलिने तो बड़ी प्रसन्नतासे धैर्य और स्थिरतापूर्वक आपको त्रिलोकीका दान कर दिया है। तब यह दुःखका भागी कैसे हो सकता है? ।।२३।।
श्रीभगवानुवाच –
(अनुष्टुप्)
ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् ।
यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥ २४ ॥
श्रीभगवान्ने कहा-ब्रह्माजी! मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उसका धन छीन लिया करता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य धनके मदसे मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगोंका तिरस्कार करने लगता है ।।२४।।
यदा कदाचित् जीवात्मा संसरन्निजकर्मभिः ।
नानायोनिष्वनीशोऽयं पौरुषीं गतिमाव्रजेत् ॥ २५ ॥
यह जीव अपने कर्मोंके कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है, जब कभी मेरी बड़ी कृपासे मनुष्यका शरीर प्राप्त करता है ।।२५।।
जन्मकर्मवयोरूप विद्यैश्वर्यधनादिभिः ।
यद्यस्य न भवेत् स्तंभः तत्रायं मदनुग्रहः ॥ २६ ॥
मनुष्ययोनिमें जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदिके कारण घमंड न हो जाय तो समझना चाहिये कि मेरी बड़ी ही कृपा है ।।२६।।
मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः ।
सर्वश्रेयःप्रतीपानां हन्त मुह्येन्न मत्परः ॥ २७ ॥
कुलीनता आदि बहुत-से ऐसे कारण हैं, जो अभिमान और जडता आदि उत्पन्न करके मनुष्यको कल्याणके समस्त साधनोंसे वंचित कर देते हैं; परन्तु जो मेरे शरणागत होते हैं, वे इनसे मोहित नहींहोते ।।२७।।
एष दानवदैत्यानामग्रनीः कीर्तिवर्धनः ।
अजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥ २८ ॥
यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशोंमें अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढानेवाला है। इसने उस मायापर विजय प्राप्त कर ली है, जिसे जीतना अत्यन्त कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुःख भोगनेपर भी यह मोहित नहीं हुआ ।।२८।।
क्षीणरिक्थश्च्युतः स्थानात्क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ।
ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥ २९ ॥
गुरुणा भर्त्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रतः ।
छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक् ॥ ३० ॥
इसका धन छीन लिया, राजपदसे अलग कर दिया, तरह-तरहके आक्षेप किये, शत्रुओंने बाँध लिया, भाई-बन्धु छोड़कर चले गये, इतनी यातनाएँ भोगनी पड़ीं-यहाँतक कि गुरुदेवने भी इसको डाँटा-फटकारा और शापतक दे दिया। परन्तु इस दृढव्रतीने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोडी। मैंने इससे छलभरी बातें कीं, मनमें छल रखकर धर्मका उपदेश किया; परन्तु इस सत्यवादीने अपना धर्म न छोडा ||२९-३०।।
एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापं अमरैरपि ।
सावर्णेरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ ३१ ॥
अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है, जो बड़े-बड़े देवताओंको भी बड़ी कठिनाईसे प्राप्त होता है। सावर्णि मन्वन्तरमें यह मेरा परम भक्त इन्द्र होगा ।।३१।।
तावत् सुतलमध्यास्तां विश्वकर्मविनिर्मितम् ।
यदाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवः ।
नोपसर्गा निवसतां सम्भवन्ति ममेक्षया ॥ ३२ ॥
तबतक यह विश्वकर्माके बनाये हुए सुतललोकमें रहे। वहाँ रहनेवाले लोग मेरी कपादष्टिका अनुभव करते हैं। इसलिये उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तन्द्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओंसे पराजय और किसी प्रकारके विघ्नोंका सामना नहीं करना पड़ता ||३२||
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते ।
सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ ३३ ॥
[बलिको सम्बोधित कर] महाराज इन्द्रसेन! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाईबन्धुओंके साथ उस सुतललोकमें जाओ जिसे स्वर्गके देवता भी चाहते रहते हैं ।।३३।।
न त्वां अभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे ।
त्वत् शासनातिगान् दैत्यान् चक्रं मे सूदयिष्यति ॥ ३४ ॥
बड़े-बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे, दूसरोंकी तो बात ही क्या है! जो दैत्य तुम्हारी आज्ञाका उल्लंघन करेंगे, मेरा चक्र उनके टुकड़े-टुकड़े कर देगा ।।३४।।
रक्षिष्ये सर्वतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम् ।
सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान् ॥ ३५ ॥
मैं तुम्हारी, तुम्हारे अनुचरोंकी और भोगसामग्रीकी भी सब प्रकारके विघ्नोंसे रक्षा करूँगा। वीर बलि! तुम मुझे वहाँ सदा-सर्वदा अपने पास ही देखोगे ।।३५।।
तत्र दानवदैत्यानां संगात् ते भाव आसुरः ।
दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुण्ठो विनंक्ष्यति ॥ ३६ ॥
दानव और दैत्योंके संसर्गसे तुम्हारा जो कुछ आसुरभाव होगा वह मेरे प्रभावसे तुरंत दब जायगा और नष्ट हो जायगा ।।३६।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भवे बलिवामनसंवादे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥