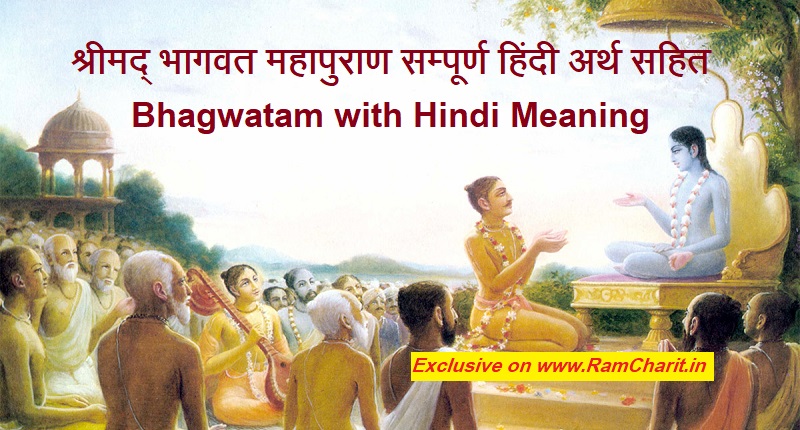श्रीमद् भागवत महापुराण स्कन्ध 8 अध्याय 8
अध्यायः ९
श्रीमद्भागवत महापुराण
अष्टमः स्कन्धः – नवमोऽध्यायः
देवानां अमृतपानं दैत्यवंचनं, राहुशिरश्छेदश्च –
श्रीशुक उवाच –
(अनुष्टुप्)
तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः ।
क्षिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं ददृशुः स्त्रियम् ॥ १ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! असुर आपसके सद्भाव और प्रेमको छोड़कर एकदूसरेकी निन्दा कर रहे थे और डाकूकी तरह एक-दूसरेके हाथसे अमृतका कलश छीन रहे थे। इसी बीचमें उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुन्दरी स्त्री उनकी ओर चली आ रही है ||१||
अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः ।
इति ते तां अभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहृच्छयाः ॥ २ ॥
वे सोचने लगे—’कैसा अनुपम सौन्दर्य है। शरीरमेंसे कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है! तनिक इसकी नयी उम्र तो देखो!’ बस, अब वे आपसकी लाग-डाँट भूलकर उसके पास दौड़ गये। उन लोगोंने काममोहित होकर उससे पूछा- ||२||
का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कुतो वा किं चिकीर्षसि ।
कस्यासि वद वामोरु मथ्नतीव मनांसि नः ॥ ३ ॥
‘कमलनयनी! तम कौन हो? कहाँसे आ रही हो? क्या करना चाहती हो? सुन्दरी! तुम किसकी कन्या हो? तुम्हें देखकर हमारे मनमें खलबली मच गयी है ।।३।।
न वयं त्वामरैर्दैत्यैः सिद्धगन्धर्वचारणैः ।
नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः ॥ ४ ॥
हम समझते हैं कि अबतक देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, चारण और लोकपालोंने भी तुम्हें स्पर्शतक न किया होगा। फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते? ||४||
नूनं त्वं विधिना सुभ्रूः प्रेषितासि शरीरिणाम् ।
सर्वेन्द्रियमनःप्रीतिं विधातुं सघृणेन किम् ॥ ५ ॥
सुन्दरी! अवश्य ही विधाताने दया करके शरीरधारियोंकी सम्पूर्ण इन्द्रियों एवं मनको तृप्त करनेके लिये तुम्हें यहाँ भेजा है ||५||
सा त्वं नः स्पर्धमानानां एकवस्तुनि मानिनि ।
ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥ ६ ॥
मानिनी! वैसे हमलोग एक ही जातिके हैं। फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिये हममें डाह और वैरकी गाँठ पड़ गयी है। सुन्दरी! तुम हमारा झगड़ा मिटा दो ।।६।।
वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः ।
विभजस्व यथान्यायं नैव भेदो यथा भवेत् ॥ ७ ॥
हम सभी कश्यपजीके पुत्र होनेके नाते सगे भाई हैं। हमलोगोंने अमतके लिये बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्यायके अनुसार निष्पक्षभावसे इसे बाँट दो, जिससे फिर हमलोगोंमें किसी प्रकारका झगड़ा न हो’ ||७||
इति उपामंत्रितो दैत्यैः मायायोषिद् वपुर्हरिः ।
प्रहस्य रुचिरापाङ्गैः निरीक्षन् इदमब्रवीत् ॥ ८ ॥
असुरोंने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीलासे स्त्रीवेष धारण करनेवाले भगवान्ने तनिक हँसकर और तिरछी चितवनसे उनकी ओर देखते हुए कहा- ||८||
श्रीभगवानुवाच –
कथं कश्यपदायादाः पुंश्चल्यां मयि संगताः ।
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥ ९ ॥
श्रीभगवान्ने कहा-आपलोग महर्षि कश्यपके पुत्र हैं और मैं हूँ कुलटा। आपलोग मुझपर न्यायका भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियोंका कभी विश्वास नहीं करते ।।९।।
सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः ।
सख्यान्याहुरनित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम् ॥ १० ॥
दैत्यो! कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियोंकी मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नये-नये शीकार ढूँढ़ा करते हैं ।।१०।।
श्रीशुक उवाच –
इति ते क्ष्वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः ।
जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम् ॥ ११ ॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्! मोहिनीकी परिहासभरी वाणीसे दैत्योंके मनमें और भी विश्वास हो गया। उन लोगोंने रहस्यपूर्ण भावसे हँसकर अमृतका कलश मोहिनीके हाथमें दे दिया ।।११।।
ततो गृहीत्वामृतभाजनं हरिः
बभाष ईषत् स्मितशोभया गिरा ।
यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाधु वा
कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम् ॥ १२ ॥
भगवान्ने अमृतका कलश अपने हाथमें लेकर तनिक मुसकराते हुए मीठी वाणीसे कहा -‘मैं उचित या अनुचित जो कुछ भी करूँ, वह सब यदि तुमलोगोंको स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बाँट सकती हूँ’ ।।१२।।
इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुंगवाः ।
अप्रमाणविदस्तस्याः तत् तथेत्यन्वमंसत ॥ १३ ॥
बड़े-बड़े दैत्योंने मोहिनीकी यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिये सबने एक स्वरसे कह दिया ‘स्वीकार है।’ इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनीके वास्तविक स्वरूपका पता नहीं था ।।१३।।
अथोपोष्य कृतस्नाना हुत्वा च हविषानलम् ।
दत्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजैः ॥ १४ ॥
इसके बाद एक दिनका उपवास करके सबने स्नान किया। हविष्यसे अग्निमें हवन किया। गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियोंको घास-चारा, अन्न-धनादिका यथायोग्य दान दिया तथा ब्राह्मणोंसे स्वस्त्ययन कराया ।।१४।।
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते ।
कुशेषु प्राविशन्सर्वे प्राग् अग्रेष्वभिभूषिताः ॥ १५ ॥
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सबने नये-नये वस्त्र धारण किये और इसके बाद सुन्दर-सुन्दर आभूषण धारण करके सब-के-सब उन कुशासनोंपर बैठ गये, जिनका अगला हिस्सा पूर्वकी ओर था ।।१५।।
प्राङ्मुखेषूपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च ।
धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥ १६ ॥
तस्यां नरेन्द्र करभोरुरुशद्दुकूल
श्रोणीतटालसगतिर्मदविह्वलाक्षी ।
सा कूजती कनकनूपुरशिञ्जितेन
कुम्भस्तनी कलसपाणिरथाविवेश ॥ १७ ॥
जब देवता और दैत्य दोनों ही धूपसे सुगन्धित, मालाओं और दीपकोंसे सजे-सजाये भव्य भवनमें पूर्वकी ओर मुंह करके बैठ गये, तब हाथमें अमृतका कलश लेकर मोहिनी सभामण्डपमें आयी। वह एक बड़ी सुन्दर साड़ी पहने हुए थी। नितम्बोंके भारके कारण वह धीरे-धीरे चल रही थी। आँखें मदसे विह्वल हो रही थीं। कलशके समान स्तन और गजशावककी सूंड़के समान जंघाएँ थीं। उसके स्वर्णनूपुर अपनी झनकारसे सभाभवनको मुखरित कर रहे थे ||१६-१७||
तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकर्ण
नासाकपोलवदनां परदेवताख्याम् ।
संवीक्ष्य सम्मुमुहुरुत्स्मितवीक्षणेन
देवासुरा विगलित स्तनपट्टिकान्ताम् ॥ १८ ॥
सुन्दर कानोंमें सोनेके कुण्डल थे और उसकी नासिका, कपोल तथा मुख बड़े ही सुन्दर थे। स्वयं परदेवता भगवान् मोहिनीके रूपमें ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मीजीकी कोई श्रेष्ठ सखी वहाँ आ गयी हो । मोहिनीने अपनी मुसकानभरी चितवनसे देवता और दैत्योंकी ओर देखा, तो वे सब-केसब मोहित हो गये। उस समय उनके स्तनोंपरसे अंचल कुछ खिसक गया था ।।१८।।
(अनुष्टुप्)
असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम् ।
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥ १९ ॥
भगवान्ने मोहिनीरूपमें यह विचार किया कि असुर तो जन्मसे ही क्रूर स्वभाववाले हैं। इनको अमृत पिलाना सर्पोको दूध पिलानेके समान बड़ा अन्याय होगा। इसलिये उन्होंने असुरोंको अमृतमें भाग नहीं दिया ||१९||
कल्पयित्वा पृथक् पंक्तीः उभयेषां जगत्पतिः ।
तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु ॥ २० ॥
भगवान्ने देवता और असुरोंकी अलग-अलग पंक्तियाँ बना दी और फिर दोनोंको कतार बाँधकर अपने-अपने दलमें बैठा दिया ||२०||
दैत्यान् गृहीतकलसो वञ्चयन् उपसञ्चरैः ।
दूरस्थान् पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम् ॥ २१ ॥
इसके बाद अमृतका कलश हाथमें लेकर भगवान् दैत्योंके पास चले गये। उन्हें हाव-भाव और कटाक्षसे मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओंके पास आ गये तथा उन्हें वह अमृत पिलाने लगे, जिसे पी लेनेपर बुढ़ापे और मृत्युका नाश हो जाता है ।।२१।।
ते पालयन्तः समयं असुराः स्वकृतं नृप ।
तूष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्त्रीविवादजुगुप्सया ॥ २२ ॥
परीक्षित्! असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञाका पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था और वे स्त्रीसे झगड़ने में अपनी निन्दा भी समझते थे। इसलिये वे चुपचाप बैठे रहे ।।२२।।
तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः ।
बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विप्रियम् ॥ २३ ॥
मोहिनीमें उनका अत्यन्त प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेमसम्बन्ध टूट न जाय। मोहिनीने भी पहले उन लोगोंका बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बँध गये थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनीको कोई अप्रिय बात नहीं कही ।।२३।।
देवलिङ्गप्रतिच्छन्नः स्वर्भानुर्देवसंसदि ।
प्रविष्टः सोममपिबत् चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः ॥ २४ ॥
जिस समय भगवान् देवताओंको अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु दैत्य देवताओंका वेष बनाकर उनके बीचमें आ बैठा और देवताओंके साथ उसने भी अमृत पी लिया। परन्तु तत्क्षण चन्द्रमा और सूर्यने उसकी पोल खोल दी ।।२४।।
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरः ।
हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाप्लावितोऽपतत् ॥ २५ ॥
अमृत पिलाते-पिलाते ही भगवान्ने अपने तीखी धारवाले चक्रसे उसका सिर काट डाला। अमृतका संसर्ग न होनेसे उसका धड़ नीचे गिर गया ।।२५।।
शिरस्त्वमरतां नीतं अजो ग्रहमचीकॢपत् ।
यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कौ अभिधावति वैरधीः ॥ २६ ॥
परन्तु सिर अमर हो गया और ब्रह्माजीने उसे ‘ग्रह’ बना दिया। वही राहु पर्वके दिन (पूर्णिमा और अमावस्याको) वैर-भावसे बदला लेनेके लिये चन्द्रमा तथा सूर्यपर आक्रमण किया करता है ।।२६।।
पीतप्रायेऽमृते देवैः भगवान् लोकभावनः ।
पश्यतां असुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरिः ॥ २७ ॥
जब देवताओंने अमृत पी लिया, तब समस्त लोकोंको जीवनदान करनेवाले भगवान्ने बड़े-बड़े दैत्योंके सामने ही मोहिनीरूप त्यागकर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया ।।२७।।
एवं सुरासुरगणाः समदेशकाल
हेत्वर्थकर्ममतयोऽपि फले विकल्पाः ।
तत्रामृतं सुरगणाः फलमञ्जसापुः
यत्पादपंकजरजःश्रयणान्न दैत्याः ॥ २८ ॥
परीक्षित्! देखो-देवता और दैत्य दोनोंने एक ही समय एक स्थानपर एक प्रयोजन तथा एक वस्तुके लिये एक विचारसे एक ही कर्म किया था, परन्तु फलमें बड़ा भेद हो गया। उनमेंसे देवताओंने बड़ी सुगमतासे अपने परिश्रमका फल-अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने भगवान्के चरणकमलोंकी रजका आश्रय लिया था। परन्तु उससे विमुख होनेके कारण परिश्रम करनेपर भी असुरगण अमृतसे वंचित ही रहे ।।२८।।
यद् युज्यतेऽसुवसुकर्ममनोवचोभिः
देहात्मजादिषु नृभिस्तदसत्पृथक्त्वात् ।
तैरेव सद्भवति यत् क्रियतेऽपृथक्त्वात्
सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत् ॥ २९ ॥
मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदिसे शरीर एवं पुत्र आदिके लिये जो कुछ करता है-वह व्यर्थ ही होता है; क्योंकि उसके मूलमें भेदबुद्धि बनी रहती है। परन्तु उन्हीं प्राण आदि वस्तुओंके द्वारा भगवान्के लिये जो कुछ किया जाता है, वह सब भेदभावसे रहित होनेके कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसारके लिये सफल हो जाता है। जैसे वृक्षकी जड़में पानी देनेसे उसका तना, टहनियाँ और पत्ते-सब-के-सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान्के लिये कर्म करनेसे वे सबके लिये हो जाते हैं ।।२९।।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
अष्टमस्कन्धे अमृतमथने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥
हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥